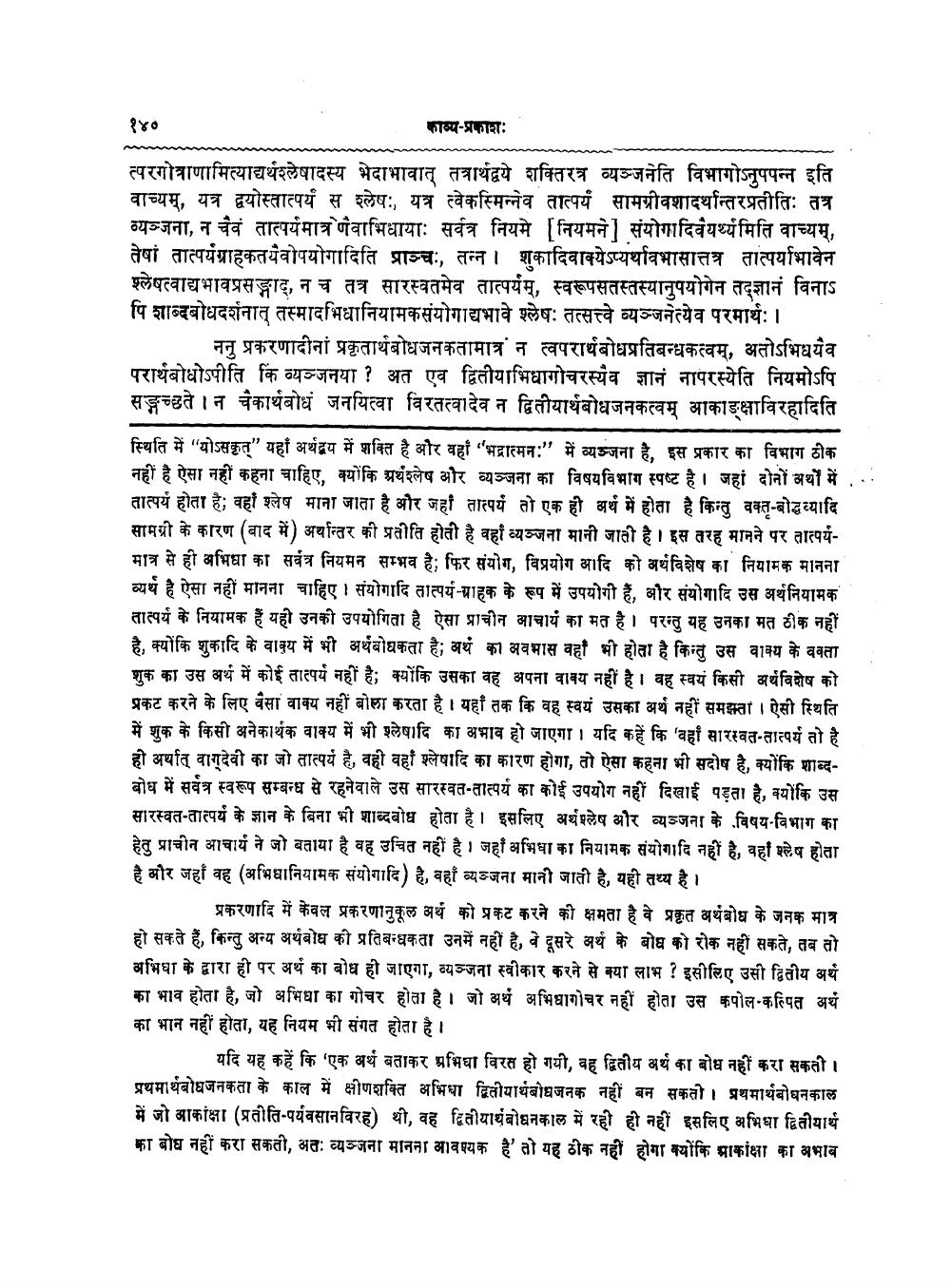________________
१४०
काव्य-प्रकाशः
-
त्परगोत्राणामित्याद्यर्थश्लेषादस्य भेदाभावात् तत्रार्थद्वये शक्तिरत्र व्यञ्जनेति विभागोऽनुपपन्न इति वाच्यम्, यत्र द्वयोस्तात्पर्य स श्लेषः, यत्र त्वेकस्मिन्नेव तात्पर्य सामग्रीवशादर्थान्तरप्रतीतिः तत्र व्यञ्जना, न चैवं तात्पर्यमाणैवाभिधायाः सर्वत्र नियमे [नियमने] संयोगादिवैयर्थ्य मिति वाच्यम्, तेषां तात्पर्यग्राहकतयैवोपयोगादिति प्राञ्चः, तन्न। शुकादिवाक्येऽप्यर्थावभासात्तत्र तात्पर्याभावेन श्लेषत्वाद्यभावप्रसङ्गाद, न च तत्र सारस्वतमेव तात्पर्यम्, स्वरूपसतस्तस्यानुपयोगेन तद्ज्ञानं विनाऽ पि शाब्दबोधदर्शनात् तस्मादभिधानियामकसंयोगाद्यभावे श्लेषः तत्सत्त्वे व्यञ्जनेत्येव परमार्थः ।
ननु प्रकरणादीनां प्रकृतार्थबोधजनकतामात्र न त्वपरार्थबोधप्रतिबन्धकत्वम्, अतोऽभिधयैव परार्थबोधोऽपीति किं व्यञ्जनया ? अत एव द्वितीयाभिधागोचरस्यैव ज्ञानं नापरस्येति नियमोऽपि सङ्गच्छते । न चैकार्थबोधं जनयित्वा विरतत्वादेव न द्वितीयार्थबोधजनकत्वम् आकाङ्क्षाविरहादिति
स्थिति में "योऽसकृत" यहाँ अर्थद्वय में शक्ति है और वहाँ "भद्रात्मनः" में व्यञ्जना है, इस प्रकार का विभाग ठीक नहीं है ऐसा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि अर्थश्लेष और व्यञ्जना का विषयविभाग स्पष्ट है। जहां दोनों अर्थों में तात्पर्य होता है; वहां श्लेष माना जाता है और जहाँ तात्पर्य तो एक ही अर्थ में होता है किन्तु वक्तृ-बोद्धव्यादि सामग्री के कारण (बाद में) अर्थान्तर की प्रतीति होती है वहाँ व्यञ्जना मानी जाती है। इस तरह मानने पर तात्पर्यमात्र से ही अभिधा का सर्वत्र नियमन सम्भव है; फिर संयोग, विप्रयोग आदि को अर्थविशेष का नियामक मानना व्यर्थ है ऐसा नहीं मानना चाहिए। संयोगादि तात्पर्य-ग्राहक के रूप में उपयोगी हैं, और संयोगादि उस अर्थनियामक तात्पर्य के नियामक हैं यही उनकी उपयोगिता है ऐसा प्राचीन आचार्य का मत है। परन्तु यह उनका मत ठीक नहीं है, क्योंकि शुकादि के वाक्य में भी अर्थबोधकता है; अथं का अवभास वहाँ भी होता है किन्तु उस वाक्य के वक्ता शुक का उस अर्थ में कोई तात्पर्य नहीं है; क्योंकि उसका वह अपना वाक्य नहीं है। वह स्वयं किसी अर्थविशेष को प्रकट करने के लिए वैसा वाक्य नहीं बोला करता है । यहाँ तक कि वह स्वयं उसका अर्थ नहीं समझता । ऐसी स्थिति में शुक के किसी अनेकार्थक वाक्य में भी श्लेषादि का अभाव हो जाएगा। यदि कहें कि 'वहाँ सारस्वत-तात्पर्य तो है हो अर्थात् वाग्देवी का जो तात्पर्य है, वही वहाँ श्लेषादि का कारण होगा, तो ऐसा कहना भी सदोष है, क्योंकि शाब्दबोध में सर्वत्र स्वरूप सम्बन्ध से रहनेवाले उस सारस्वत-तात्पर्य का कोई उपयोग नहीं दिखाई पड़ता है, क्योंकि उस सारस्वत-तात्पर्य के ज्ञान के बिना भी शाब्दबोध होता है। इसलिए अर्थश्लेष और व्यञ्जना के विषय विभाग का हेतु प्राचीन आचार्य ने जो बताया है वह उचित नहीं है । जहाँ अभिधा का नियामक संयोगादि नहीं है, वहाँ श्लेष होता है और जहाँ वह (अभिधानियामक संयोगादि) है, वहाँ व्यञ्जना मानी जाती है, यही तथ्य है।
प्रकरणादि में केवल प्रकरणानुकूल अर्थ को प्रकट करने की क्षमता है वे प्रकृत अर्थबोध के जनक मात्र हो सकते हैं, किन्तु अन्य अर्थबोध की प्रतिबन्धकता उनमें नहीं है, वे दूसरे अर्थ के बोध को रोक नहीं सकते, तब तो अभिधा के द्वारा ही पर अर्थ का बोध हो जाएगा, व्यञ्जना स्वीकार करने से क्या लाभ ? इसीलिए उसी द्वितीय अर्थ का भाव होता है, जो अभिधा का गोचर होता है। जो अर्थ अभिधागोचर नहीं होता उस कपोल कल्पित अर्थ का भान नहीं होता, यह नियम भी संगत होता है।
यदि यह कहें कि 'एक अर्थ बताकर अभिधा विरत हो गयी, वह द्वितीय अर्थ का बोध नहीं करा सकती। प्रथमार्थबोधजनकता के काल में क्षीणशक्ति अभिधा द्वितीयार्थबोधजनक नहीं बन सकती। प्रथमार्थबोधनकाल में जो आकांक्षा (प्रतीति-पर्यवसानविरह) थी, वह द्वितीयार्थबोधनकाल में रही ही नहीं इसलिए अभिधा द्वितीयार्थ का बोध नहीं करा सकती, अतः व्यञ्जना मानना आवश्यक है तो यह ठीक नहीं होगा क्योंकि भाकांक्षा का अभाव