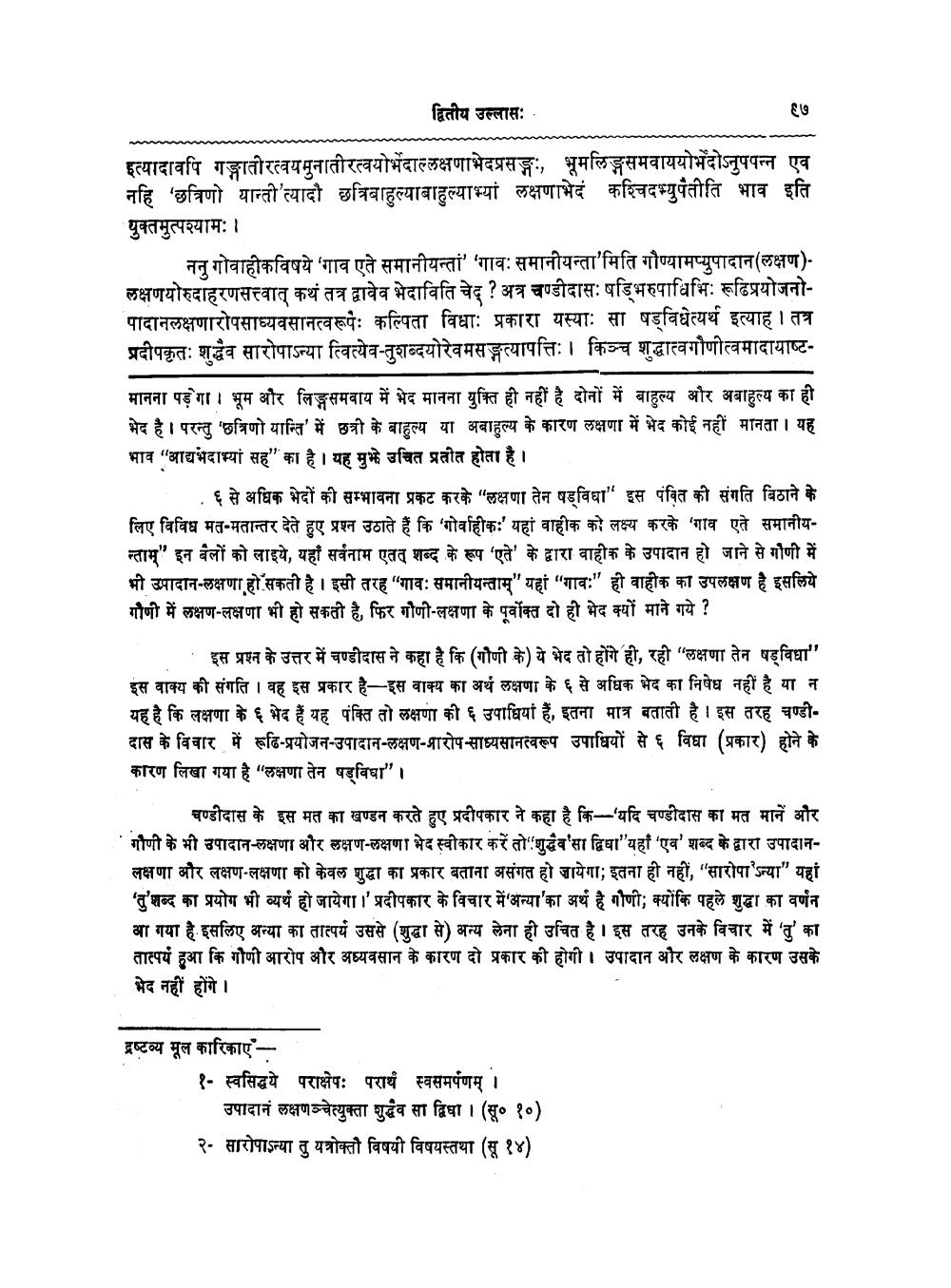________________
द्वितीय उल्लास: .
६७
इत्यादावपि गङ्गातीरत्वयमुनातीरत्वयोर्भेदाल्लक्षणाभेदप्रसङ्गः, भूमलिङ्गसमवाययो दोऽनुपपन्न एव नहि 'छत्रिणो यान्तो'त्यादौ छत्रिबाहुल्याबाहुल्याभ्यां लक्षणाभेदं कश्चिदभ्युपैतीति भाव इति युक्तमुत्पश्यामः।
ननु गोवाहीकविषये 'गाव एते समानीयन्तां' 'गावः समानीयन्ता'मिति गौण्यामप्युपादान(लक्षण). लक्षणयोरुदाहरणसत्त्वात् कथं तत्र द्वावेव भेदाविति चेद् ? अत्र चण्डीदासः षड्भिरुपाधिभिः रूढिप्रयोजनोपादानलक्षणारोपसाध्यवसानत्वरूपैः कल्पिता विधाः प्रकारा यस्याः सा षड्विधेत्यर्थ इत्याह । तत्र प्रदीपकृतः शुद्धैव सारोपाऽन्या त्वित्येव-तुशब्दयोरेवमसङ्गत्यापत्तिः । किञ्च शुद्धात्वगौणीत्वमादायाष्ट
मानना पड़ेगा। भूम और लिङ्गसमवाय में भेद मानना युक्ति ही नहीं है दोनों में बाहुल्य और अबाहुल्य का ही भेद है । परन्तु 'छत्रिणो यान्ति' में छत्री के बाहुल्य या अबाहुल्य के कारण लक्षणा में भेद कोई नहीं मानता। यह भाव "आद्यभेदाभ्यां सह" का है। यह मुझे उचित प्रतीत होता है।
.६ से अधिक भेदों की सम्भावना प्रकट करके "लक्षणा तेन षड्विधा" इस पंक्ति की संगति बिठाने के लिए विविध मत-मतान्तर देते हुए प्रश्न उठाते हैं कि 'गोर्वाहीकः' यहां वाहीक को लक्ष्य करके 'गाव एते समानीयन्ताम्" इन बैलों को लाइये, यहाँ सर्वनाम एतत् शब्द के रूप 'एते' के द्वारा वाहीक के उपादान हो जाने से गौणी में भी आदान-लक्षणा हो सकती है । इसी तरह "गावः समानीयन्ताम्" यहां "गावः" ही वाहीक का उपलक्षण है इसलिये गौणी में लक्षण-लक्षणा भी हो सकती है, फिर गौणी-लक्षणा के पूर्वोक्त दो ही भेद क्यों माने गये ?
- इस प्रश्न के उत्तर में चण्डीदास ने कहा है कि (गौणी के) ये भेद तो होंगे ही, रही "लक्षणा तेन षडविधा" इस वाक्य की संगति । वह इस प्रकार है-इस वाक्य का अर्थ लक्षणा के ६ से अधिक भेद का निषेध नहीं है या न यह है कि लक्षणा के ६ भेद हैं यह पंक्ति तो लक्षणा की ६ उपाधियां हैं, इतना मात्र बताती है । इस तरह चण्डीदास के विचार में रूढि-प्रयोजन-उपादान-लक्षण-आरोप-साध्यसानत्वरूप उपाधियों से ६ विध होने के कारण लिखा गया है "लक्षणा तेन षड्विधा"।
चण्डीदास के इस मत का खण्डन करते हए प्रदीपकार ने कहा है कि-'यदि चण्डीदास का मत माने और गौणी के भी उपादान-लक्षणा और लक्षण-लक्षणा भेद स्वीकार करें तो शुद्धव'सा द्विधा"यहाँ 'एव' शब्द के द्वारा उपादानलक्षणा और लक्षण-लक्षणा को केवल शुद्धा का प्रकार बताना असंगत हो जायेगा; इतना ही नहीं, "सारोपा'ऽन्या" यहां 'तु'शब्द का प्रयोग भी व्यर्थ हो जायेगा।' प्रदीपकार के विचार में अन्या'का अर्थ है गौणी; क्योंकि पहले शुद्धा का वर्णन आ गया है इसलिए अन्या का तात्पर्य उससे (शुद्धा से) अन्य लेना ही उचित है । इस तरह उनके विचार में 'तु' का तात्पर्य हुआ कि गौणी आरोप और अध्यवसान के कारण दो प्रकार की होगी। उपादान और लक्षण के कारण उसके भेद नहीं होंगे।
द्रष्टव्य मूल कारिकाएं
१. स्वसिद्धये पराक्षेपः परार्थ स्वसमर्पणम् ।
उपादानं लक्षणञ्चेत्युक्ता शुद्धव सा द्विधा । (सू० १०) २. सारोपाऽन्या तु यत्रोक्तौ विषयी विषयस्तथा (सू १४)