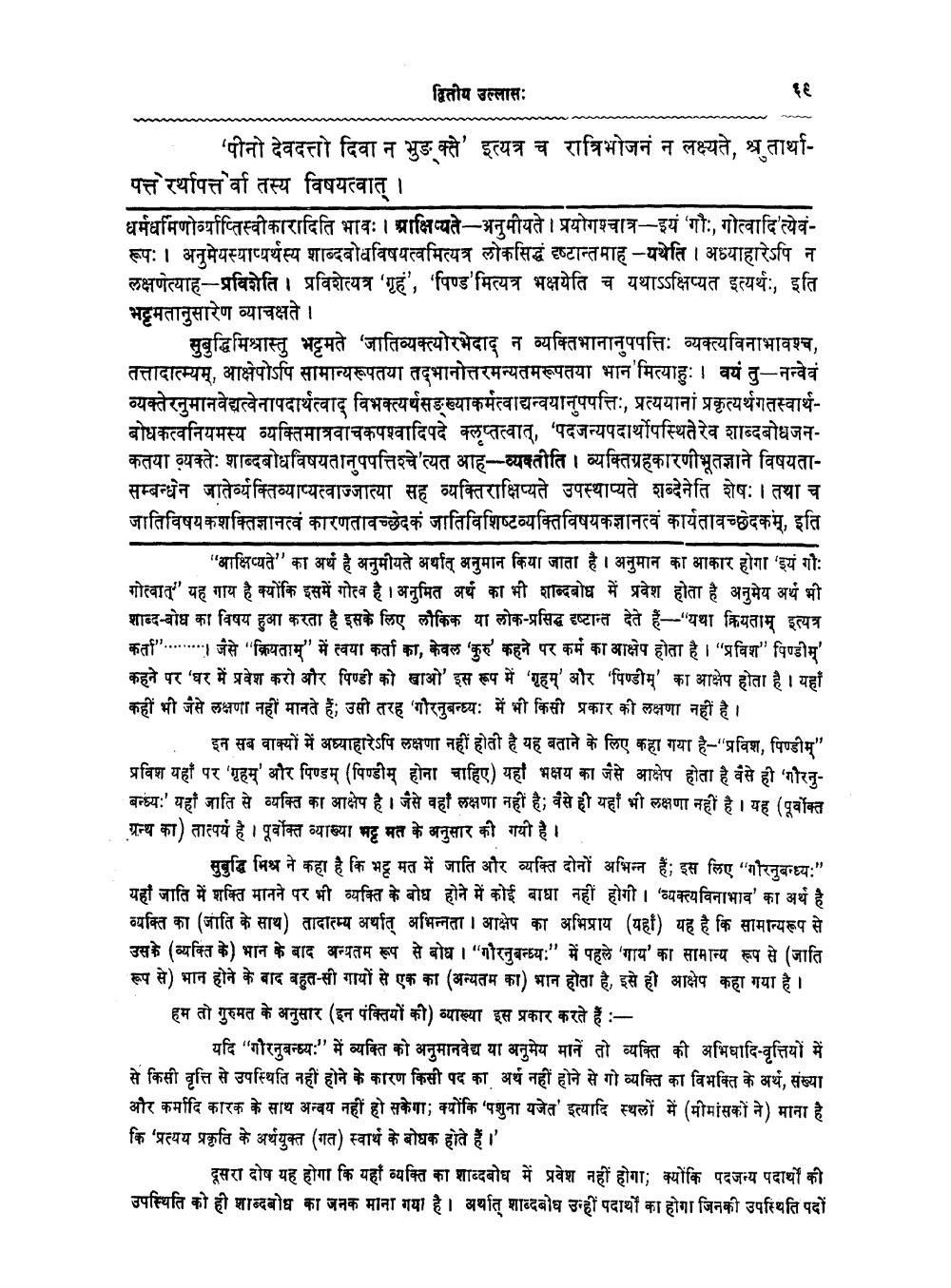________________
द्वितीय उल्लासः
1
'पीनो देवदत्तो दिवा न भुङ्क्ते' इत्यत्र च रात्रिभोजनं न लक्ष्यते श्रुतार्था - पत्रपत्र्वा तस्य विषयत्वात् ।
६६
धर्मधर्मिणोर्व्याप्तिस्वीकारादिति भावः । श्राक्षिप्यते - अनुमीयते । प्रयोगश्चात्र - इयं 'गौः, गोत्वादित्येवंरूपः । अनुमेयस्याप्यर्थस्य शाब्दबोधविषयत्वमित्यत्र लोकसिद्धं दृष्टान्तमाह-यथेति । अध्याहारेऽपि न लक्षणेत्याह - प्रविशेति । प्रविशेत्यत्र 'गृह', 'पिण्ड' मित्यत्र भक्षयेति च यथाऽऽक्षिप्यत इत्यर्थः, इति भट्टमतानुसारेण व्याचक्षते ।
सुबुद्धिमिश्रास्तु भट्ट 'जातिव्यक्त्योरभेदाद् न व्यक्तिभानानुपपत्तिः व्यक्त्यविनाभावश्च, तत्तादात्म्यम्, आक्षेपोऽपि सामान्यरूपतया तद्भानोत्तरमन्यतमरूपतया भान मित्याहुः । वयं तु– नन्वेवं व्यक्तेरनुमानवेद्यत्वेनापदार्थत्वाद् विभक्त्यर्थ सङ्ख्या कर्मत्वाद्यन्वयानुपपत्तिः प्रत्ययानां प्रकृत्यर्थगतस्वार्थबोधकत्वनियमस्य व्यक्तिमात्रवाचकपश्वादिपदे क्लृप्तत्वात्, 'पदजन्यपदार्थोपस्थितेरेव शाब्दबोधजनकतया व्यक्तेः शाब्दबोधविषयतानुपपत्तिश्चेत्यत आह-व्यक्तीति । व्यक्तिग्रहकारणीभूतज्ञाने विषयतासम्बन्धेन जातेर्व्यक्तिव्याप्यत्वाज्जात्या सह व्यक्तिराक्षिप्यते उपस्थाप्यते शब्देनेति शेषः । तथा च जातिविषयक शक्तिज्ञानत्वं कारणतावच्छेदकं जातिविशिष्टव्यक्ति विषयकज्ञानत्वं कार्यतावच्छेदकम्, इति
"आक्षिप्यते " का अर्थ है अनुमीयते अर्थात् अनुमान किया जाता है। अनुमान का आकार होगा 'इयं गौः गोत्वात्" यह गाय है क्योंकि इसमें गोत्व है । अनुमित अर्थ का भी शाब्दबोध में प्रवेश होता है अनुमेय अर्थ भी शाब्द-बोध का विषय हुआ करता है इसके लिए लौकिक या लोक प्रसिद्ध दृष्टान्त देते हैं- "यथा क्रियताम् इत्यत्र कर्ता”-----.! जैसे “क्रियताम्' में त्वया कर्ता का, केवल 'कुरु' कहने पर कर्म का आक्षेप होता है । "प्रविश" पिण्डीम्' कहने पर 'घर में प्रवेश करो और पिण्डी को खाओ' इस रूप में 'गृहम्' और 'पिण्डीम्' का आक्षेप होता है । यहाँ कहीं भी जैसे लक्षणा नहीं मानते हैं; उसी तरह 'गौरनुबन्ध्यः में भी किसी प्रकार की लक्षणा नहीं है ।
इन सब वाक्यों में अध्याहारेऽपि लक्षणा नहीं होती है यह बताने के लिए कहा गया है - " प्रविश, पिण्डीम् " प्रविश यहाँ पर 'गृहम्' और पिण्डम् ( पिण्डीम् होना चाहिए ) यहाँ भक्षय का जैसे आक्षेप होता है वैसे ही 'गौरनुबन्ध्यः' यहाँ जाति से व्यक्ति का आक्षेप है। जैसे वहाँ लक्षणा नहीं है; वैसे ही यहाँ भी लक्षणा नहीं है । यह (पूर्वोक्त ग्रन्थ का) तात्पर्य है । पूर्वोक्त व्याख्या भट्ट मत के अनुसार की गयी है । सुबुद्धि मिश्र ने कहा है कि भट्ट मत में जाति और व्यक्ति दोनों अभिन्न हैं; इस लिए "गौरनुबन्ध्य : " यहाँ जाति में शक्ति मानने पर भी व्यक्ति के बोध होने में कोई बाधा नहीं होगी । 'व्यक्त्य विनाभाव' का अर्थ है। व्यक्ति का ( जाति के साथ) तादात्म्य अर्थात् अभिन्नता । आक्षेप का अभिप्राय ( यहाँ ) यह है कि सामान्यरूप से उसके ( व्यक्ति के ) भान के बाद अन्यतम रूप से बोध । "गौरनुबन्ध्यः" में पहले 'गाय' का सामान्य रूप से (जाति रूप से) भान होने के बाद बहुत-सी गायों से एक का ( अन्यतम का ) भान होता है, इसे ही आक्षेप कहा गया है ।
हम तो गुरुमत के अनुसार ( इन पंक्तियों की ) व्याख्या इस प्रकार करते हैं
-
यदि "गौरनुबन्ध्य:" में व्यक्ति को अनुमानवेद्य या अनुमेय मानें तो व्यक्ति की अभिघादि-वृत्तियों में से किसी वृत्ति से उपस्थिति नहीं होने के कारण किसी पद का अर्थ नहीं होने से गो व्यक्ति का विभक्ति के अर्थ, संख्या और कर्मादि कारक के साथ अन्वय नहीं हो सकेगा; क्योंकि 'पशुना यजेत' इत्यादि स्थलों में ( मीमांसकों ने) माना है for 'प्रत्यय प्रकृति के अर्थयुक्त (गत ) स्वार्थ के बोधक होते हैं।'
दूसरा दोष यह होगा कि यहाँ व्यक्ति का शाब्दबोध में प्रवेश नहीं होगा; क्योंकि पदजन्य पदार्थों की उपस्थिति को ही शाब्दबोध का जनक माना गया है । अर्थात् शाब्दबोध उन्हीं पदार्थों का होगा जिनकी उपस्थिति पदों