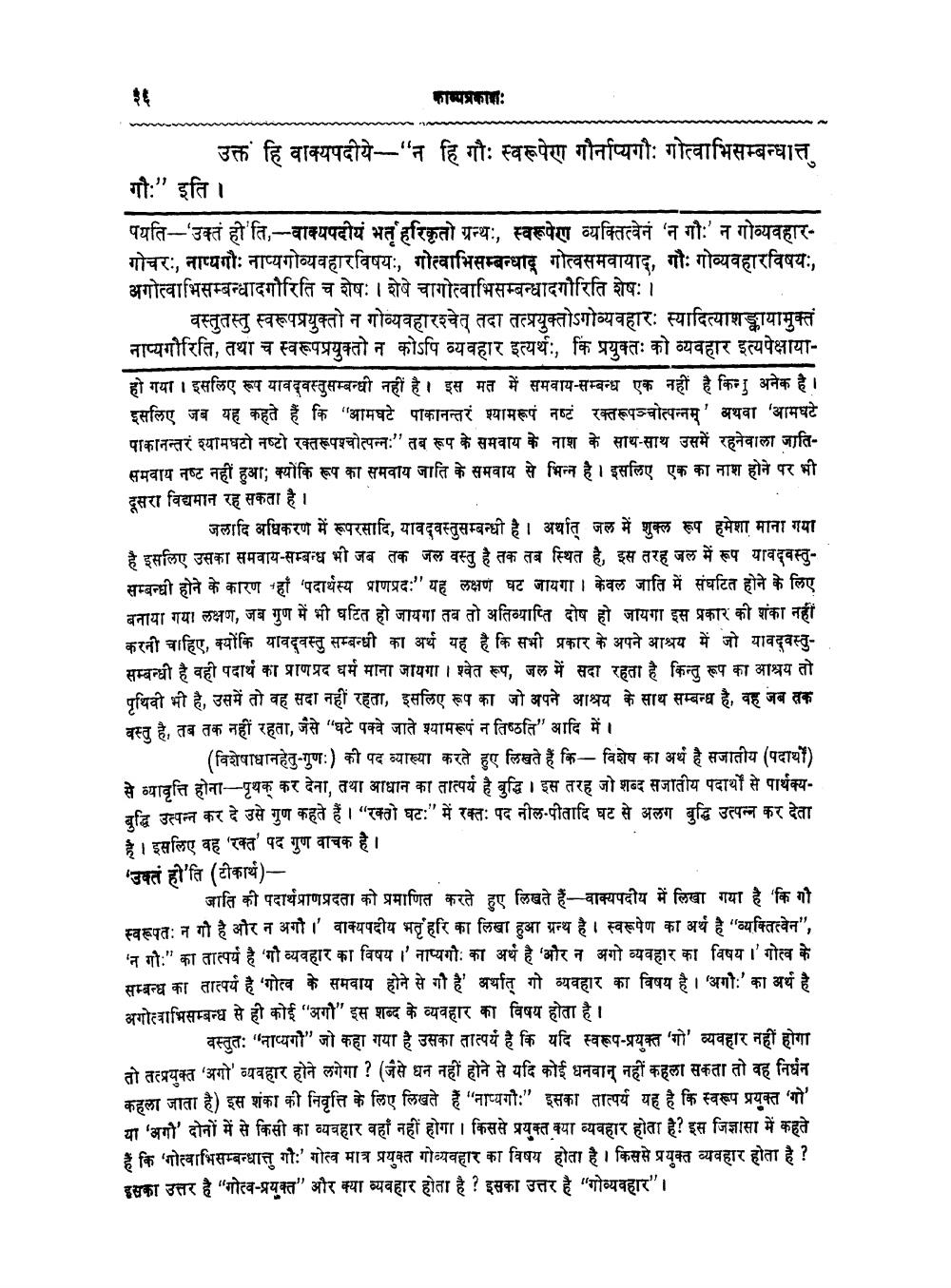________________
काव्यप्रकाश
उक्त हि वाक्यपदीये-"न हि गौः स्वरूपेण गौ प्यगौः गोत्वाभिसम्बन्धात्त गौः" इति। पयति-'उक्तं ही ति,-वाक्यपदीयं भर्तृहरिकृतो ग्रन्थः, स्वरूपेण व्यक्तित्वेनं 'न गौः' न गोव्यवहारगोचरः, नाप्यगौः नाप्यगोव्यवहारविषयः, गोत्वाभिसम्बन्धादू गोत्वसमवायाद्, गौः गोव्यवहारविषयः, अगोत्वाभिसम्बन्धादगौरिति च शेषः । शेषे चागोत्वाभिसम्बन्धादगौरिति शेषः ।।
___ वस्तुतस्तु स्वरूपप्रयुक्तो न गोव्यवहारश्चेत् तदा तत्प्रयुक्तोऽगोव्यवहारः स्यादित्याशङ्कायामुक्तं नाप्यगौरिति, तथा च स्वरूपप्रयुक्तो न कोऽपि व्यवहार इत्यर्थः, किं प्रयुक्तः को व्यवहार इत्यपेक्षायाहो गया । इसलिए रूप यावद्वस्तुसम्बन्धी नहीं है। इस मत में समवाय-सम्बन्ध एक नहीं है किन्तु अनेक है। इसलिए जब यह कहते हैं कि "आमघटे पाकानन्तरं श्यामरूपं नष्टं रक्तरूपञ्चोत्पन्नम्' अथवा 'आमघटे पाकानन्तरं श्यामघटो नष्टो रक्तरूपश्चोत्पन्नः" तब रूप के समवाय के नाश के साथ-साथ उसमें रहनेवाला जातिसमवाय नष्ट नहीं हुआ; क्योंकि रूप का समवाय जाति के समवाय से भिन्न है । इसलिए एक का नाश होने पर भी दूसरा विद्यमान रह सकता है।
जलादि अधिकरण में रूपरसादि, यावद्वस्तुसम्बन्धी है। अर्थात् जल में शुक्ल रूप हमेशा माना गया है इसलिए उसका समवाय-सम्बन्ध भी जब तक जल वस्तु है तक तब स्थित है, इस तरह जल में रूप यावद्वस्तुसम्बन्धी होने के कारण हो 'पदार्थस्य प्राणप्रदः" यह लक्षण घट जायगा। केवल जाति में संघटित होने के लिए बनाया गया लक्षण, जब गुण में भी घटित हो जायगा तब तो अतिव्याप्ति दोष हो जायगा इस प्रकार की शंका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यावद्वस्तु सम्बन्धी का अर्थ यह है कि सभी प्रकार के अपने आश्रय में जो यावद्वस्तुसम्बन्धी है वही पदार्थ का प्राणप्रद धर्म माना जायगा । श्वेत रूप, जल में सदा रहता है किन्तु रूप का आश्रय तो पृथिवी भी है, उसमें तो वह सदा नहीं रहता, इसलिए रूप का जो अपने आश्रय के साथ सम्बन्ध है, वह जब तक वस्तु है, तब तक नहीं रहता, जैसे “घटे पक्वे जाते श्यामरूपं न तिष्ठति" आदि में।
(विशेषाधानहेतु-गुणः) की पद व्याख्या करते हुए लिखते हैं कि- विशेष का अर्थ है सजातीय (पदार्थों) से व्यावृत्ति होना-पृथक् कर देना, तथा आधान का तात्पर्य है बुद्धि । इस तरह जो शब्द सजातीय पदार्थों से पार्थक्यबद्धि उत्पन्न कर दे उसे गुण कहते हैं । “रक्तो घटः” में रक्तः पद नील-पीतादि घट से अलग बुद्धि उत्पन्न कर देता है। इसलिए वह 'रक्त' पद गुण वाचक है। 'उक्तं हो ति (टीकार्थ)
जाति की पदार्थप्राणप्रदता को प्रमाणित करते हुए लिखते हैं-वाक्यपदीय में लिखा गया है कि गौ स्वरूपतः न गौ है और न अगौ।' वाक्यपदीय भर्तृहरि का लिखा हुआ ग्रन्थ है। स्वरूपेण का अर्थ है "व्यक्तित्वेन", नगौः" का तात्पर्य है 'गौ व्यवहार का विषय ।' नाप्यगौः का अर्थ है 'और न अगो व्यवहार का विषय ।' गोत्व के सम्बन्ध का तात्पर्य है 'गोत्व के समवाय होने से गौ है अर्थात् गो व्यवहार का विषय है । 'अगोः' का अर्थ है अगोवाभिसम्बन्ध से ही कोई "अगों" इस शब्द के व्यवहार का विषय होता है।
वस्तुत: "नाप्यगो" जो कहा गया है उसका तात्पर्य है कि यदि स्वरूप-प्रयुक्त 'गो' व्यवहार नहीं होगा तो तत्प्रयक्त 'अगो' व्यवहार होने लगेगा ? (जैसे धन नहीं होने से यदि कोई धनवान् नहीं कहला सकता तो वह निर्धन कहला जाता है) इस शंका की निवृत्ति के लिए लिखते हैं "नाप्यगौः" इसका तात्पर्य यह है कि स्वरूप प्रयुक्त 'गो' या 'अगौं' दोनों में से किसी का व्यवहार वहाँ नहीं होगा। किससे प्रयुक्त क्या व्यवहार होता है? इस जिज्ञासा में कहते हैं कि 'गोत्वाभिसम्बन्धात्तु गौः' गोत्व मात्र प्रयुक्त गोव्यवहार का विषय होता है । किससे प्रयुक्त व्यवहार होता है ? इसका उत्तर है “गोत्व-प्रयुक्त” और क्या व्यवहार होता है ? इसका उत्तर है “गोव्यवहार"।