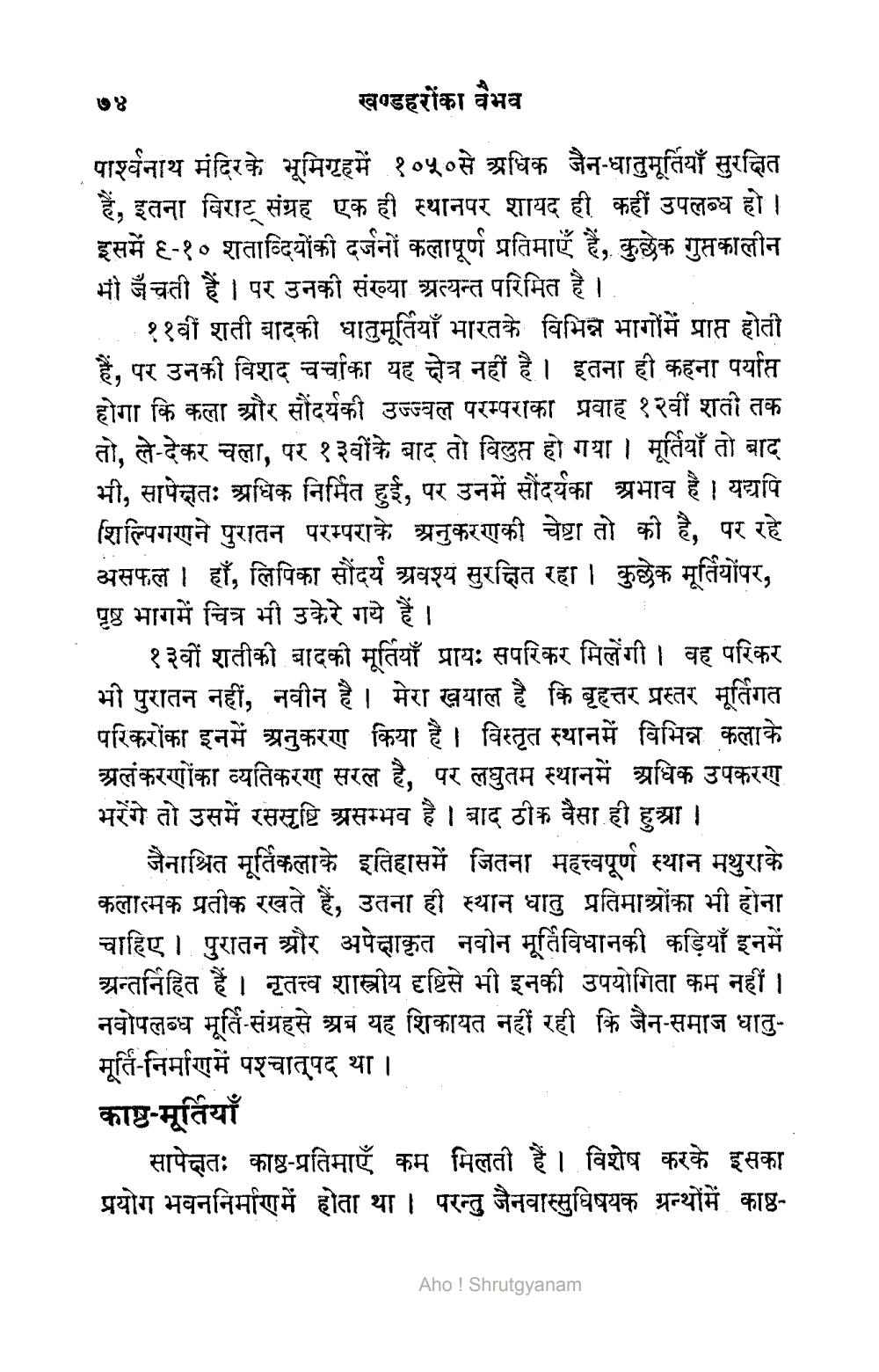________________
७४
खण्डहरोंका वैभव पार्श्वनाथ मंदिर के भूमिगृहमें १०५० से अधिक जैन-धातुमूर्तियाँ सुरक्षित हैं, इतना विराट् संग्रह एक ही स्थानपर शायद ही कहीं उपलब्ध हो । इसमें ६-१० शताब्दियोंकी दर्जनों कलापूर्ण प्रतिमाएँ हैं, कुछेक गुप्तकालीन भी ऊँचती हैं । पर उनकी संख्या अत्यन्त परिमित है।
११वीं शती बादकी धातुमूर्तियाँ भारतके विभिन्न भागोंमें प्राप्त होती हैं, पर उनकी विशद चर्चाका यह क्षेत्र नहीं है। इतना ही कहना पर्याप्त होगा कि कला और सौंदर्यकी उज्ज्वल परम्पराका प्रवाह १२वीं शती तक तो, ले-देकर चला, पर १३वीं के बाद तो विलुप्त हो गया। मूर्तियाँ तो बाद भी, सापेक्षतः अधिक निर्मित हुई, पर उनमें सौंदर्यका अभाव है । यद्यपि शिल्पिगणने पुरातन परम्पराके अनुकरणकी चेष्टा तो की है, पर रहे असफल । हाँ, लिपिका सौंदर्य अवश्य सुरक्षित रहा। कुछेक मूर्तियोंपर, पृष्ठ भागमें चित्र भी उकेरे गये हैं।
१३वीं शतीकी बादकी मूर्तियाँ प्रायः सपरिकर मिलेंगी। वह परिकर भी पुरातन नहीं, नवीन है। मेरा खयाल है कि बृहत्तर प्रस्तर मूर्तिगत परिकरोंका इनमें अनुकरण किया है। विस्तृत स्थानमें विभिन्न कलाके अलंकरणोंका व्यतिकरण सरल है, पर लघुतम स्थानमें अधिक उपकरण भरेंगे तो उसमें रससृष्टि असम्भव है । बाद ठीक वैसा ही हुआ।
जैनाश्रित मूर्तिकलाके इतिहासमें जितना महत्त्वपूर्ण स्थान मथुराके कलात्मक प्रतीक रखते हैं, उतना ही स्थान धातु प्रतिमाओंका भी होना चाहिए। पुरातन और अपेक्षाकृत नवोन मूर्तिविधानकी कड़ियाँ इनमें अन्तर्निहित हैं। नृतत्त्व शास्त्रीय दृष्टिसे भी इनकी उपयोगिता कम नहीं। नवोपलब्ध मूर्ति-संग्रहसे अब यह शिकायत नहीं रही कि जैन-समाज धातुमूर्ति-निर्माणमें पश्चात्पद था। काष्ठ-मूर्तियाँ ___ सापेक्षतः काष्ठ-प्रतिमाएँ कम मिलती हैं। विशेष करके इसका प्रयोग भवननिर्माणमें होता था। परन्तु जैनवास्सुघिषयक ग्रन्थोंमें काष्ठ
Aho! Shrutgyanam