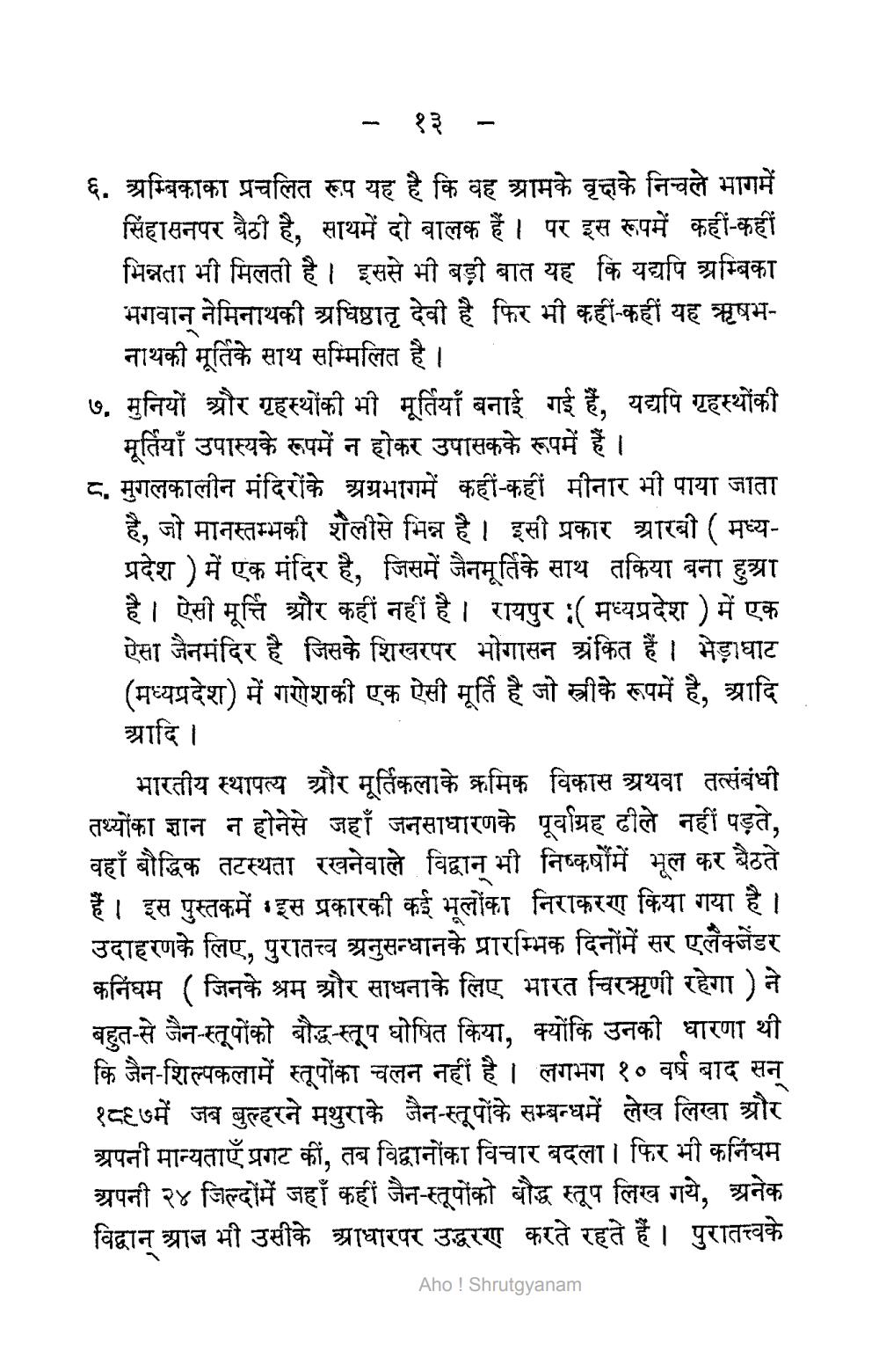________________
- १३ - ६. अम्बिकाका प्रचलित रूप यह है कि वह अामके वृक्षके निचले भागमें सिंहासनपर बैठी है, साथमें दो बालक हैं । पर इस रूपमें कहीं-कहीं भिन्नता भी मिलती है। इससे भी बड़ी बात यह कि यद्यपि अम्बिका भगवान नेमिनाथकी अधिष्ठातृ देवी है फिर भी कहीं-कहीं यह ऋषभ
नाथकी मूर्तिके साथ सम्मिलित है। ७. मुनियों और गृहस्थोंकी भी मूर्तियाँ बनाई गई हैं, यद्यपि गृहस्थोंकी
मूर्तियाँ उपास्यके रूपमें न होकर उपासकके रूपमें हैं। ८. मुगलकालीन मंदिरोंके अग्रभागमें कहीं-कहीं मीनार भी पाया जाता
है, जो मानस्तम्भकी शैलीसे भिन्न है। इसी प्रकार प्रारबी ( मध्यप्रदेश ) में एक मंदिर है, जिसमें जैनमूर्तिके साथ तकिया बना हुअा है। ऐसी मूर्ति और कहीं नहीं है। रायपुर :( मध्यप्रदेश ) में एक ऐसा जैनमंदिर है जिसके शिखरपर भोगासन अंकित हैं । भेड़ाघाट (मध्यप्रदेश) में गणेशकी एक ऐसी मूर्ति है जो स्त्रीके रूपमें है, आदि आदि ।
भारतीय स्थापत्य और मूर्तिकलाके क्रमिक विकास अथवा तत्संबंधी तथ्योंका ज्ञान न होनेसे जहाँ जनसाधारणके पूर्वाग्रह ढीले नहीं पड़ते, वहाँ बौद्धिक तटस्थता रखनेवाले विद्वान् भी निष्कर्षों में भूल कर बैठते हैं। इस पुस्तकमें । इस प्रकारकी कई भूलोंका निराकरण किया गया है । उदाहरणके लिए, पुरातत्त्व अनुसन्धानके प्रारम्भिक दिनों सर एलेक्जेंडर कनिंघम (जिनके श्रम और साधनाके लिए भारत चिरऋणी रहेगा ) ने बहुत-से जैन-स्तूपोंको बौद्ध स्तूप घोषित किया, क्योंकि उनको धारणा थी कि जैन-शिल्पकलामें स्तूपोंका चलन नहीं है । लगभग १० वर्ष बाद सन् १८६७में जब बुल्हरने मथुराके जैन-स्तूपोंके सम्बन्धमें लेख लिखा और अपनी मान्यताएँ प्रगट की, तब विद्वानोंका विचार बदला। फिर भी कनिंघम अपनी २४ जिल्दोंमें जहाँ कहीं जैन-स्तूपोंको बौद्ध स्तूप लिख गये, अनेक विद्वान आज भी उसीके अाधारपर उद्धरण करते रहते हैं। पुरातत्त्वके
Aho ! Shrutgyanam