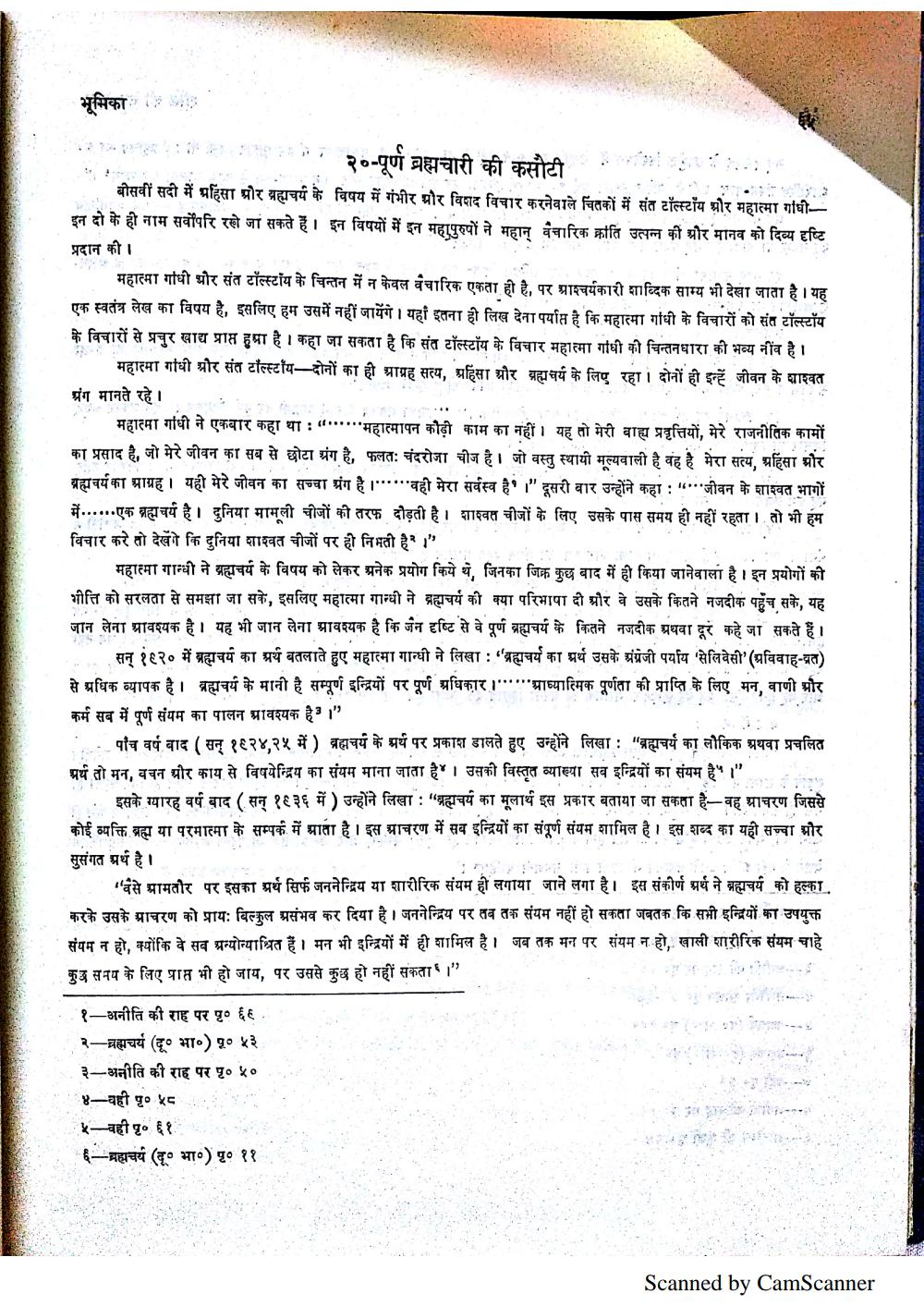________________
भूमिका
बीसवीं सदी में हिंसा और ब्रह्मचर्य के इन दो के ही नाम सर्वोपरि रखे जा सकते हैं। प्रदान की।
महात्मा गांधी धौर संत टॉल्स्टॉय के चिन्तन में न केवल वैचारिक एकता ही है. पर धावकारी शाब्दिक साम्य भी देखा जाता है। यह एक स्वतंत्र लेख का विषय है, इसलिए हम उसमें नहीं जायेंगे। यहाँ इतना ही लिख देना पर्याप्त है कि महात्मा गांधी के विचारों को संत टॉल्स्टॉय के विचारों से प्रचुर खाद्य प्राप्त हुआ है। कहा जा सकता है कि संत टॉल्स्टॉय के विचार महात्मा गांधी की चिन्तनधारा की भव्य नींव है । महात्मा गांधी और संत टॉल्स्टॉय दोनों का ही धाग्रह सत्य, पहिया धीर ब्रह्मचर्य के लिए रहा। दोनों ही इन्हें जीवन के पा अंग मानते रहे।
२०- पूर्ण ब्रह्मचारी की कसौटी
विषय में गंभीर और विशद विचार करनेवाले चिंतकों में संत टॉल्स्टॉय और महात्मा गांधीइन विषयों में इन महापुरुषों ने महान वैचारिक क्रांति उत्पन्न की धौर मानव को दिव्य दृष्टि
:
महात्मा गांधी ने एकबार कहा था महात्मापन कौड़ी काम का नहीं यह तो मेरी बाह्य प्रवृत्तियों, मेरे राजनीतिक कामों का प्रसाद है, जो मेरे जीवन का सब से छोटा अंग है, फलतः चंदरोजा चीज है। जो वस्तु स्थायी मूल्यवाली है वह है मेरा सत्य, अहिंसा और ब्रह्मचर्य का यही मेरे जीवन का सच्चा चंग है। बड़ी मेरा सर्वस्व है " दूसरी बार उन्होंने कहा में...... एक ब्रह्मचर्य है। दुनिया मामूली चीजों की तरफ दौड़ती है। शाश्वत चीजों के लिए उसके पास समय ही नहीं रहता। तो भी हम विचार करे तो देखने कि दुनिया शाश्वत चीजों पर हो निमती है" "
जीवन के सात भागों
शाश्वत
महात्मा गान्धी ने ब्रह्मचर्य के विषय को लेकर अनेक प्रयोग किये थे, जिनका जिक्र कुछ बाद में ही किया जानेवाला है। इन प्रयोगों की भीत्ति को सरलता से समझा जा सके, इसलिए महात्मा गान्धी ने ब्रह्मचर्य की क्या परिभाषा दी और वे उसके कितने नजदीक पहुँच सके, यह जान लेना आवश्यक है। यह भी जान लेना आवश्यक है कि जैन दृष्टि से ये पूर्ण ब्रह्मचर्य के कितने नजदीक अथवा दूरं कहे जा सकते हैं।
सन् १९२० में ब्रह्मचर्य का अर्थ बतलाते हुए महात्मा गान्धी ने लिखा "ब्रह्मचर्य का पर्व उसके अंग्रेजी पर्याय 'सेलिवेसी (विवाह-प्रत से अधिक व्यापक है । ब्रह्मचर्य के मानी है सम्पूर्ण इन्द्रियों पर पूर्ण अधिकार ..... घाध्यात्मिक पूर्णता की प्राप्ति के लिए मन, वाणी और कर्म सब में पूर्ण संयम का पालन श्रावश्यक है ।"
:
बाद (१९२४, २५ में) ब्रह्मचर्य के अर्थ पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने तिला "ब्रह्मचर्य का लौकिक अथवा प्रचलित अर्थ तो मन, वचन धीर काय से विषयेन्द्रिय का संयम माना जाता है। उसकी विस्तृत व्याख्या सब इन्द्रियों का संयम है५ ।"
इसके ग्यारह वर्ष बाद ( सन् १९३६ में ) उन्होंने लिखा : " ब्रह्मचर्य का मूलार्थ इस प्रकार बताया जा सकता है- वह श्राचरण जिससे कोई व्यक्ति ब्रह्म या परमात्मा के सम्पर्क में आता है । इस आचरण में सब इन्द्रियों का संपूर्ण संयम शामिल है। इस शब्द का यही सच्चा और सुसंगत अर्थ है ।
"वैसे आमतौर पर इसका अर्थ सिर्फ जननेन्द्रिय या शारीरिक संयम ही लगाया जाने लगा है। इस संकीर्ण अर्थ ने ब्रह्मचर्य को हल्का करके उसके प्राचरण को प्रायः बिल्कुल असंभव कर दिया है। जननेन्द्रिय पर तब तक संयम नहीं हो सकता जबतक कि सभी इन्द्रियों का उपयुक्त संयम न हो, क्योंकि वे सब अन्योन्याश्रित हैं। मन भी इन्द्रियों में ही शामिल है। जब तक मन पर संयम न हो, खाली शारीरिक संयम चाहे कुछ समय के लिए पास भी हो जाय, पर उससे कुछ हो नहीं सकता।"
१- अनीति की राह पर पृ० ६६.
२ – ब्रह्मचर्य (दू० भा०) १० ५३
३- अनीति की राह पर पृ० ५०
४ - वही पृ० ५८ ५यही पृ० ६१ ६-महाचर्य (० भा०) पृ० ११
Scanned by CamScanner