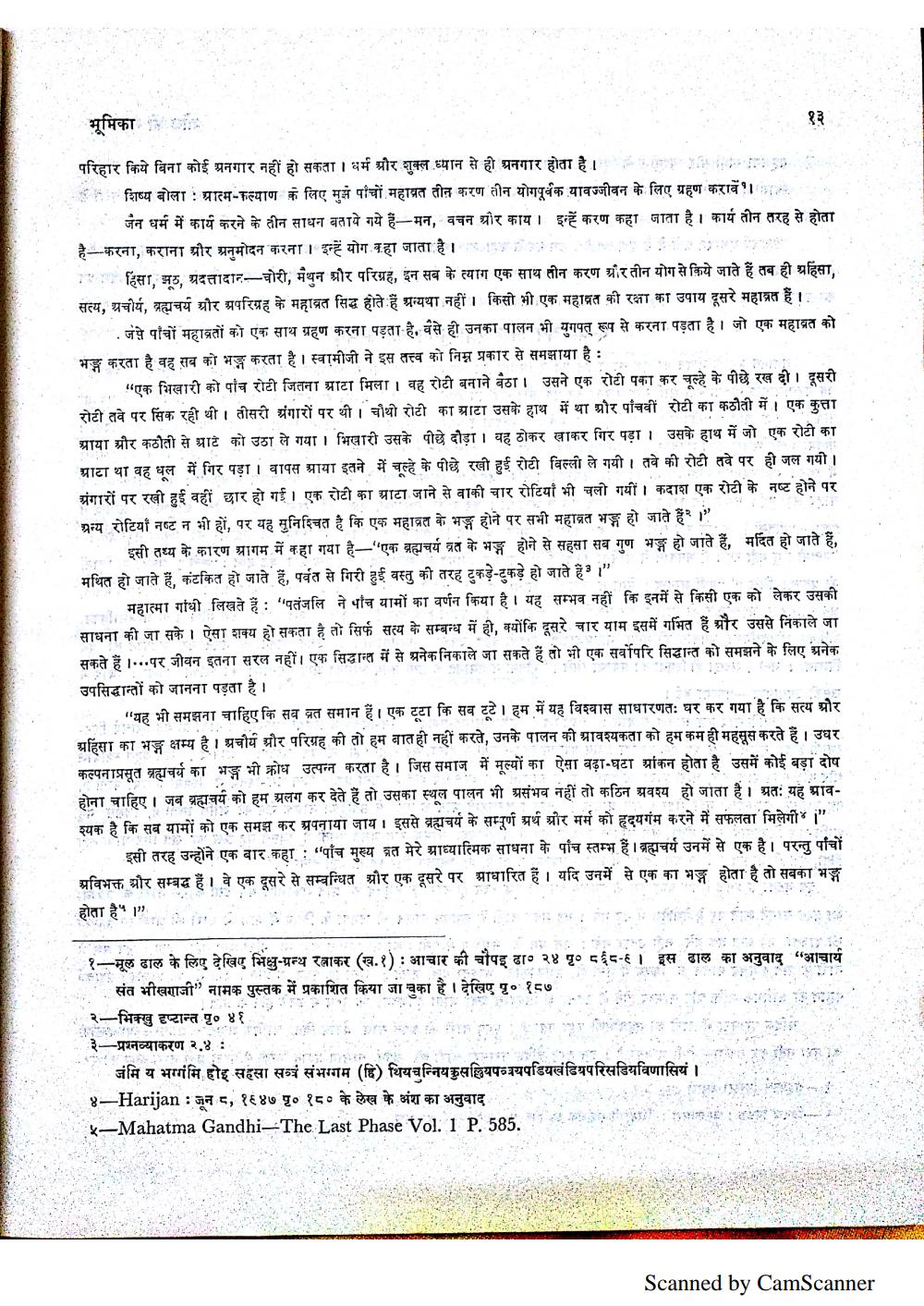________________
भूमिका
परिहार किये बिना कोई अनगार नहीं हो सकता। धर्म और शुक्ल ध्यान से ही अनगार होता है ।
20
शिष्य बोला : ग्रात्म-कल्याण के लिए मुझे पाँचों महाव्रत तीन करण तीन योगपूर्वक यावज्जीवन के लिए ग्रहण करावें ? | जैन धर्म में कार्य करने के तीन साधन बताये गये हैं— मन, वचन और काय । इन्हें करण कहा जाता है। कार्य तीन तरह से होता है— करना, कराना और अनुमोदन करना। इन्हें योग कहा जाता है ।
हिंसा, झूठ, श्रदत्तादान - चोरी, मैथुन और परिग्रह, इन सब के त्याग एक साथ तीन करण और तीन योग से किये जाते हैं तब ही श्रहिंसा, सत्य, श्रचीर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह के महाव्रत सिद्ध होते हैं अन्यथा नहीं। किसी भी एक महाव्रत की रक्षा का उपाय दूसरे महाव्रत हैं ।
. जेसे पाँचों महाव्रतों को एक साथ ग्रहण करना पड़ता है, वैसे ही उनका पालन भी युगपत् रूप से करना पड़ता है। जो एक महाव्रत को भङ्ग करता है वह सब को भङ्ग करता है। स्वामीजी ने इस तत्त्व को निम्न प्रकार से समझाया है :
"एक भिखारी को पांच रोटी जितना श्राटा मिला। वह रोटी बनाने बैठा। उसने एक रोटी पका कर चूल्हे के पीछे रख दी। दूसरी रोटी तवे पर सिंक रही थी। तीसरी अंगारों पर थी। चौथी रोटी का घाटा उसके हाथ में था और पांचवीं रोटी का कठौती में एक कुत्ता आया और कठौती से घाटे को उठा ले गया। भिखारी उसके पीछे दौड़ा। यह ठोकर खाकर गिर पड़ा। उसके हाथ में जो एक रोटी का घाटा था वह धूल में गिर पड़ा। वापस आया इतने में चूल्हे के पीछे रखी हुई रोटी बिल्ली ले गयी । तवे की रोटी तवे पर ही जल गयी । अंगारों पर रखी हुई वहीं छार हो गई। एक रोटी का आटा जाने से बाकी चार रोटियां भी चली गयीं। कदाश एक रोटी के नष्ट होने पर अन्य रोटियाँ नष्ट न भी हों, पर यह सुनिश्चित है कि एक महाव्रत के भङ्ग होने पर सभी महाव्रत भङ्ग हो जाते हैं ।"
इसी तथ्य के कारण श्रागम में कहा गया है- "एक ब्रह्मचर्य व्रत के भङ्ग होने से सहसा सब गुण भङ्ग हो जाते हैं, मदित हो जाते हैं, मत हो जाते हैं, कंति हो जाते हैं, पर्वत से घिरी हुई वस्तु की तरह टुकड़े-टुकड़े हो जाते है" "
महात्मा गांधी लिखते हैं: "पतंजलि ने पाँच यामों का वर्णन किया है। यह सम्भव नहीं कि इनमें से किसी एक को लेकर उसकी साधना की जा सके। ऐसा शक्य हो सकता है तो सिर्फ सत्य के सम्बन्ध में ही, क्योंकि दूसरे चार याम इसमें गर्भित हैं और उससे निकाले जा सकते हैं।... पर जीवन इतना सरल नहीं। एक सिद्धान्त में से अनेक निकाले जा सकते हैं तो भी एक सर्वोपरि सिद्धान्त को समझने के लिए अनेक उपसिद्धान्तों को जानना पड़ता है।
१३
"यह भी समझना चाहिए कि सब व्रत समान हैं। एक टूटा कि सब टूटे। हम में यह विश्वास साधारणतः घर कर गया है कि सत्य श्रीर अहिंसा का भङ्ग क्षम्य है । अचौर्य और परिग्रह की तो हम बात ही नहीं करते, उनके पालन की श्रावश्यकता को हम कम ही महसूस करते हैं। उधर कल्पनाप्रसूत ब्रह्मचर्य का भङ्ग भी क्रोध उत्पन्न करता है। जिस समाज में मूल्यों का ऐसा बढ़ा-घटा ग्रांकन होता है उसमें कोई बड़ा दोष होना चाहिए। जब ब्रह्मचर्य को हम अलग कर देते हैं तो उसका स्थूल पालन भी असंभव नहीं तो कठिन अवश्य हो जाता है। अतः यह भावश्यक है कि सब यामों को एक समझ कर अपनाया जाय। इससे ब्रह्मचर्य के सम्पूर्ण अर्थ और मर्म को हृदयगंम करने में सफलता मिलेगी ।"
४
पाँचों इसी तरह उन्होंने एक बार कहा “पाँच मुख्य व्रत मेरे प्राध्यात्मिक साधना के पाँच स्तम्भ हैं। ब्रह्मचर्य उनमें से एक है । परन्तु अविभक्त और सम्बद्ध हैं । वे एक दूसरे से सम्बन्धित और एक दूसरे पर आधारित हैं। यदि उनमें से एक का भङ्ग होता है तो सबका भङ्ग होता है" । "
१- मूल ढाल के लिए देखिए भिक्षु ग्रन्थ रत्नाकर (ख. १) आचार की चौपइ ढा० २४ पृ० ८६८-६ । इस ढाल का अनुवाद “आचार्य संत भीखगाजी" नामक पुस्तक में प्रकाशित किया जा चुका है। देखिए पृ० १८७
- भिक्खु दृष्टान्त पृ० ४१
१३- प्रश्नव्याकरण २.४
संभग्गम (हि) थियचन्निय कुस लियपव्त्रयपडियखंडिय परिसडियविणासियं । १८० के लेख के अंश का अनुवाद
जंमिय भग्गमि होइ सहसा स
४— Harijan : जून ८, १६४७ पृ० ५- Mahatma Gandhi - The Last Phase Vol. 1P.585.
Scanned by CamScanner