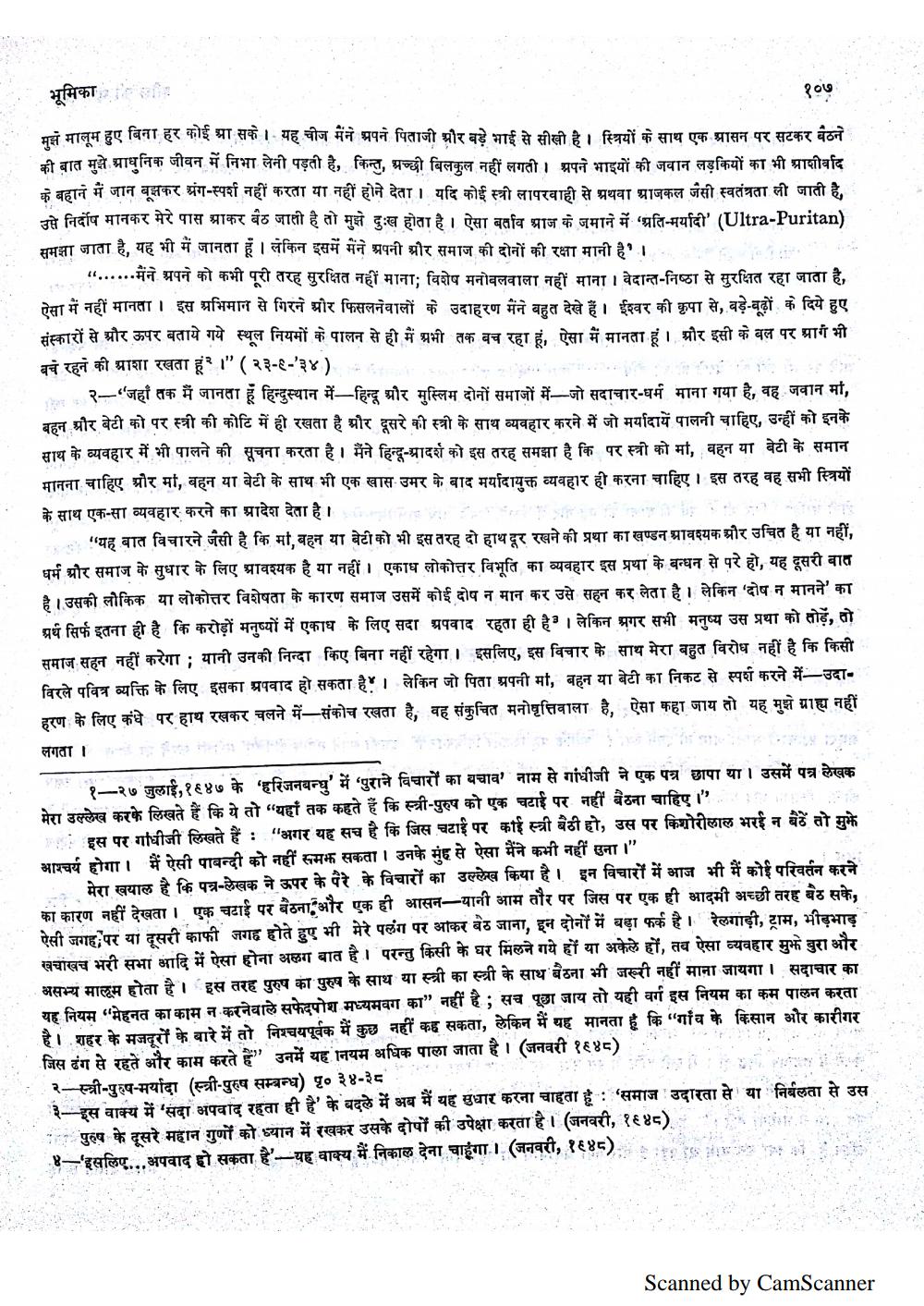________________
भूमिका
ofs
१०७
मुझे मालूम हुए बिना हर कोई था सके। यह चीज मैंने अपने पिताजी और बड़े भाई से सीखी है। स्त्रियों के साथ एक मासन पर पटकर बैठने की बात मुझे आधुनिक जीवन में निभा लेनी पड़ती है, किन्तु, अच्छी बिलकुल नहीं लगती । श्रपने भाइयों की जवान लड़कियों का भी आशीर्वाद के बहाने में जान बूझकर अंग स्पर्श नहीं करता या नहीं होने देता। यदि कोई स्त्री लापरवाही से अथवा भाजकल जैसी स्वतंत्रता सी जाती है, उसे निर्दोष मानकर मेरे पास आकर बैठ जाती है तो मुझे दुःख होता है । ऐसा बर्ताव आज के जमाने में 'श्रति-मर्यादी' (Ultra-Puritan) समझा जाता है, यह भी मैं जानता हूँ । लेकिन इसमें मैंने अपनी और समाज की दोनों की रक्षा मानी है' ।
........मैंने अपने को कभी पूरी तरह सुरक्षित नहीं माना विशेष मनोबलवाला नहीं माना। वेदान्त-निष्ठा से सुरक्षित रहा जाता है, ऐसा मैं नहीं मानता । इस अभिमान से गिरने और फिसलनेवालों के उदाहरण मैंने बहुत देखे हैं । ईश्वर की कृपा से, बड़े-बूढ़ों के दिये हुए संस्कारों से और ऊपर बताये गये स्थूल नियमों के पालन से ही में अभी तक बच रहा हूं, ऐसा में मानता हूँ और इसी के बल पर धागे भी बचे रहने की आशा रखता हूं।" ( २३-९-२३४ )
२ - " जहाँ तक मैं जानता हूँ हिन्दुस्थान में – हिन्दू और मुस्लिम दोनों समाजों में— जो सदाचार-धर्म माना गया है, वह जवान मां, और बेटी को पर स्त्री की कोटि में ही रखता है और दूसरे की स्त्री के साथ व्यवहार करने में जो मर्यादायें पालनी चाहिए, उन्हीं को इनके बहन साथ के व्यवहार में भी पालने की सूचना करता है। मैंने हिन्दू-आदर्श को इस तरह समझा है कि पर स्त्री को मां, वहन या बेटी के समान मानना चाहिए और मां, बहन या बेटी के साथ भी एक खास उमर के बाद मर्यादायुक्त व्यवहार ही करना चाहिए। इस तरह वह सभी स्त्रियों के साथ एक-सा व्यवहार करने का प्रादेश देता है ।
अर्थ सिर्फ इतना ही है कि करोड़ों मनुष्यों में एकाध के लिए सदा अपवाद रहता ही है। लेकिन समाज सहन नहीं करेगा; यानी उनकी निन्दा किए बिना नहीं रहेगा । इसलिए, इस विचार के विरले पवित्र व्यक्ति के लिए इसका अपवाद हो सकता है। लेकिन जो पिता अपनी मां, बहन या हरण के लिए कंधे पर हाथ रखकर चलने में संकोच रखता है, वह संकुचित मनोवृत्तिवाला है,
"यह बात विचारने जैसी है कि मां, बहन या बेटी को भी इस तरह दो हाथ दूर रखने की प्रथा का खण्डन आवश्यक और उचित है या नहीं, धर्म और समाज के सुधार के लिए आवश्यक है या नहीं । एकाध लोकोत्तर विभूति का व्यवहार इस प्रथा के बन्धन से परे हो, यह दूसरी बात है। उसकी लौकिक या लोकोत्तर विशेषता के कारण समाज उसमें कोई दोष न मान कर उसे सहन कर लेता है लेकिन 'दोष न मानने' का अगर सभी मनुष्य उस प्रथा को तोड़ें, तो साथ मेरा बहुत विरोध नहीं है कि किसी बेटी का निकट से स्पर्श करने में— उदाऐसा कहा जाय तो यह मुझे ग्राह्य नहीं
लगता ।
नाम से गांधीजी ने एक पत्र छापा था। उसमें पत्र लेखक चटाई पर नहीं बैठना चाहिए
१ – २७ जुलाई, १९४७ के 'हरिजनबन्धु' में 'पुराने विचारों का बचाव' मेरा उल्लेख करके लिखते हैं कि ये तो "यहां तक कहते हैं कि स्त्री-पुरुष को एक इस पर गांधीजी लिखते हैं "अगर यह सच है कि जिस पटाई पर कोई स्त्री बैठी हो, उस पर किशोरीखाल भरई न बैठे तो मुके आश्चर्य होगा । मैं ऐसी पाबन्दी को नहीं समझ सकता। उनके मुंह से ऐसा मैंने कभी नहीं सुना ।"
:
मेरा खयाल है कि पत्र लेखक ने ऊपर के धेरे के विचारों का उल्लेख किया है। इन विचारों में आज भी में कोई परिवर्तन करने
का कारण नहीं देखता । एक चटाई पर बैठना और एक ही आसन - यानी आम तौर पर जिस पर एक ही आदमी अच्छी तरह स ऐसी जगह पर या दूसरी काफी जगह होते हुए भी मेरे पलंग पर आकर बैठ जाना, इन दोनों में बड़ा फर्क है। रेलगाड़ी, ट्राम, भीड़भाड़ खचाखच भरी सभा आदि में ऐसा होना अलग बात है । परन्तु किसी के घर मिलने गये हों या अकेले हों, तब ऐसा व्यवहार मुझे बुरा और असभ्य मालूम होता है । इस तरह पुरुष का पुरुष के साथ या स्त्री का स्त्री के साथ बैठना भी जरूरी नहीं माना जायगा । सदाचार यह नियम “मेहनत का काम न करनेवाले सफेदपोश मध्यमवग का” नहीं है; सच पूछा जाय तो यही वर्ग इस नियम का कम पालन करता है। शहर के मजदूरों के बारे में तो निश्चयपूर्वक में कुछ नहीं कह सकता, लेकिन में यह मानता हूँ कि गाँव के किसान और कारीगर जिस ढंग से रहते और काम करते हैं" उनमें यह नियम अधिक पाला जाता है । ( जनवरी १६४८ )
२ - स्त्री - पुरुष - मर्यादा ( स्त्री-पुरुष सम्बन्ध ) पृ० ३४-३८
३- इस वाक्य में 'सदा अपवाद रहता ही है' के बदले में अब मैं यह सुधार करना चाहता हूँ 'समाज उदारता से या निर्बलता से उस पुरुष के दूसरे महान गुणों को ध्यान में रखकर उसके दोषों की उपेक्षा करता है। (जनवरी, १६४८ )
- इसलिए... अपवाद हो सकता है' यह वाक्य मैं निकाल देना चाहूंगा। (जनवरी, १६४८)
Scanned by CamScanner