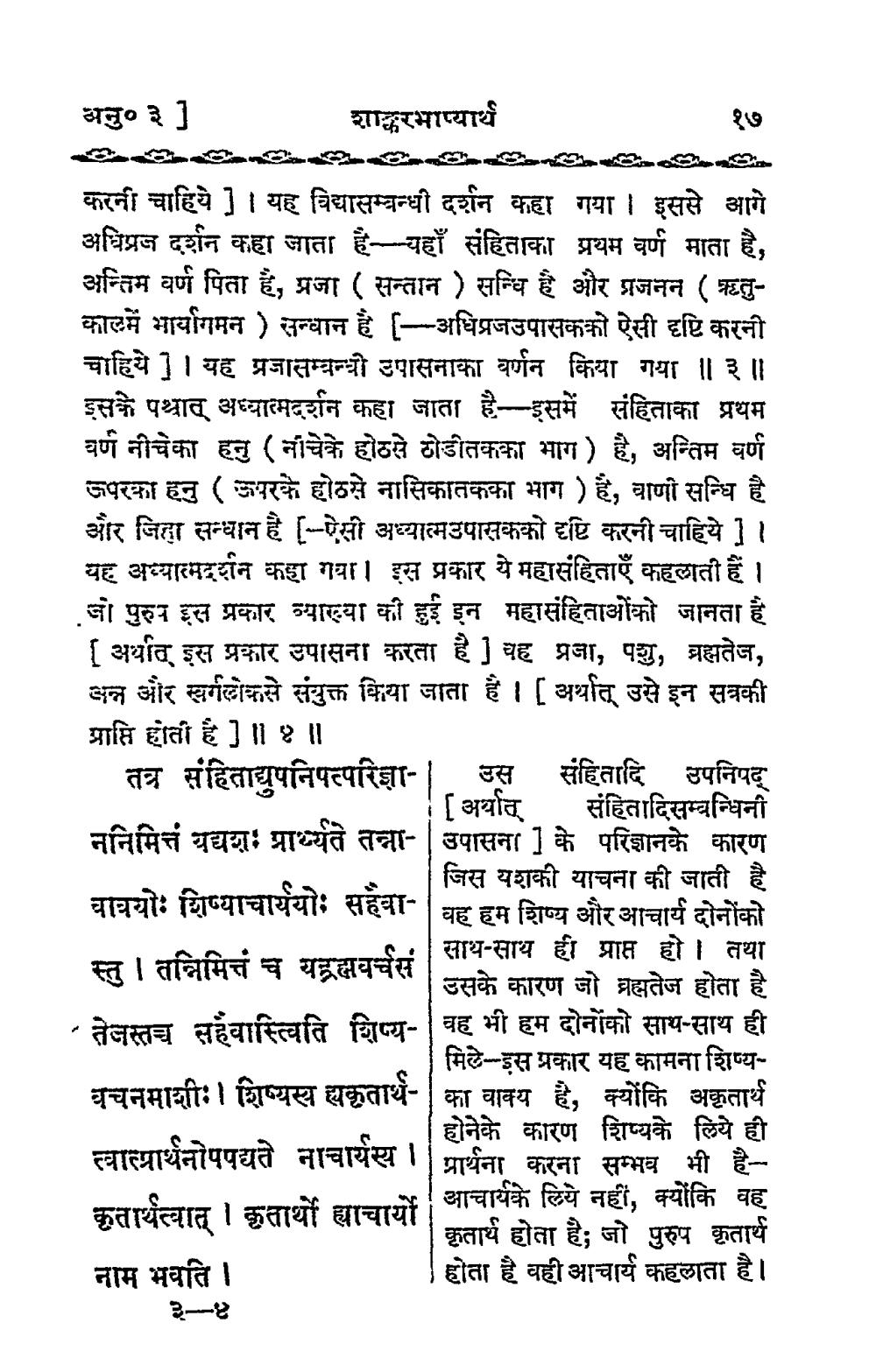________________
अनु० ३]
शारभाप्यार्थ
करनी चाहिये] । यह विद्यासम्बन्धी दर्शन कहा गया। इससे आगे अधिप्रज दर्शन कहा जाता है-यहाँ संहिताका प्रथम वर्ण माता है, अन्तिम वर्ण पिता है, प्रजा ( सन्तान ) सन्धि है और प्रजनन (ऋतुकालमें भार्यागमन ) सन्धान है -अधिप्रजउपासकको ऐसी दृष्टि करनी चाहिये ] । यह प्रजासम्बन्धी उपासनाका वर्णन किया गया ॥ ३ ॥ इसके पश्चात् अध्यात्मदर्शन कहा जाता है-इसमें संहिताका प्रथम वर्ण नीचेका हनु (नांचेके होठसे ठोडीतकका भाग) है, अन्तिम वर्ण जपरका हनु (ऊपरके होठसे नासिकातकका भाग ) है, वाणी सन्धि है और जिला सन्धान है [-ऐसी अध्यात्मउपासकको दृष्टि करनी चाहिये । यह अध्यात्मदर्शन कहा गया। इस प्रकार ये महासंहिताएँ कहलाती हैं। जो पुरुष इस प्रकार व्याख्या की हुई इन महासंहिताओंको जानता है [ अर्थात् इस प्रकार उपासना करता है वह प्रजा, पशु, ब्रह्मतेज, अन्न और स्वर्गलोकसे संयुक्त किया जाता है। [अर्थात् उसे इन सबकी प्राप्ति होती है ] ॥ ४ ॥ तत्र संहिताद्युपनिपत्परिज्ञा- उस संहितादि उपनिपद्
[अर्थात् संहितादिसम्बन्धिनी ननिमित्तं यद्यशःप्रार्थ्यते तन्ना- | उपासना ] के परिज्ञानके कारण
| जिस यशकी याचना की जाती है चावयोः शिष्याचार्ययोः सहवा- | वह हम शिष्य और आचार्य दोनोंको
साथ-साथ ही प्राप्त हो। तथा स्तु | तन्निमित्तं च यद्रह्मवर्चसं
उसके कारण जो ब्रह्मतेज होता है - तेजस्तच सहवास्त्विति शिष्य- वह भी हम दोनोंको साथ-साथ ही
मिले-इस प्रकार यह कामना शिष्यवचनमाशी। शिष्यस्य यकृतार्थ- का वाक्य है, क्योंकि अकृतार्थ
होनेके कारण शिप्यके लिये ही वात्प्रार्थनोपपद्यते नाचार्यस्य । प्रार्थना करना सम्भव भी हैकृतार्थत्वात । कृतार्थो ह्याचार्यो आचार्यके लिये नहीं, क्योंकि वह
कृतार्थ होता है। जो पुरुप कृतार्थ नाम भवति ।
होता है वही आचार्य कहलाता है।