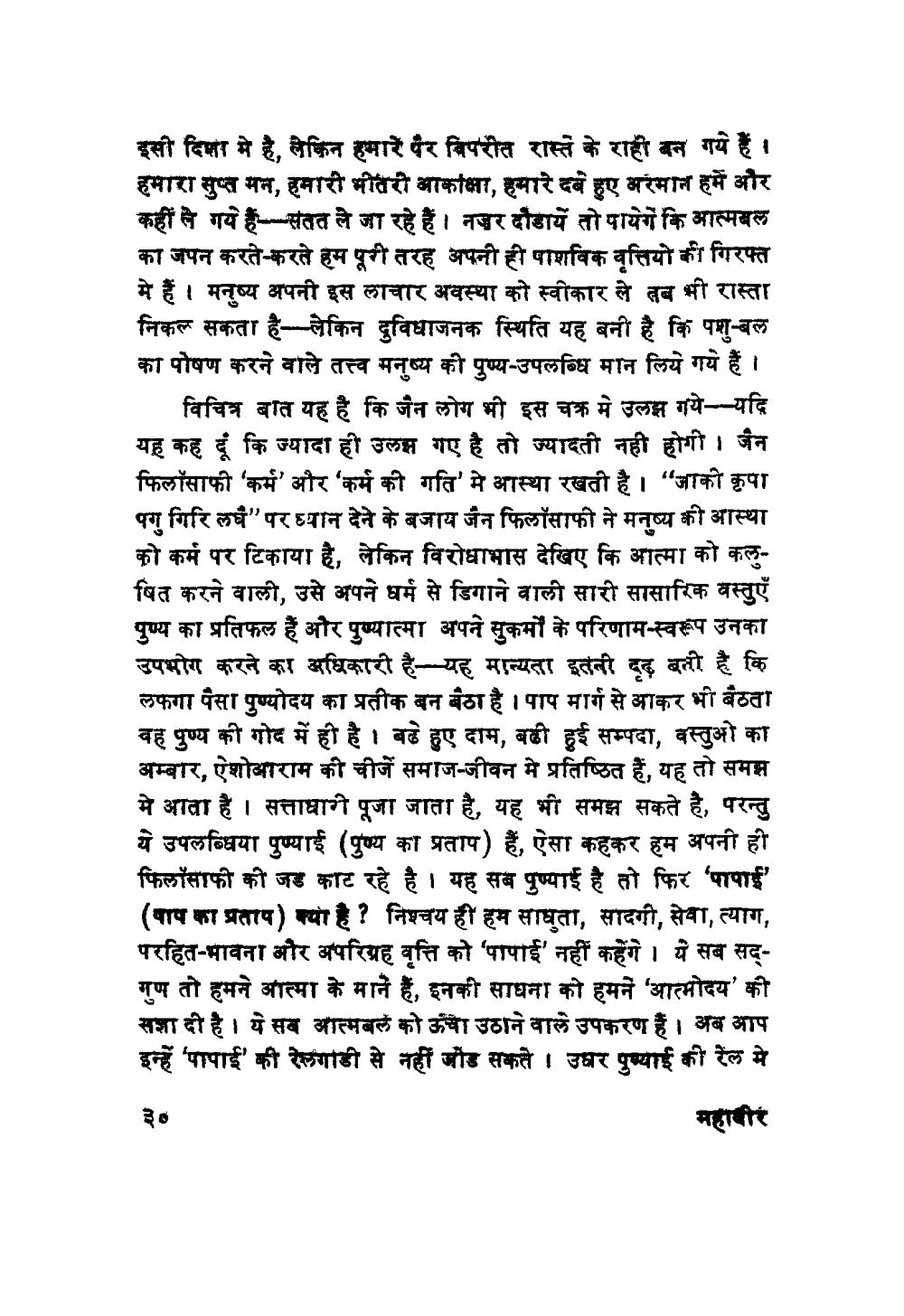________________
इसी दिशा मे है, लेकिन हमारे पर विपरीत रास्ते के राही बन गये हैं। हमारा सुप्त मन, हमारी भीतरी आकांक्षा, हमारे दबे हए अरमान हमें और कहीं ले गये हैं. सतत ले जा रहे हैं। नजर दौडायें तो पायेगें कि आत्मबल का जपन करते-करते हम पूरी तरह अपनी ही पाशविक वृत्तियो की गिरफ्त मे हैं। मनुष्य अपनी इस लाचार अवस्था को स्वीकार ले बब भी रास्ता निकल सकता है लेकिन दुविधाजनक स्थिति यह बनी है कि पशु-बल का पोषण करने वाले तत्त्व मनुष्य की पुण्य-उपलब्धि मान लिये गये हैं।
विचित्र बात यह है कि जैन लोग भी इस चक्र मे उलझ गये यदि यह कह दूं कि ज्यादा ही उलझ गए है तो ज्यादती नही होगी। जैन फिलॉसाफी 'कर्म' और 'कर्म की गति' में आस्था रखती है। "जाको कृपा पगु गिरि लघ" पर ध्यान देने के बजाय जैन फिलॉसाफी ने मनुष्य की आस्था को कर्म पर टिकाया है, लेकिन विरोधाभास देखिए कि आत्मा को कलुषित करने वाली, उसे अपने धर्म से डिगाने वाली सारी सासारिक वस्तुएँ पुण्य का प्रतिफल हैं और पुण्यात्मा अपने सुकर्मों के परिणाम स्वरूप उनका उपभोग करने का अधिकारी है- यह मान्यता इतनी दृढ़ बनी है कि लफगा पैसा पुण्योदय का प्रतीक बन बैठा है । पाप मार्ग से आकर भी बैठता वह पुण्य की गोद में ही है। बढे हुए दाम, बढी हुई सम्पदा, वस्तुओ का अम्बार, ऐशोआराम की चीजें समाज-जीवन में प्रतिष्ठित हैं, यह तो समझ मे आता है । सत्ताधारी पूजा जाता है, यह भी समझ सकते है, परन्तु ये उपलब्धिया पुण्याई (पुण्य का प्रताप) हैं, ऐसा कहकर हम अपनी ही फिलॉसाफी की जड काट रहे है । यह सब पुण्याई है तो फिर 'पापाई (पाप का प्रताप) क्या है? निश्चय ही हम साधुता, सादगी, सेवा, त्याग, परहित-भावना और अपरिग्रह वृत्ति को 'पापाई' नहीं कहेंगे। ये सब सद्गुण तो हमने आत्मा के माने हैं, इनकी साधना को हमने 'आत्मोदय' की सज्ञा दी है। ये सब आत्मबले को ऊंचा उठाने वाले उपकरण हैं। अब आप इन्हें 'पापाई की रेलगाडी से नहीं जोड सकते । उधर पुण्याई की रेल मे