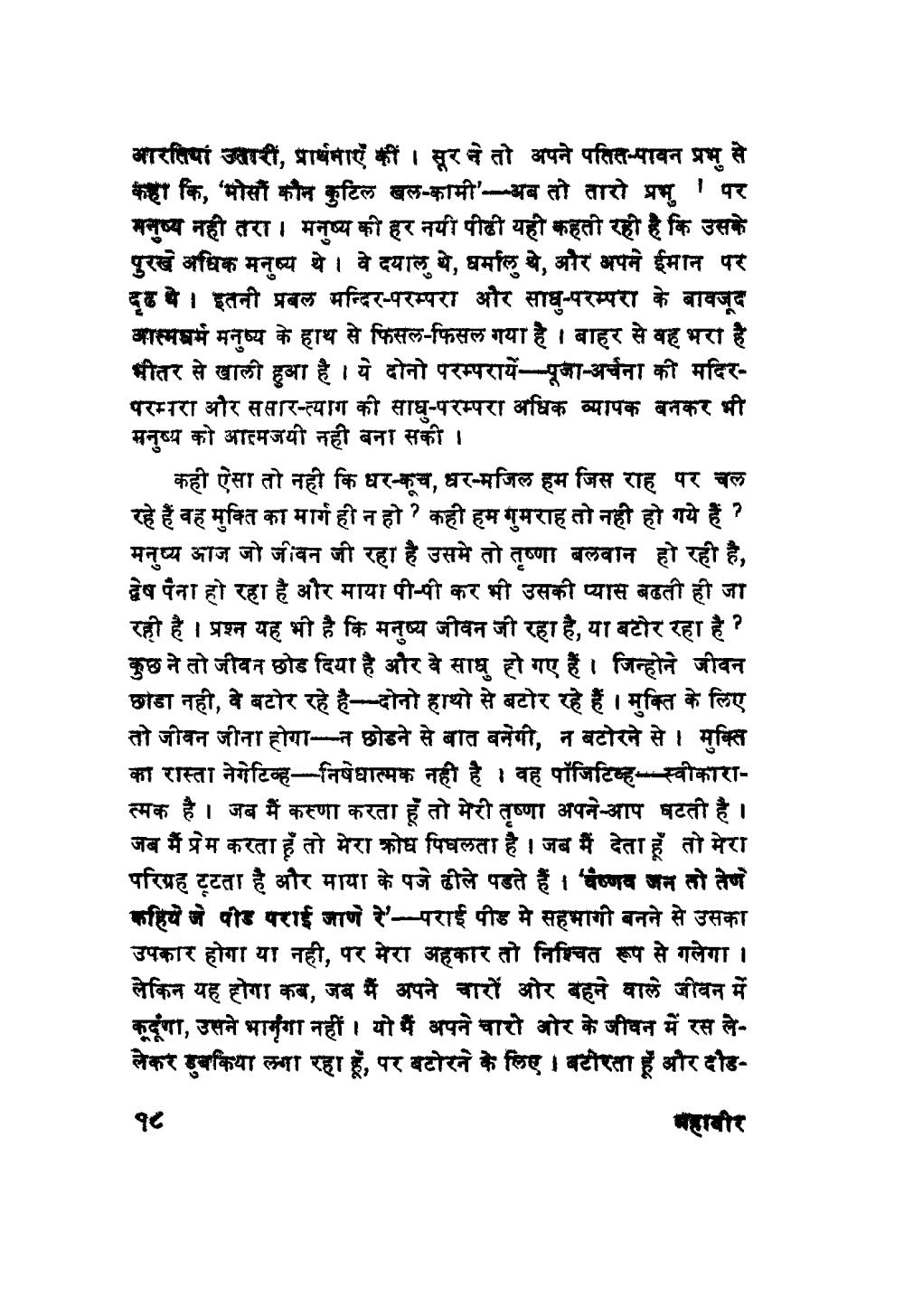________________
भारतियां उतारी, प्रार्थमाएँ की । सूर ने तो अपने पतित-पावन प्रभु से कहा कि, 'मोसौं कौन कुटिल खल-कामी'- अब तो तारो प्रभु । पर मनुष्य नही तरा। मनुष्य की हर नयी पीढी यही कहती रही है कि उसके पुरखे अधिक मनुष्य थे। वे दयालु थे, धर्मालु थे, और अपने ईमान पर दृढ थे। इतनी प्रबल मन्दिर-परम्परा और साधु-परम्परा के बावजूद आत्मधर्म मनुष्य के हाथ से फिसल-फिसल गया है । बाहर से वह भरा है भीतर से खाली हुआ है । ये दोनो परम्परायें-पूजा-अर्चना की मदिरपरम्भरा और ससार-त्याग की साधु-परम्परा अधिक व्यापक बनकर भी मनुष्य को आत्मजयी नही बना सकी।
कही ऐसा तो नही कि धर-कच, धर-मजिल हम जिस राह पर चल रहे हैं वह मुक्ति का मार्ग ही न हो? कही हम गुमराह तो नही हो गये हैं ? मनुष्य आज जो जीवन जी रहा है उसमे तो तृष्णा बलवान हो रही है, द्वेष पैना हो रहा है और माया पी-पी कर भी उसकी प्यास बढ़ती ही जा रही है। प्रश्न यह भी है कि मनुष्य जीवन जी रहा है, या बटोर रहा है ? कुछ ने तो जीवन छोड दिया है और वे साधु हो गए हैं। जिन्होने जीवन छोडा नही, वे बटोर रहे है-दोनो हाथो से बटोर रहे हैं । मुक्ति के लिए तो जीवन जीना होगा-न छोडने से बात बनेगी, न बटोरने से । मुक्ति का रास्ता नेगेटिव्ह-निषेधात्मक नहीं है । वह पॉजिटिव्ह स्वीकारात्मक है। जब मैं करुणा करता हूँ तो मेरी तृष्णा अपने-आप घटती है। जब मैं प्रेम करता हूँ तो मेरा क्रोध पिघलता है । जब मैं देता हूँ तो मेरा परिग्रह टूटता है और माया के पजे ढीले पडते हैं । 'वैष्णव जन तो तेणे कहिये जे पीड पराई जाणे रें--पराई पीड मे सहभागी बनने से उसका उपकार होगा या नही, पर मेरा अहकार तो निश्चित रूप से गलेगा। लेकिन यह होगा कब, जब मैं अपने चारों ओर बहने वाले जीवन में कूदूंगा, उसने भागा नहीं। यो मैं अपने चारो ओर के जीवन में रस लेलेकर मुबकिया लगा रहा हूँ, पर बटोरने के लिए । बटोरता हूँ और दौड