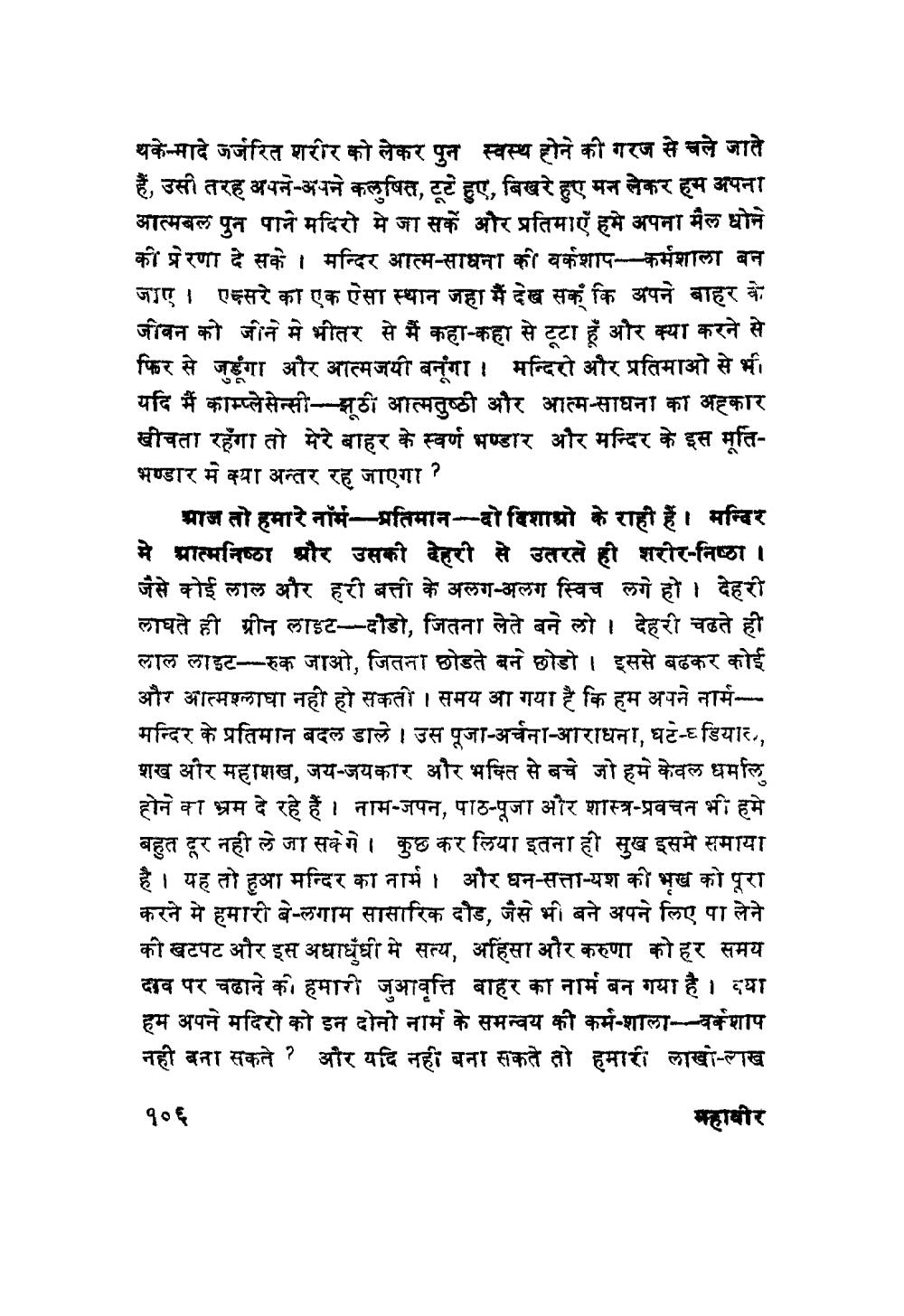________________
थके-मादे जर्जरित शरीर को लेकर पुन स्वस्थ होने की गरज से चले जाते हैं, उसी तरह अपने-अपने कलुषित, टे हए, बिखरे हुए मन लेकर हम अपना आत्मबल पुन पाने मदिरो मे जा सकें और प्रतिमाएँ हमे अपना मैल धोने की प्रेरणा दे सके । मन्दिर आत्म-साधना की वर्कशाप-कर्मशाला बन जाए। एक्सरे का एक ऐसा स्थान जहा मैं देख सकें कि अपने बाहर के जीवन को जीने मे भीतर से मैं कहा-कहा से टूटा हूँ और क्या करने से फिर से जडंगा और आत्मजयी बनूंगा। मन्दिरो और प्रतिमाओ से भी यदि मैं काम्प्लेसेन्सी-झूठी आत्मतुष्ठी और आत्म-साधना का अहकार खीचता रहँगा तो मेरे बाहर के स्वर्ण भण्डार और मन्दिर के इस मूर्तिभण्डार मे क्या अन्तर रह जाएगा?
माज तो हमारे नॉर्म-प्रतिमान-वो दिशामो के राही हैं। मन्दिर मे प्रात्मनिष्ठा और उसकी देहरी से उतरते ही शरीर-निष्ठा । जैसे कोई लाल और हरी बत्ती के अलग-अलग स्विच लगे हो। देहरी लाघते ही ग्रीन लाइट--दौडो, जितना लेते बने लो। देहरी चढते ही लाल लाइट-रुक जाओ, जितना छोडते बने छोडो। इससे बढकर कोई
और आत्मश्लाघा नही हो सकती। समय आ गया है कि हम अपने नाममन्दिर के प्रतिमान बदल डाले । उस पूजा-अर्चना-आराधना, घट-डियार, शख और महाशख, जय-जयकार और भक्ति से बचे जो हमे केवल धर्माल होने का भ्रम दे रहे हैं। नाम-जपन, पाठ-पूजा और शास्त्र-प्रवचन भी हमे बहुत दूर नहीं ले जा सकेंगे। कुछ कर लिया इतना ही सुख इसमे समाया है। यह तो हुआ मन्दिर का नार्म। और धन-सत्ता-यश की भूख को पूरा करने में हमारी बे-लगाम सासारिक दौड, जैसे भी बने अपने लिए पा लेने की खटपट और इस अधाधुंधी मे सत्य, अहिंसा और करुणा को हर समय दाव पर चढाने को हमारी जुआवृत्ति बाहर का नाम बन गया है। क्या हम अपने मदिरो को इन दोनो नार्म के समन्वय की कर्म-शाला-वर्कशाप नहीं बना सकते ? और यदि नहीं बना सकते तो हमारी लाखो-लाख
१०६
महावीर