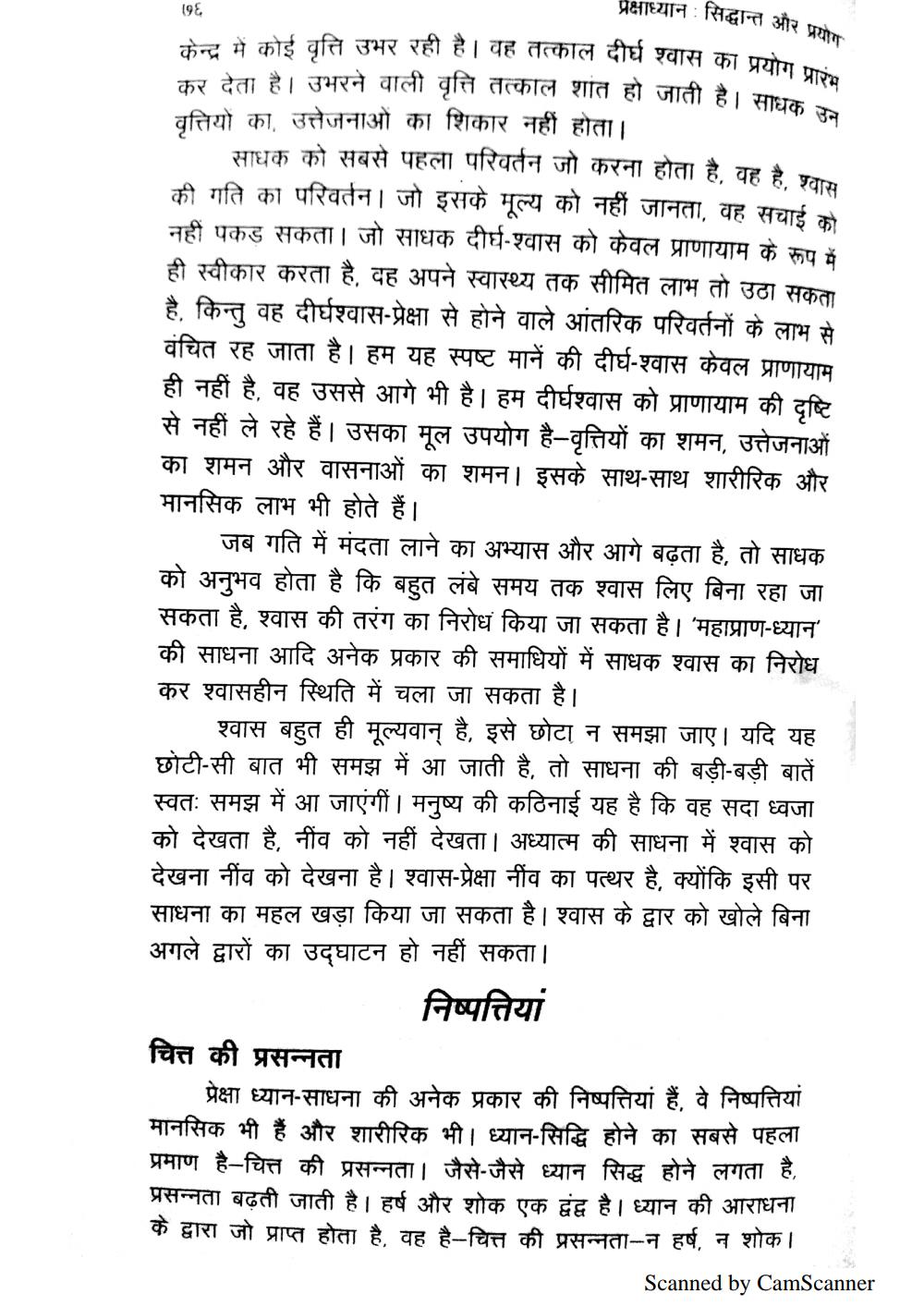________________
प्रेक्षाध्यान सिद्धान्त और प्रयोग
केन्द्र में कोई वृत्ति उभर रही है। वह तत्काल दीर्घ श्वास का प्रयोग प्रारंभ कर देता है । उभरने वाली वृत्ति तत्काल शांत हो जाती है। साधक उन वृत्तियों का उत्तेजनाओं का शिकार नहीं होता ।
साधक को सबसे पहला परिवर्तन जो करना होता है, वह है, श्वास की गति का परिवर्तन। जो इसके मूल्य को नहीं जानता, वह सचाई को नहीं पकड़ सकता। जो साधक दीर्घ श्वास को केवल प्राणायाम के रूप में ही स्वीकार करता है, वह अपने स्वास्थ्य तक सीमित लाभ तो उठा सकता है, किन्तु वह दीर्घश्वास- प्रेक्षा से होने वाले आंतरिक परिवर्तनों के लाभ से वंचित रह जाता है । हम यह स्पष्ट मानें की दीर्घ श्वास केवल प्राणायाम ही नहीं है, वह उससे आगे भी है। हम दीर्घश्वास को प्राणायाम की दृष्टि से नहीं ले रहे हैं। उसका मूल उपयोग है - वृत्तियों का शमन, उत्तेजनाओं का शमन और वासनाओं का शमन । इसके साथ-साथ शारीरिक और मानसिक लाभ भी होते हैं ।
७६
जब गति में मंदता लाने का अभ्यास और आगे बढ़ता है, तो साधक को अनुभव होता है कि बहुत लंबे समय तक श्वास लिए बिना रहा जा सकता है, श्वास की तरंग का निरोध किया जा सकता है। 'महाप्राण-ध्यान' की साधना आदि अनेक प्रकार की समाधियों में साधक श्वास का निरोध कर श्वासहीन स्थिति में चला जा सकता है।
श्वास बहुत ही मूल्यवान् है, इसे छोटा न समझा जाए। यदि यह छोटी-सी बात भी समझ में आ जाती है, तो साधना की बड़ी-बड़ी बातें स्वतः समझ में आ जाएंगीं । मनुष्य की कठिनाई यह है कि वह सदा ध्वजा को देखता है, नींव को नहीं देखता । अध्यात्म की साधना में श्वास को देखना नींव को देखना है। श्वास-प्रेक्षा नींव का पत्थर है, क्योंकि इसी पर साधना का महल खड़ा किया जा सकता है। श्वास के द्वार को खोले बिना अगले द्वारों का उद्घाटन हो नहीं सकता ।
निष्पत्तियां
चित्त की प्रसन्नता
प्रेक्षा ध्यान-साधना की अनेक प्रकार की निष्पत्तियां हैं, वे निष्पत्तियां मानसिक भी हैं और शारीरिक भी । ध्यान - सिद्धि होने का सबसे पहला प्रमाण है- चित्त की प्रसन्नता । जैसे-जैसे ध्यान सिद्ध होने लगता है, प्रसन्नता बढ़ती जाती है। हर्ष और शोक एक द्वंद्व है। ध्यान की आराधना के द्वारा जो प्राप्त होता है, वह है-चित्त की प्रसन्नता-न हर्ष, न शोक ।
Scanned by CamScanner