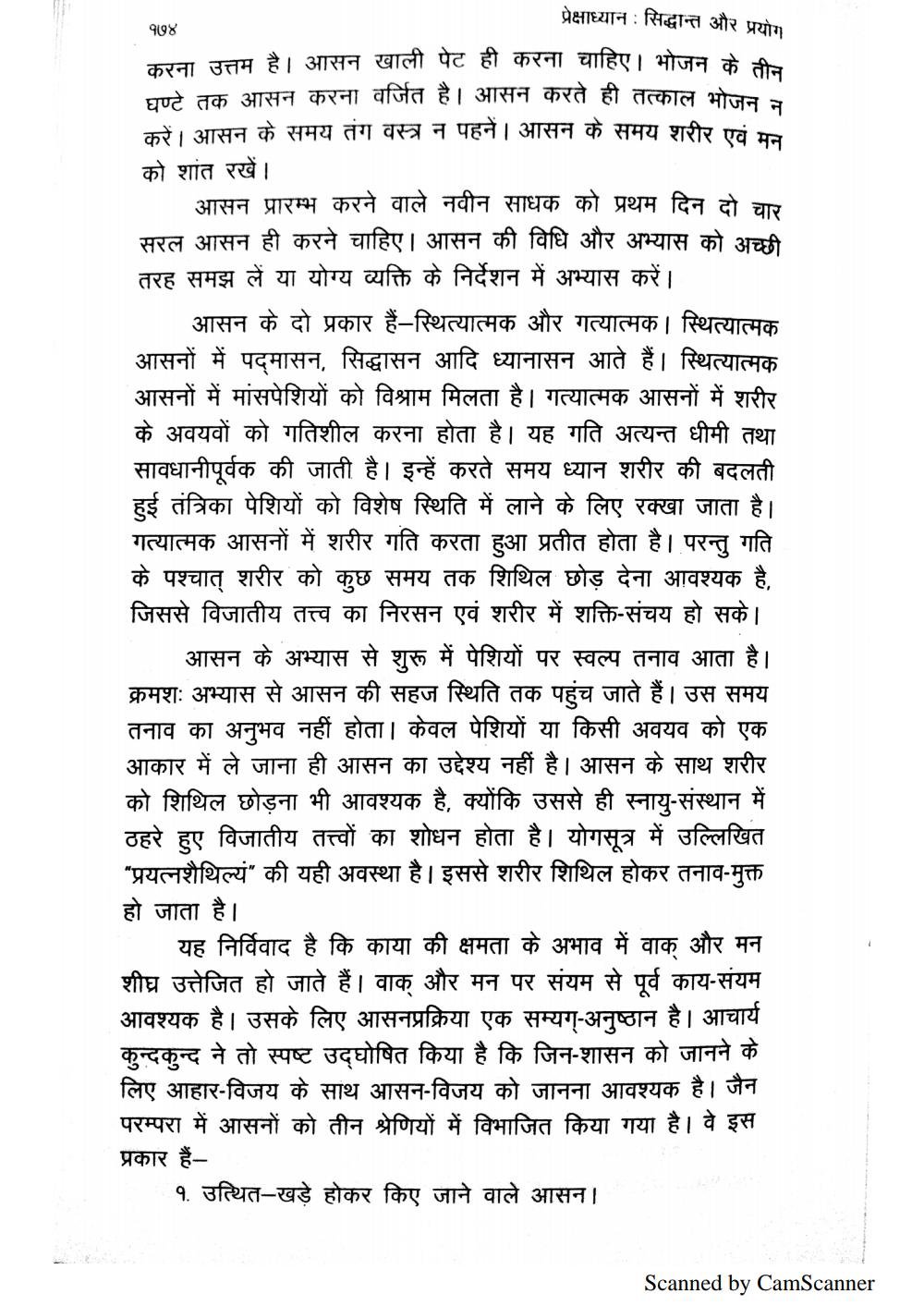________________
प्रेक्षाध्यान : सिद्धान्त और प्रयोग १७४ करना उत्तम है। आसन खाली पेट ही करना चाहिए। भोजन के तीन घण्टे तक आसन करना वर्जित है। आसन करते ही तत्काल भोजन करें। आसन के समय तंग वस्त्र न पहनें। आसन के समय शरीर एवं मन को शांत रखें। ___आसन प्रारम्भ करने वाले नवीन साधक को प्रथम दिन दो चार सरल आसन ही करने चाहिए। आसन की विधि और अभ्यास को अच्छी तरह समझ लें या योग्य व्यक्ति के निर्देशन में अभ्यास करें।
आसन के दो प्रकार हैं-स्थित्यात्मक और गत्यात्मक । स्थित्यात्मक आसनों में पदमासन, सिद्धासन आदि ध्यानासन आते हैं। स्थित्यात्मक आसनों में मांसपेशियों को विश्राम मिलता है। गत्यात्मक आसनों में शरीर के अवयवों को गतिशील करना होता है। यह गति अत्यन्त धीमी तथा सावधानीपूर्वक की जाती है। इन्हें करते समय ध्यान शरीर की बदलती हुई तंत्रिका पेशियों को विशेष स्थिति में लाने के लिए रक्खा जाता है। गत्यात्मक आसनों में शरीर गति करता हुआ प्रतीत होता है। परन्तु गति के पश्चात् शरीर को कुछ समय तक शिथिल छोड़ देना आवश्यक है, जिससे विजातीय तत्त्व का निरसन एवं शरीर में शक्ति-संचय हो सके।
आसन के अभ्यास से शुरू में पेशियों पर स्वल्प तनाव आता है। क्रमशः अभ्यास से आसन की सहज स्थिति तक पहुंच जाते हैं। उस समय तनाव का अनुभव नहीं होता। केवल पेशियों या किसी अवयव को एक आकार में ले जाना ही आसन का उद्देश्य नहीं है। आसन के साथ शरीर को शिथिल छोड़ना भी आवश्यक है, क्योंकि उससे ही स्नायु-संस्थान में ठहरे हुए विजातीय तत्त्वों का शोधन होता है। योगसूत्र में उल्लिखित "प्रयत्नशैथिल्यं” की यही अवस्था है। इससे शरीर शिथिल होकर तनाव-मुक्त हो जाता है।
यह निर्विवाद है कि काया की क्षमता के अभाव में वाक और मन शीघ्र उत्तेजित हो जाते हैं। वाक् और मन पर संयम से पूर्व काय-संयम आवश्यक है। उसके लिए आसनप्रक्रिया एक सम्यग्-अनुष्ठान है। आचार्य कुन्दकुन्द ने तो स्पष्ट उद्घोषित किया है कि जिन-शासन को जानने के लिए आहार-विजय के साथ आसन-विजय को जानना आवश्यक है। जैन परम्परा में आसनों को तीन श्रेणियों में विभाजित किया गया है। वे इस प्रकार हैं
१. उत्थित-खड़े होकर किए जाने वाले आसन।
Scanned by CamScanner