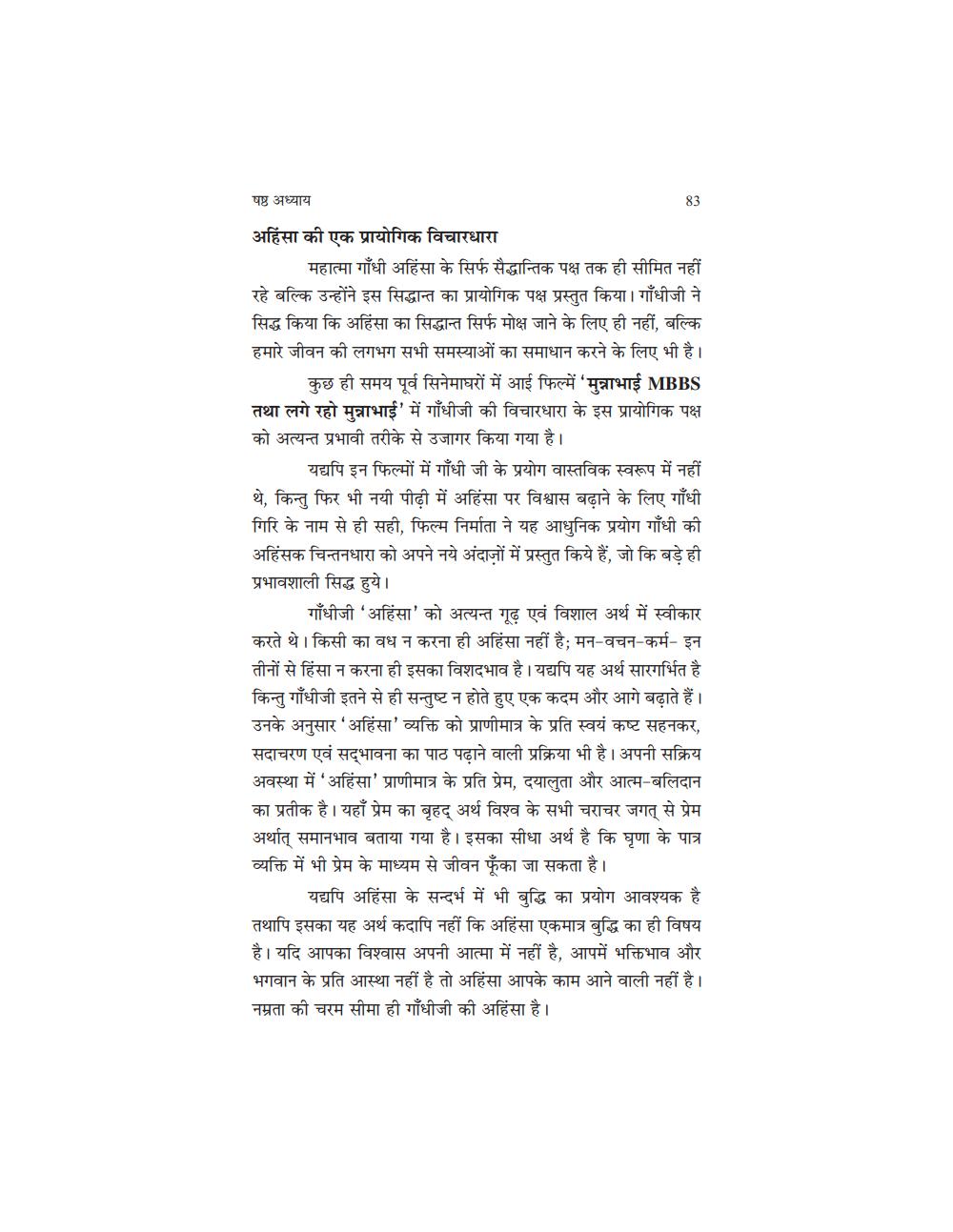________________
षष्ठ अध्याय
अहिंसा की एक प्रायोगिक विचारधारा
महात्मा गाँधी अहिंसा के सिर्फ सैद्धान्तिक पक्ष तक ही सीमित नहीं रहे बल्कि उन्होंने इस सिद्धान्त का प्रायोगिक पक्ष प्रस्तुत किया। गाँधीजी ने सिद्ध किया कि अहिंसा का सिद्धान्त सिर्फ मोक्ष जाने के लिए ही नहीं, बल्कि हमारे जीवन की लगभग सभी समस्याओं का समाधान करने के लिए भी है।
कुछ ही समय पूर्व सिनेमाघरों में आई फिल्में 'मुन्नाभाई MBBS तथा लगे रहो मुन्नाभाई' में गाँधीजी की विचारधारा के इस प्रायोगिक पक्ष को अत्यन्त प्रभावी तरीके से उजागर किया गया है।
यद्यपि इन फिल्मों में गाँधी जी के प्रयोग वास्तविक स्वरूप में नहीं थे, किन्तु फिर भी नयी पीढ़ी में अहिंसा पर विश्वास बढ़ाने के लिए गाँधी गिरि के नाम से ही सही, फिल्म निर्माता ने यह आधुनिक प्रयोग गाँधी की अहिंसक चिन्तनधारा को अपने नये अंदाजों में प्रस्तुत किये हैं, जो कि बड़े ही प्रभावशाली सिद्ध हुये।
गाँधीजी 'अहिंसा' को अत्यन्त गूढ़ एवं विशाल अर्थ में स्वीकार करते थे। किसी का वध न करना ही अहिंसा नहीं है; मन-वचन-कर्म- इन तीनों से हिंसा न करना ही इसका विशदभाव है। यद्यपि यह अर्थ सारगर्भित है किन्तु गाँधीजी इतने से ही सन्तुष्ट न होते हुए एक कदम और आगे बढ़ाते हैं। उनके अनुसार 'अहिंसा' व्यक्ति को प्राणीमात्र के प्रति स्वयं कष्ट सहनकर, सदाचरण एवं सद्भावना का पाठ पढ़ाने वाली प्रक्रिया भी है। अपनी सक्रिय अवस्था में 'अहिंसा' प्राणीमात्र के प्रति प्रेम, दयालुता और आत्म-बलिदान का प्रतीक है। यहाँ प्रेम का बृहद् अर्थ विश्व के सभी चराचर जगत् से प्रेम अर्थात् समानभाव बताया गया है। इसका सीधा अर्थ है कि घृणा के पात्र व्यक्ति में भी प्रेम के माध्यम से जीवन फूंका जा सकता है।
यद्यपि अहिंसा के सन्दर्भ में भी बुद्धि का प्रयोग आवश्यक है तथापि इसका यह अर्थ कदापि नहीं कि अहिंसा एकमात्र बुद्धि का ही विषय है। यदि आपका विश्वास अपनी आत्मा में नहीं है, आपमें भक्तिभाव और भगवान के प्रति आस्था नहीं है तो अहिंसा आपके काम आने वाली नहीं है। नम्रता की चरम सीमा ही गाँधीजी की अहिंसा है।