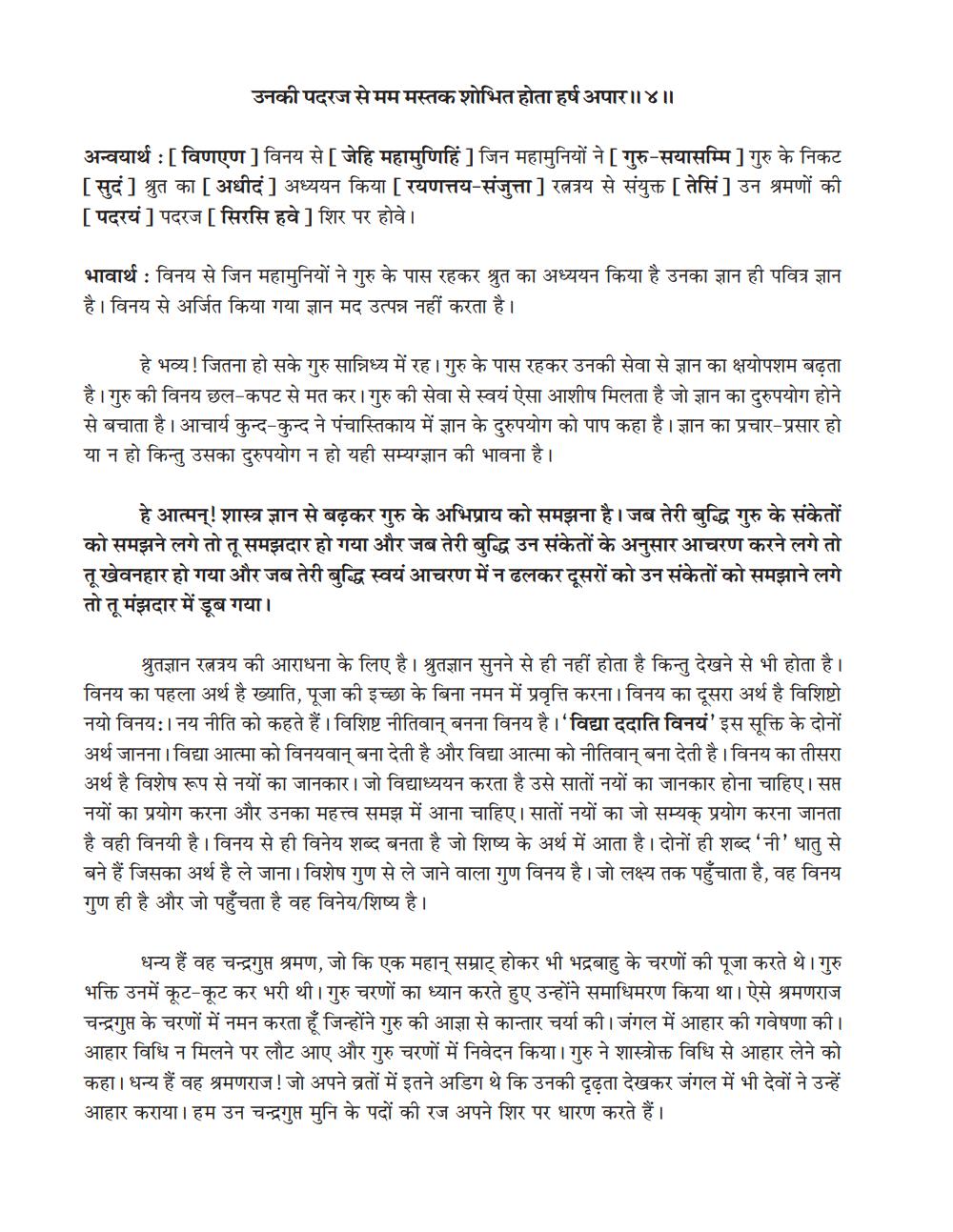________________
उनकी पदरज से मम मस्तक शोभित होता हर्ष अपार॥४॥
अन्वयार्थ : [विणएण] विनय से [ जेहि महामुणिहिं] जिन महामुनियों ने [ गुरु-सयासम्मि] गुरु के निकट [सुदं] श्रुत का [अधीदं] अध्ययन किया [रयणत्तय-संजुत्ता] रत्नत्रय से संयुक्त [तेसिं] उन श्रमणों की [पदरयं] पदरज [सिरसि हवे ] शिर पर होवे।
भावार्थ : विनय से जिन महामुनियों ने गुरु के पास रहकर श्रृत का अध्ययन किया है उनका ज्ञान ही पवित्र ज्ञान है। विनय से अर्जित किया गया ज्ञान मद उत्पन्न नहीं करता है।
हे भव्य ! जितना हो सके गुरु सान्निध्य में रह । गुरु के पास रहकर उनकी सेवा से ज्ञान का क्षयोपशम बढ़ता है। गुरु की विनय छल-कपट से मत कर। गुरु की सेवा से स्वयं ऐसा आशीष मिलता है जो ज्ञान का दुरुपयोग होने से बचाता है। आचार्य कुन्द-कुन्द ने पंचास्तिकाय में ज्ञान के दुरुपयोग को पाप कहा है। ज्ञान का प्रचार-प्रसार हो या न हो किन्तु उसका दुरुपयोग न हो यही सम्यग्ज्ञान की भावना है।
हे आत्मन्! शास्त्र ज्ञान से बढ़कर गुरु के अभिप्राय को समझना है। जब तेरी बुद्धि गुरु के संकेतों को समझने लगे तो तू समझदार हो गया और जब तेरी बुद्धि उन संकेतों के अनुसार आचरण करने लगे तो तू खेवनहार हो गया और जब तेरी बुद्धि स्वयं आचरण में न ढलकर दूसरों को उन संकेतों को समझाने लगे तो तू मंझदार में डूब गया।
श्रुतज्ञान रत्नत्रय की आराधना के लिए है। श्रुतज्ञान सुनने से ही नहीं होता है किन्तु देखने से भी होता है।
का पहला अर्थ है ख्याति. पजा की इच्छा के बिना नमन में प्रवत्ति करना। विनय का दसरा अर्थ है विशिष्टो नयो विनयः। नय नीति को कहते हैं। विशिष्ट नीतिवान् बनना विनय है। 'विद्या ददाति विनयं' इस सूक्ति के दोनों अर्थ जानना। विद्या आत्मा को विनयवान् बना देती है और विद्या आत्मा को नीतिवान् बना देती है। विनय का तीसरा अर्थ है विशेष रूप से नयों का जानकार। जो विद्याध्ययन करता है उसे सातों नयों का जानकार होना चाहिए। सप्त नयों का प्रयोग करना और उनका महत्त्व समझ में आना चाहिए। सातों नयों का जो सम्यक् प्रयोग करना जानता है वही विनयी है। विनय से ही विनेय शब्द बनता है जो शिष्य के अर्थ में आता है। दोनों ही शब्द 'नी' धातु से बने हैं जिसका अर्थ है ले जाना। विशेष गुण से ले जाने वाला गुण विनय है। जो लक्ष्य तक पहुँचाता है, वह विनय गुण ही है और जो पहँचता है वह विनेय/शिष्य है।
धन्य हैं वह चन्द्रगुप्त श्रमण, जो कि एक महान् सम्राट होकर भी भद्रबाहु के चरणों की पूजा करते थे। गुरु भक्ति उनमें कूट-कूट कर भरी थी। गुरु चरणों का ध्यान करते हुए उन्होंने समाधिमरण किया था। ऐसे श्रमणराज चन्द्रगुप्त के चरणों में नमन करता हूँ जिन्होंने गुरु की आज्ञा से कान्तार चर्या की। जंगल में आहार की गवेषणा की। आहार विधि न मिलने पर लौट आए और गुरु चरणों में निवेदन किया। गुरु ने शास्त्रोक्त विधि से आहार लेने को कहा। धन्य हैं वह श्रमणराज! जो अपने व्रतों में इतने अडिग थे कि उनकी दृढ़ता देखकर जंगल में भी देवों ने उन्हें आहार कराया। हम उन चन्द्रगुप्त मुनि के पदों की रज अपने शिर पर धारण करते हैं।