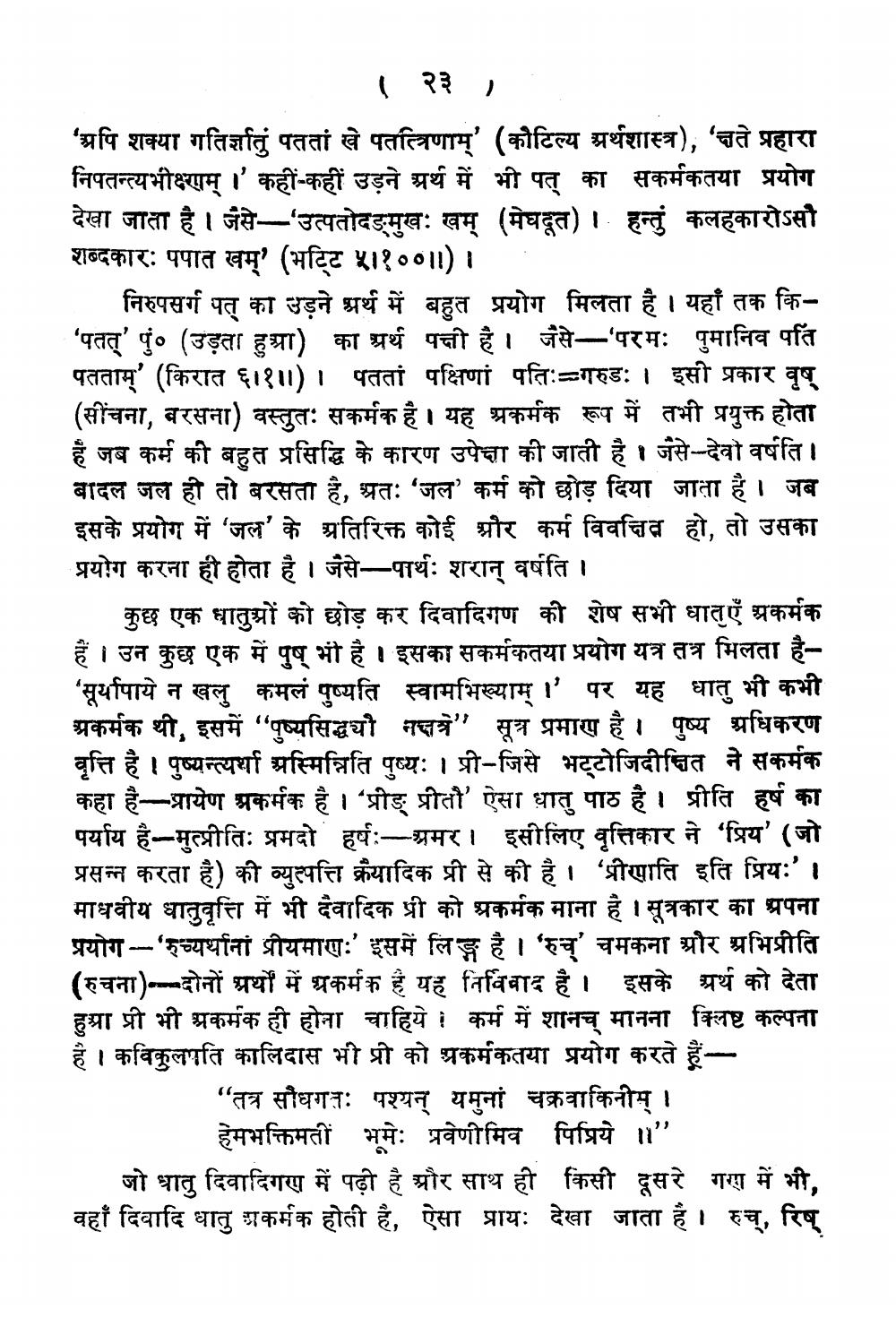________________ / 23 / 'अपि शक्या गतिर्ज्ञातुं पततां खे पतत्त्रिणाम्' (कौटिल्य अर्थशास्त्र), 'क्षते प्रहारा निपतन्त्यभीक्षणम् / ' कहीं-कहीं उड़ने अर्थ में भी पत् का सकर्मकतया प्रयोग देखा जाता है / जैसे-'उत्पतोदङ्मुखः खम् (मेघदूत)। हन्तुं कलहकारोऽसौ शब्दकारः पपात खम्' (भट्टि 52100 // ) / निरुपसर्ग पत् का उड़ने अर्थ में बहुत प्रयोग मिलता है / यहाँ तक कि'पतत्' पुं० (उड़ता हुआ) का अर्थ पत्ती है। जैसे-'परमः पुमानिव पति पतताम्' (किरात 6 / 1 // ) / पततां पक्षिणां पतिः गरुडः / इसी प्रकार वृष् (सींचना, बरसना) वस्तुतः सकर्मक है। यह अकर्मक रूप में तभी प्रयुक्त होता है जब कर्म की बहुत प्रसिद्धि के कारण उपेक्षा की जाती है / जैसे-देवो वर्षति / बादल जल ही तो बरसता है, अतः 'जल' कर्म को छोड़ दिया जाता है। जब इसके प्रयोग में 'जल' के अतिरिक्त कोई और कर्म विवक्षिन हो, तो उसका प्रयोग करना ही होता है / जैसे—पार्थः शरान् वर्षति / / कुछ एक धातुओं को छोड़ कर दिवादिगण की शेष सभी धातुएँ अकर्मक हैं / उन कुछ एक में पुष भी है। इसका सकर्मकतया प्रयोग यत्र तत्र मिलता है'सूर्यापाये न खलु कमलं पुष्यति स्वामभिख्याम् / ' पर यह धातु भी कभी अकर्मक थी, इसमें "पुष्यसिद्धयो नक्षत्रे" सूत्र प्रमाण है। पुष्य अधिकरण वृत्ति है। पुष्यन्त्यर्था अस्मिन्निति पुष्यः / प्री-जिसे भट्टोजिदीक्षित ने सकर्मक कहा है-प्रायेण अकर्मक है। प्री प्रीतौ' ऐसा धातु पाठ है। प्रीति हर्ष का पर्याय है-मुत्प्रीतिः प्रमदो हर्ष:--अमर। इसीलिए वृत्तिकार ने 'प्रिय' (जो प्रसन्न करता है) की व्युत्पत्ति क्रैयादिक प्री से की है। 'प्रीणाति इति प्रियः' / माधवीय धातुवृत्ति में भी देवादिक प्री को अकर्मक माना है / सूत्रकार का अपना प्रयोग-'च्यर्थानां प्रीयमाणः' इसमें लिङ्ग है / 'रुच्' चमकना और अभिप्रीति (रुचना)---दोनों अर्थों में अकर्मक है यह निर्विवाद है। इसके अर्थ को देता हुआ प्री भी अकर्मक ही होना चाहिये। कर्म में शानच् मानना क्लिष्ट कल्पना है / कविकुलपति कालिदास भी प्री को अकर्मकतया प्रयोग करते हैं "तत्र सौधगतः पश्यन् यमुनां चक्रवाकिनीम् / हेमभक्तिमती भूमेः प्रवेणीमिव पिप्रिये // " जो धातु दिवादिगण में पढ़ी है और साथ ही किसी दूसरे गण में भी, वहाँ दिवादि धातु अकर्मक होती है, ऐसा प्रायः देखा जाता है। रुच, रिष्