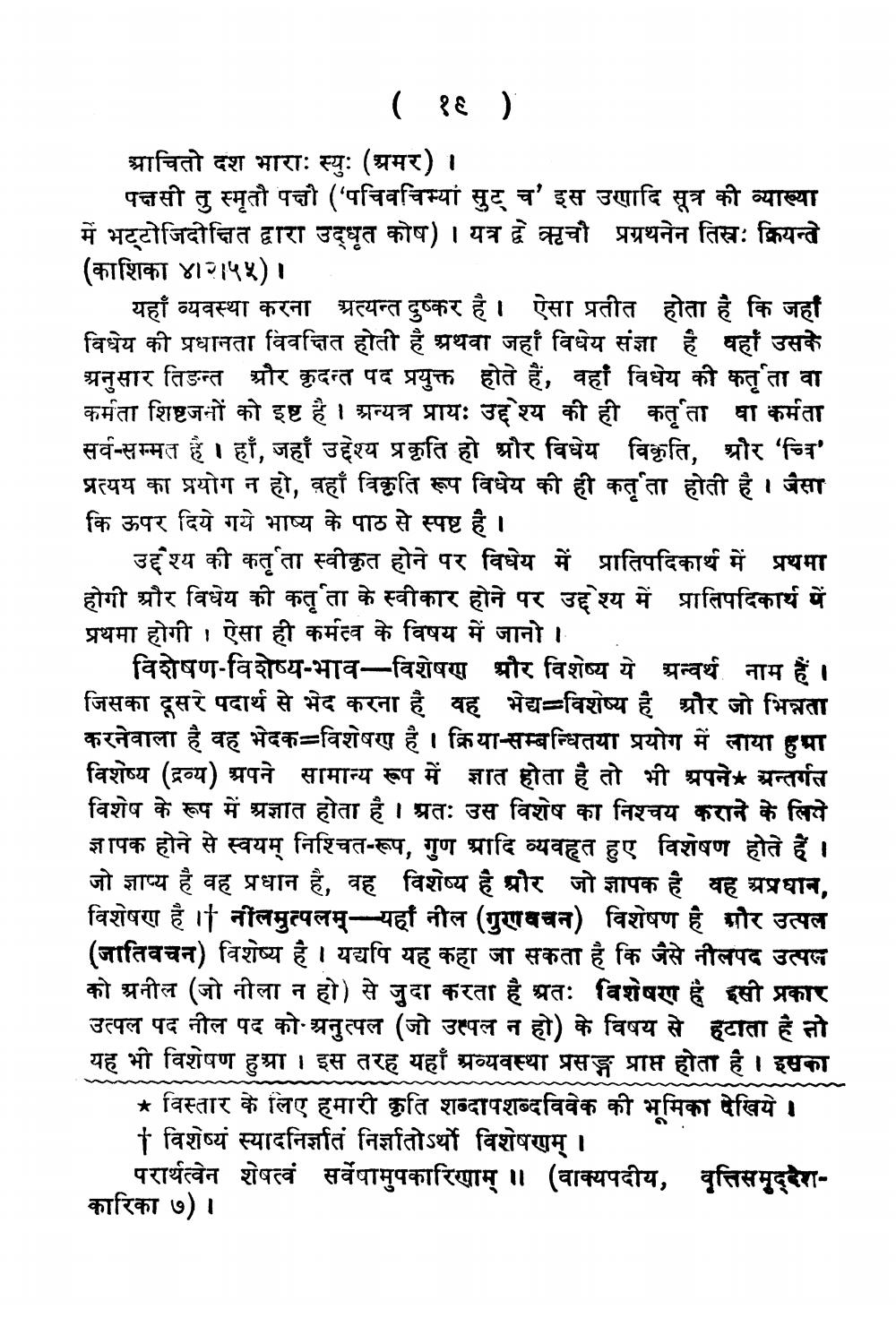________________ ( 16 ) आचितो दश भाराः स्युः (अमर)। पक्षसी तु स्मृतौ पक्षी ('पचिवचिभ्यां सुट च' इस उणादि सूत्र की व्याख्या में भट्टोजिदीक्षित द्वारा उद्धृत कोष) / यत्र द्वे ऋचौ प्रग्रथनेन तिस्रः क्रियन्ते (काशिका 4 / 2 / 55) / __ यहाँ व्यवस्था करना अत्यन्त दुष्कर है। ऐसा प्रतीत होता है कि जहाँ विधेय की प्रधानता विवक्षित होती है अथवा जहाँ विधेय संज्ञा है वहाँ उसके अनुसार तिङन्त और कृदन्त पद प्रयुक्त होते हैं, वहां विधेय की कर्तृता वा कर्मता शिष्टजनों को इष्ट है / अन्यत्र प्रायः उद्देश्य की ही कर्तृता था कर्मता सर्व-सम्मत है। हाँ, जहाँ उद्देश्य प्रकृति हो और विधेय विकृति, और 'चि' प्रत्यय का प्रयोग न हो, वहाँ विकृति रूप विधेय की ही कर्तृता होती है / जैसा कि ऊपर दिये गये भाष्य के पाठ से स्पष्ट है। __ उद्देश्य की कर्तृता स्वीकृत होने पर विधेय में प्रातिपदिकार्थ में प्रथमा होगी और विधेय की कर्तृता के स्वीकार होने पर उद्देश्य में प्रातिपदिकार्य में प्रथमा होगी। ऐसा ही कर्मत्व के विषय में जानो। विशेषण-विशेष्य-भाव-विशेषण और विशेष्य ये अन्वर्थ नाम हैं। जिसका दूसरे पदार्थ से भेद करना है वह भेद्य-विशेष्य है और जो भिन्नता करनेवाला है वह भेदक विशेषण है / क्रिया-सम्बन्धितया प्रयोग में लाया हमा विशेष्य (द्रव्य) अपने सामान्य रूप में ज्ञात होता है तो भी अपने अन्तर्गत विशेष के रूप में अज्ञात होता है / अतः उस विशेष का निश्चय कराने के लिये ज्ञापक होने से स्वयम् निश्चित-रूप, गुण प्रादि व्यवहृत हुए विशेषण होते हैं / जो ज्ञाप्य है वह प्रधान है, वह विशेष्य है और जो ज्ञापक है वह अप्रधान, विशेषण है। नीलमुत्पलम्-यहां नील (गुरगवचन) विशेषण है और उत्पल (जातिवचन) विशेष्य है / यद्यपि यह कहा जा सकता है कि जैसे नीलपद उत्पल को अनील (जो नीला न हो) से जुदा करता है अतः विशेषण है इसी प्रकार उत्पल पद नील पद को अनुत्पल (जो उत्पल न हो) के विषय से हटाता है तो यह भी विशेषण हुआ। इस तरह यहाँ अव्यवस्था प्रसङ्ग प्राप्त होता है / इसका * विस्तार के लिए हमारी कृति शब्दापशब्दविवेक की भूमिका देखिये। + विशेष्यं स्यादनितिं निख़तोऽर्थो विशेषणम् / परार्थत्वेन शेषत्वं सर्वेषामुपकारिणाम् // (वाक्यपदीय, वृत्तिसमृद्देशकारिका 7) /