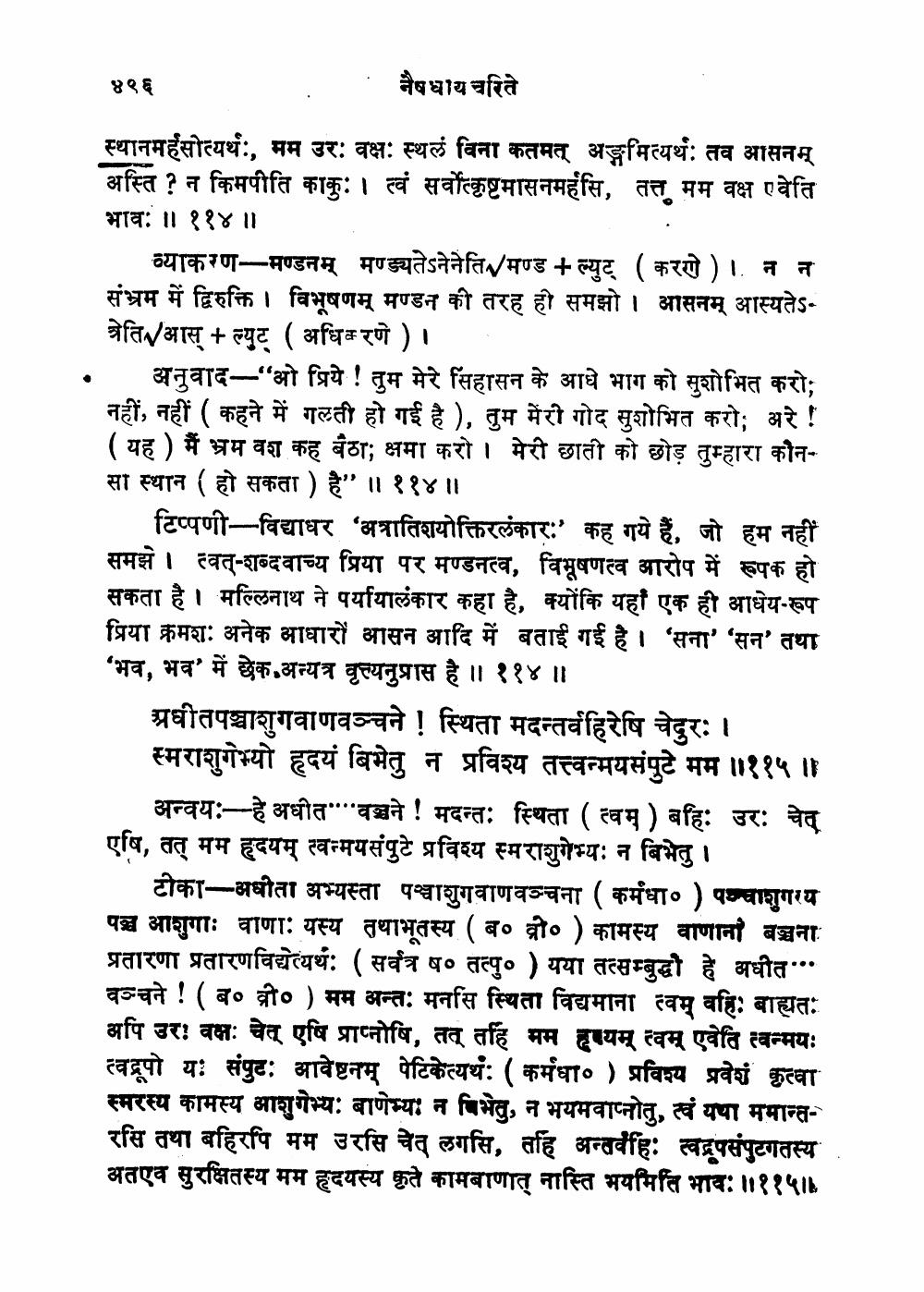________________ 496 नैषधायचरिते स्थानमर्हसोत्यर्थः, मम उरः वक्षः स्थलं विना कतमत् अङ्गमित्यर्थः तव आसनम् अस्ति ? न किमपीति काकुः / त्वं सर्वोत्कृष्टमासनमर्हसि, तत्तु मम वक्ष एवेति भावः // 114 // व्याकरण-मण्डनम् मण्ड्यतेऽनेनेति /मण्ड + ल्युट ( करणे ) / न न संभ्रम में द्विरुक्ति / विभूषणम् मण्डन की तरह ही समझो। आसनम् आस्यतेऽ. त्रेति /आस् + ल्युट् ( अधिक रणे ) / * अनुवाद-"ओ प्रिये ! तुम मेरे सिंहासन के आधे भाग को सुशोभित करो; नहीं, नहीं ( कहने में गलती हो गई है ), तुम मेरी गोद सुशोभित करो; अरे ! ( यह ) मैं भ्रम वश कह बैठा; क्षमा करो। मेरी छाती को छोड़ तुम्हारा कौनसा स्थान (हो सकता) है" // 114 // टिप्पणी-विद्याधर 'अत्रातिशयोक्तिरलंकारः' कह गये हैं, जो हम नहीं समझे। त्वत्-शब्दवाच्य प्रिया पर मण्डनत्व, विभूषणत्व आरोप में रूपक हो सकता है। मल्लिनाथ ने पर्यायालंकार कहा है, क्योंकि यहां एक ही आधेय-रूप प्रिया क्रमशः अनेक आधारों आसन आदि में बताई गई है। 'सना' 'सन' तथा 'भव, भव' में छेक अन्यत्र वृत्त्यनुप्रास है / / 114 // अधीतपञ्चाशुगवाणवञ्चने ! स्थिता मदन्तर्वहिरेषि चेदुरः / स्मराशुगेभ्यो हृदयं बिभेतु न प्रविश्य तत्त्वन्मयसंपुटे मम // 115 / / अन्वयः-हे अधीत""वञ्चने ! मदन्तः स्थिता ( त्वम् ) बहिः उरः चेत् एषि, तत् मम हृदयम् त्वन्मयसंपुटे प्रविश्य स्मराशुगेभ्यः न बिभेतु / टीका-अधीता अभ्यस्ता पञ्चाशुगवाणवञ्चना ( कर्मधा० ) पञ्चाशुगरय पञ्च आशुगाः वाणाः यस्य तथाभूतस्य (ब० वी०) कामस्य वाणाना बञ्चना प्रतारणा प्रतारणविद्यत्यर्थः ( सर्वत्र ष० तत्पु० ) यया तत्सम्बुद्धी हे अधीत वञ्चने ! ( ब० वी० ) मम अन्त: मनसि स्थिता विद्यमाना त्वम् वहिः बाह्यतः अपि उरवक्षः चेत् एषि प्राप्नोषि, तत् तर्हि मम हुण्यम् त्वम् एवेति त्वन्मयः त्वद्र्पो यः संपुट: आवेष्टनम् पेटिकेत्यर्थः (कर्मधा० ) प्रविश्य प्रवेशं कृत्वा स्मरस्य कामस्य आशुगेभ्यः बाणेभ्यः न विभेतु, न भयमवाप्नोतु, त्वं यथा ममान्तरसि तथा बहिरपि मम उरसि चेत् लगसि, तर्हि अन्तर्वहिः त्वद्रूपसंपुटगतस्य अतएव सुरक्षितस्य मम हृदयस्य कृते कामबाणात् नास्ति भयमिति भावः // 115 //