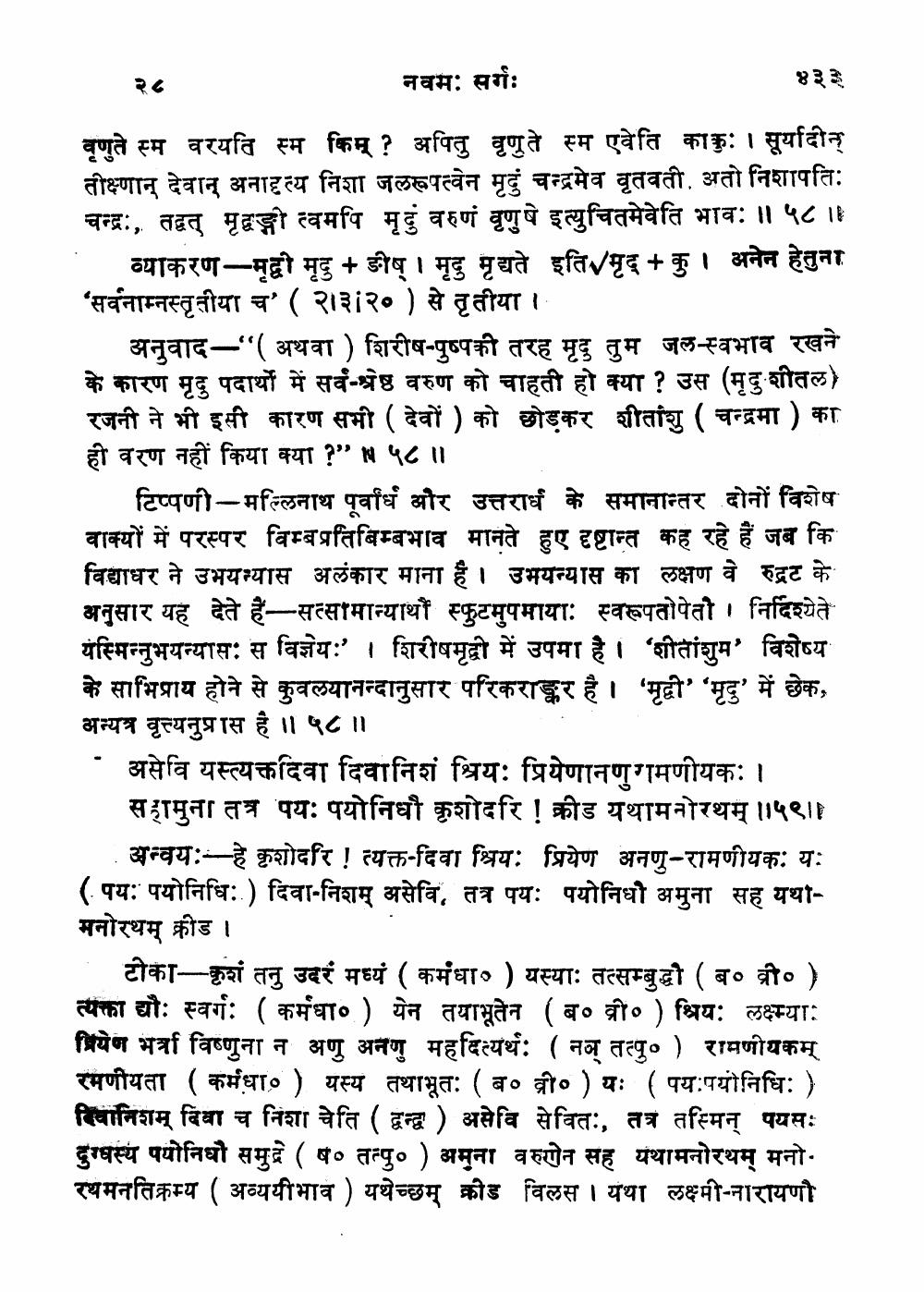________________ नवमः सर्गः 433 वृणुते स्म वरयति स्म किम् ? अपितु वृणुते स्म एवेति काकुः / सूर्यादीन् तीक्ष्णान् देवान् अनादृत्य निशा जलरूपत्वेन मृदुं चन्द्रमेव वृतवती. अतो निशापतिः चन्द्रः, तद्वत् मृदङ्गी त्वमपि मृदुं वरुणं वृणुषे इत्युचितमेवेति भावः // 58 / / व्याकरण-मृद्वी मृदु + ङीष् / मृदु मृद्यते इति/मृद् + कु / अनेन हेतुना 'सर्वनाम्नस्तृतीया च' ( 2 / 320 ) से तृतीया / __ अनुवाद-"( अथवा ) शिरीष-पुष्पकी तरह मृदु तुम जल-स्वभाव रखने के कारण मृदु पदार्थों में सर्वश्रेष्ठ वरुण को चाहती हो क्या? उस (मृदुःशीतल) रजनी ने भी इसी कारण सभी ( देवों ) को छोड़कर शीतांशु ( चन्द्रमा ) का ही वरण नहीं किया क्या ?" 58 // टिप्पणी-मल्लिनाथ पूर्वांध और उत्तरार्ध के समानान्तर दोनों विशेष वाक्यों में परस्पर विम्बप्रतिबिम्बभाव मानते हुए दृष्टान्त कह रहे हैं जब कि विद्याधर ने उभयभ्यास अलंकार माना है। उभयन्यास का लक्षण वे रुद्रट के अनुसार यह देते हैं-सत्सामान्याथों स्फुटमुपमायाः स्वरूपतोपेती / निर्दिश्येते यस्मिन्नुभयन्यास: स विज्ञेयः' / शिरीषमुद्री में उपमा है। 'शीतांशम' विशेष्य के साभिप्राय होने से कुवलयानन्दानुसार परिकरार है। 'मृद्वी' 'मृदु' में छेक, अन्यत्र वृत्त्यनुप्रास है / / 58 // * असेवि यस्त्यक्तदिवा दिवानिशं श्रियः प्रियेणानणुगमणीयकः / सहामुना तत्र पयः पयोनिधी कृशोदरि ! क्रीड यथामनोरथम् / / 59 / / अन्वयः हे कृशोदरि ! त्यक्त-दिवा श्रियः प्रियेण अनणु-रामणीयकः यः (पयः पयोनिधि:) दिवा-निशम् असेवि, तत्र पयः पयोनिधी अमुना सह यथामनोरथम् क्रीड। टोका-कृशं तनु उदरं मध्यं ( कर्मधा० ) यस्याः तत्सम्बुद्धी ( ब० वी० ) त्यता द्यौः स्वर्गः ( कर्मधा० ) येन तयाभूतेन (ब० वी० ) श्रिय: लक्ष्म्याः प्रियेण भ; विष्णुना न अणु अनणु महदित्यर्थः ( नन तत्पु० ) रामणीयकम् रमणीयता ( कर्मधा० ) यस्य तथाभूतः ( ब० वी० ) यः ( पयःपयोनिधिः ) दिवानिशम् विवा च निशा चेति ( द्वन्द्वा) असेवि सेवितः, तत्र तस्मिन् पयसः दुग्धस्य पयोनिधौ समुद्रे (10 तत्पु० ) अमुना वरुणेन सह यथामनोरथम् मनो. रथमनतिक्रम्य ( अव्ययीभाव ) यथेच्छम् क्रोड विलस / यथा लक्ष्मी-नारायणी