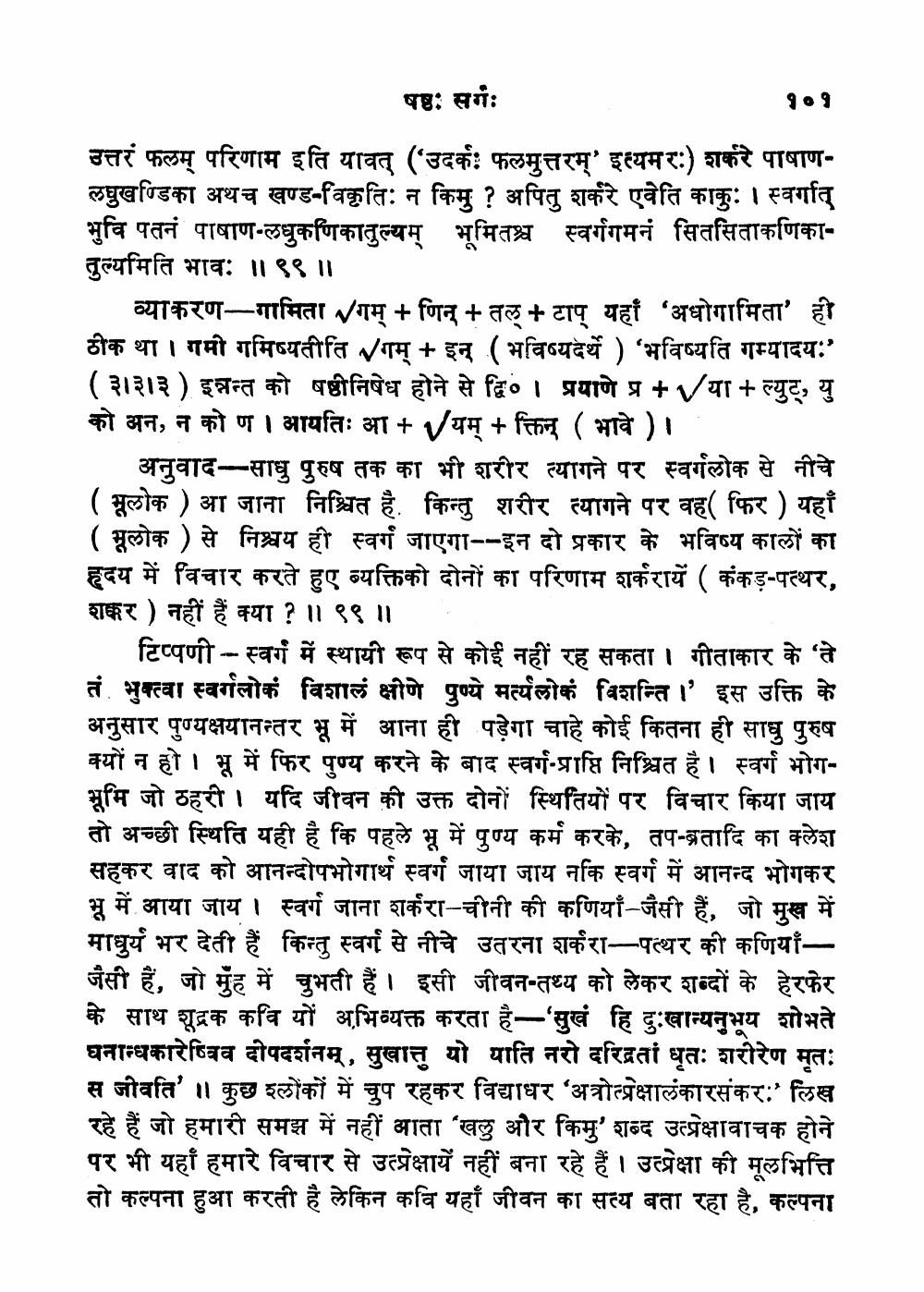________________ षष्ठः सर्गः उत्तरं फलम् परिणाम इति यावत् ('उदर्कः फलमुत्तरम्' इत्यमरः) शर्करे पाषाणलघुखण्डिका अथच खण्ड-विकृतिः न किमु ? अपितु शर्करे एवेति काकुः / स्वर्गात भुवि पतनं पाषाण-लधुकणिकातुल्यम् भूमितश्च स्वर्गगमनं सितसिताकणिकातुल्यमिति भावः // 99 // व्याकरण-गामिता गम् + णिन् + तल + टाप् यहाँ 'अधोगामिता' ही ठीक था। गमी गमिष्यतीति गम् + इन् (भविष्यदर्थे ) 'भविष्यति गम्यादयः' ( 3 / 3 / 3) इन्नन्त को षष्ठीनिषेध होने से द्वि० / प्रयाणे प्र + Vया + ल्युट्, यु को अन, न को ण / आयतिः आ + /यम् + क्तिन् ( भावे ) / ___ अनुवाद-साधु पुरुष तक का भी शरीर त्यागने पर स्वर्गलोक से नीचे ( भूलोक ) आ जाना निश्चित है. किन्तु शरीर त्यागने पर वह( फिर ) यहाँ ( भूलोक ) से निश्चय ही स्वर्ग जाएगा--इन दो प्रकार के भविष्य कालों का हृदय में विचार करते हुए व्यक्तिको दोनों का परिणाम शर्कराय ( कंकड़-पत्थर, शकर ) नहीं हैं क्या ? // 99 // टिप्पणी- स्वर्ग में स्थायी रूप से कोई नहीं रह सकता। गीताकार के 'ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति / ' इस उक्ति के अनुसार पुण्यक्षयानन्तर भू में आना ही पड़ेगा चाहे कोई कितना ही साधु पुरुष क्यों न हो। भू में फिर पुण्य करने के बाद स्वर्ग-प्राप्ति निश्चित है। स्वर्ग भोगभूमि जो ठहरी / यदि जीवन की उक्त दोनों स्थितियों पर विचार किया जाय तो अच्छी स्थिति यही है कि पहले भू में पुण्य कर्म करके, तप-ब्रतादि का क्लेश सहकर वाद को आनन्दोपभोगार्थ स्वर्ग जाया जाय नकि स्वर्ग में आनन्द भोगकर भू में आया जाय / स्वर्ग जाना शर्करा-चीनी की कणियाँ-जैसी हैं, जो मुख में माधुर्य भर देती हैं किन्तु स्वर्ग से नीचे उतरना शर्करा-पत्थर की कणियाँजैसी हैं, जो मुंह में चुभती हैं। इसी जीवन-तथ्य को लेकर शब्दों के हेरफेर के साथ शूद्रक कवि यों अभिव्यक्त करता है-'सुखं हि दुःखान्यनुभूय शोभते घनान्धकारेष्विव दोपदर्शनम् , सुखात्तु यो याति नरो दरिद्रतां धृतः शरीरेण मृतः स जीवति' // कुछ श्लोकों में चुप रहकर विद्याधर 'अत्रोत्प्रेक्षालंकारसंकरः' लिख रहे हैं जो हमारी समझ में नहीं आता 'खलु और किमु' शब्द उत्प्रेक्षावाचक होने पर भी यहाँ हमारे विचार से उत्प्रेक्षायें नहीं बना रहे हैं। उत्प्रेक्षा की मूलभित्ति तो कल्पना हुआ करती है लेकिन कवि यहाँ जीवन का सत्य बता रहा है, कल्पना