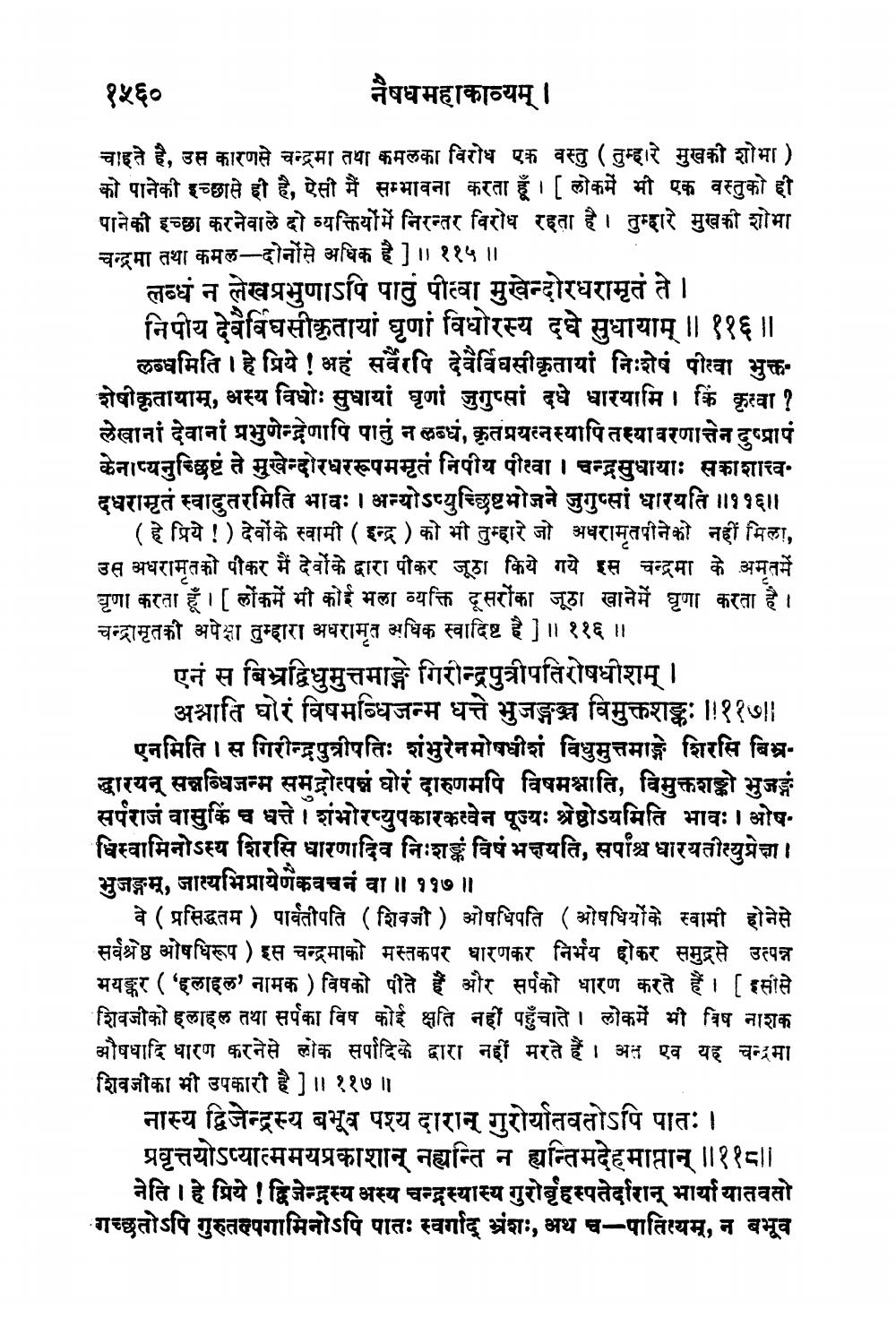________________ 1560 नैषधमहाकाव्यम् / चाहते है, उस कारणसे चन्द्रमा तथा कमलका विरोध एक वस्तु ( तुम्हारे मुखको शोमा) को पानेकी इच्छासे ही है, ऐसी मैं सम्भावना करता हूँ। [ लोकमें भी एक वस्तुको ही पाने की इच्छा करनेवाले दो व्यक्तियों में निरन्तर विरोध रहता है। तुम्हारे मुखकी शोमा चन्द्रमा तथा कमल-दोनोंसे अधिक है ] // 115 // लब्धं न लेखप्रभुणाऽपि पातुं पीत्वा मुखेन्दोरधरामृतं ते / निपीय देवविधसीकृतायां घृणां विधोरस्य दधे सुधायाम् || 116 / / लब्धमिति / हे प्रिये ! अहं सर्वैरपि देवैर्विघसीकृतायां निःशेषं पीत्वा भुक्त शेषीकृतायाम्, अस्य विधोः सुधायां घृणां जुगुप्सां दधे धारयामि / किं कृत्वा ? लेखानां देवानां प्रभुणेन्द्रेणापि पातुं न लब्धं, कृतप्रयत्नस्यापितस्यावरणात्तेन दुष्प्रापं केनाप्यनुच्छिष्टं ते मुखेन्दोरधररूपममृतं निपीय पीत्वा / चन्द्रसुधायाः सकाशाव. दधरामृतं स्वादुतरमिति भावः / अन्योऽप्युच्छिष्टमोजने जुगुप्सां धारयति // 11 // (हे प्रिये ! ) देवोंके स्वामी ( इन्द्र) को भी तुम्हारे जो अधरामृतपीने को नहीं मिला, उस अधरामतको पीकर मैं देवों के द्वारा पीकर जूठा किये गये इस चन्द्रमा के अमृतमें घृणा करता हूँ। [ लोकमें भी कोई मला व्यक्ति दूसरोंका जूठा खानेमें घृणा करता है। चन्द्रामृतकी अपेक्षा तुम्हारा अधरामृत अधिक स्वादिष्ट है ] // 116 / / एनं स बिभ्रद्विधुमुत्तमाङ्गे गिरीन्द्रपुत्रीपतिरोषधीशम् / अनाति घोरं विषमब्धिजन्म धत्ते भुजङ्गन विमुक्तशङ्कः / / 117|| एनमिति / स गिरीन्द्रपुत्रीपतिः शंभुरेनमोषधीशं विधुमुत्तमाङ्गे शिरसि बिभ्रद्धारयन् सन्नधिजन्म समद्रोत्पन्नं घोरं दारुणमपि विषमश्नाति, विमुक्तशङ्को भुजङ्गं सर्पराज वासुकिं च धत्ते / शंभोरप्युपकारकत्वेन पूज्यः श्रेष्ठोऽयमिति भावः / ओष. विस्वामिनोऽस्य शिरसि धारणादिव निःशकं विषं भक्षयति, सपश्चि धारयतीत्युप्रेक्षा। भुजङ्गम, जात्यभिप्रायेणेकवचनं वा // 117 // वे ( प्रसिद्धतम ) पार्वतीपति (शिवजी ) ओषधिपति (ओषधियों के स्वामी होनेसे सर्वश्रेष्ठ ओषधिरूप ) इस चन्द्रमाको मस्तकपर धारणकर निर्भय होकर समुद्रसे उत्पन्न भयङ्कर ( 'इलाहल' नामक ) विषको पीते हैं और सर्पको धारण करते हैं। [इसीसे शिवजीको हलाहल तथा सर्पका विष कोई क्षति नहीं पहुँचाते / लोकमें भी विष नाशक औषधादि धारण करनेसे लोक सादिके द्वारा नहीं मरते हैं। अत एव यह चन्द्रमा शिवजीका भी उपकारी है ] // 117 // नास्य द्विजेन्द्रस्य बभूव पश्य दारान गुरोर्यातवतोऽपि पातः / प्रवृत्तयोऽप्यात्ममयप्रकाशान् नह्यन्ति न ह्यन्तिमदेहमाप्तान् / / 118 / / नेति / हे प्रिये ! द्विजेन्द्रस्य अस्य चन्द्रस्यास्य गुरोबृहस्पतेर्दारान् भार्या यातवतो गच्छतोऽपि गुरुतल्पगामिनोऽपि पातः स्वर्गाद् भ्रंशः, अथ च-पातित्यम्, न बभूव