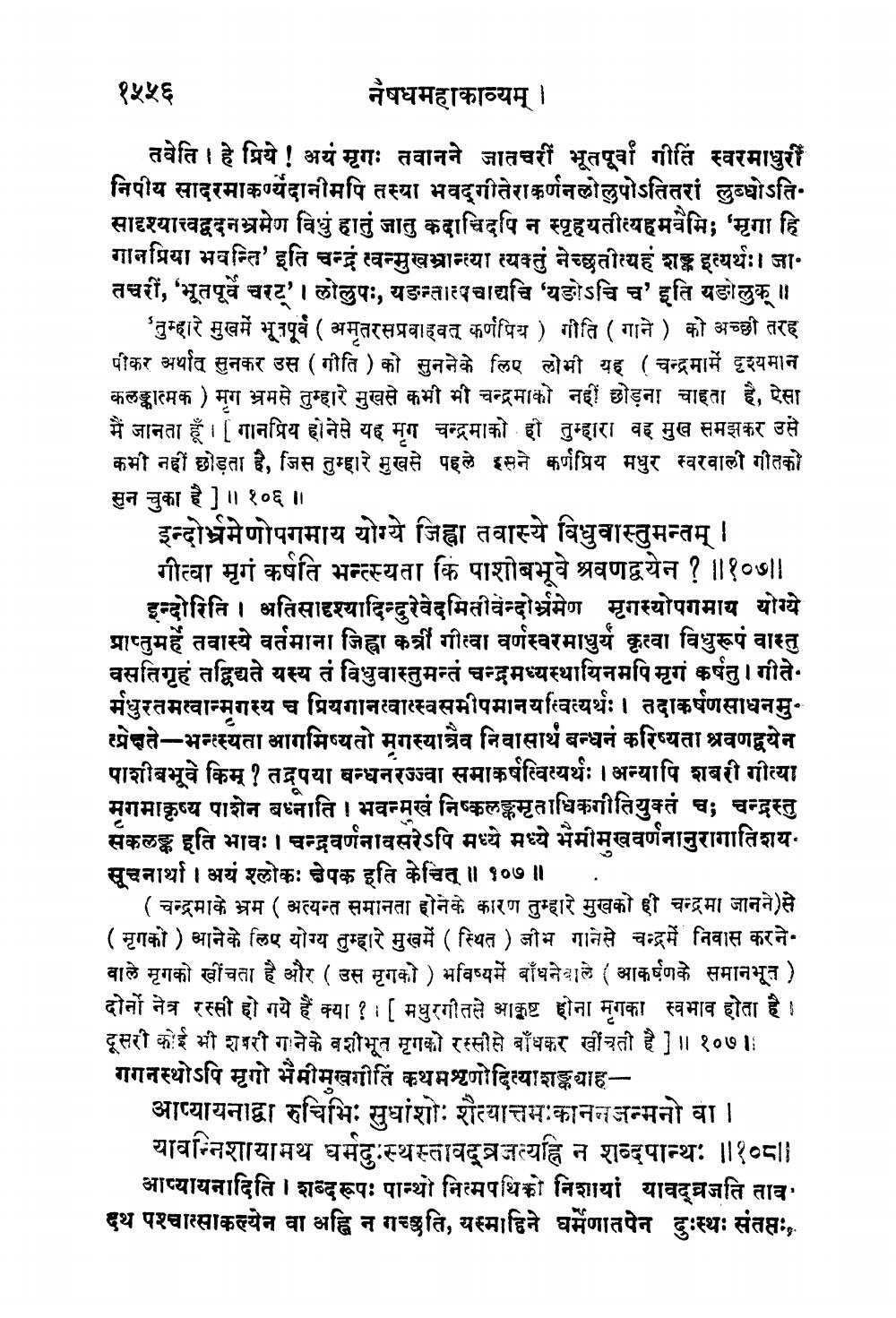________________ 1556 नैषधमहाकाव्यम्। तवेति / हे प्रिये ! अयं मृगः तवानने जातचरी भूतपूर्वां गीति स्वरमाधुरी निपीय सादरमाकण्यदानीमपि तस्या भवद्गीतेराकर्णनलोलुपोऽतितरां लुब्धोऽति. सादृश्यात्वद्वदनभ्रमेण विधुं हातुं जातु कदाचिदपि न स्पृहयतीत्यहमवैमि; 'मृगा हि गानप्रिया भवन्ति' इति चन्द्रं स्वन्मुखभ्रान्त्या त्यक्तुं नेच्छतीत्यहं शङ्क इत्यर्थः। जा. तचरी, भूतपूर्वे चरट्' / लोलुपः, यङन्तापचाद्यचि 'यङोऽचि च' इति यङोलुक् // 'तुम्हारे मुखमें भूतपूर्व ( अमतरसप्रवाहवत् कर्णप्रिय ) गीति ( गाने ) को अच्छी तरह पीकर अर्थात् सुनकर उस (गीति ) को सुनने के लिए लोभी यह ( चन्द्रमामें दृश्यमान कलङ्कात्मक ) मृग भ्रमसे तुम्हारे मुखसे कभी भी चन्द्रमाको नहीं छोड़ना चाहता है, ऐसा मैं जानता हूँ। [ गानप्रिय होने से यह मृग चन्द्रमाको ही तुम्हारा वह मुख समझकर उसे कमी नहीं छोड़ता है, जिस तुम्हारे मुखसे पहले इसने कर्णप्रिय मधुर स्वरवाली गीतको सुन चुका है ] / / 106 // इन्दोर्धमेणोपगमाय योग्ये जिह्वा तवास्ये विधुवास्तुमन्तम् / गीत्वा मृगं कर्षति भन्त्स्य ता कि पाशोबभूवे श्रवणद्वयेन ? ||107|| इन्दोरिति / अतिसादृश्यादिन्दुरेवेदमितीवेन्दोभ्रंमेण मृगस्योपगमाय योग्ये प्राप्तुम, तवास्ये वर्तमाना जिह्वा की गीत्वा वर्णस्वरमाधुर्यं कृत्वा विधुरूपं वास्तु वसतिगृहं तद्विद्यते यस्य तं विधुवास्तुमन्तं चन्द्रमध्यस्थायिनमपि मृगं कर्षतु / गीते. मधुरतमत्वान्मगस्य च प्रियगानस्वारस्वसमीपमानयस्वित्यर्थः। तदाकर्षणसाधनमु. स्प्रेक्षते–भन्स्यता आगमिष्यतो मृगस्यात्रैव निवासार्थ बन्धनं करिष्यता श्रवणद्वयेन पाशीबभूवे किम् ? तद्रूपया बन्धनरज्ज्वा समाकर्षस्वित्यर्थः / अन्यापि शबरी गीत्या मगमाकृष्य पाशेन बध्नाति / भवन्मुखं निष्कलङ्कमृताधिकगीतियुक्तं च; चन्द्रस्तु सकलङ्क इति भावः / चन्द्रवर्णनावसरेऽपि मध्ये मध्ये भैमीमुखवर्णनानुरागातिशय सूचनार्था / अयं श्लोकः क्षेपक इति केचित् // 107 // . ( चन्द्रमाके भ्रम ( अत्यन्त समानता होने के कारण तुम्हारे मुखको ही चन्द्रमा जानने)से ( मृगको ) आने के लिए योग्य तुम्हारे मुखमें ( स्थित ) जीम गानेसे चन्द्रमें निवास करने. वाले मृगको खींचता है और ( उस मृगको ) भविष्यमें बाँधनेवाले ( आकर्षणके समानभूत ) दोनों नेत्र रस्सी हो गये हैं क्या ? : [ मधुरगीतले आकृष्ट होना मृगका स्वभाव होता है। दूसरी कोई भी शपरी गाने के वशीभूत मृगको रस्सीसे बाँधकर खींचती है ] // 107 / / गगनस्थोऽपि मृगो भैमीमखगीति कथमशृणोदित्याशङ्कयाह आप्यायनाद्वा रुचिभिः सुधांशोः शैत्यात्तमःकाननजन्मनो वा / यावन्निशायामथ धर्मदुःस्थस्तावबजत्यह्नि न शब्दपान्थः ||108|| आप्यायनादिति / शब्दरूपः पान्थो नित्मपथिको निशायां यावद्बजति ताव दथ पश्चारसाकल्येन वा अहि न गच्छति, यस्माहिने धर्मेणातपेन दुःस्थः संतप्तः,