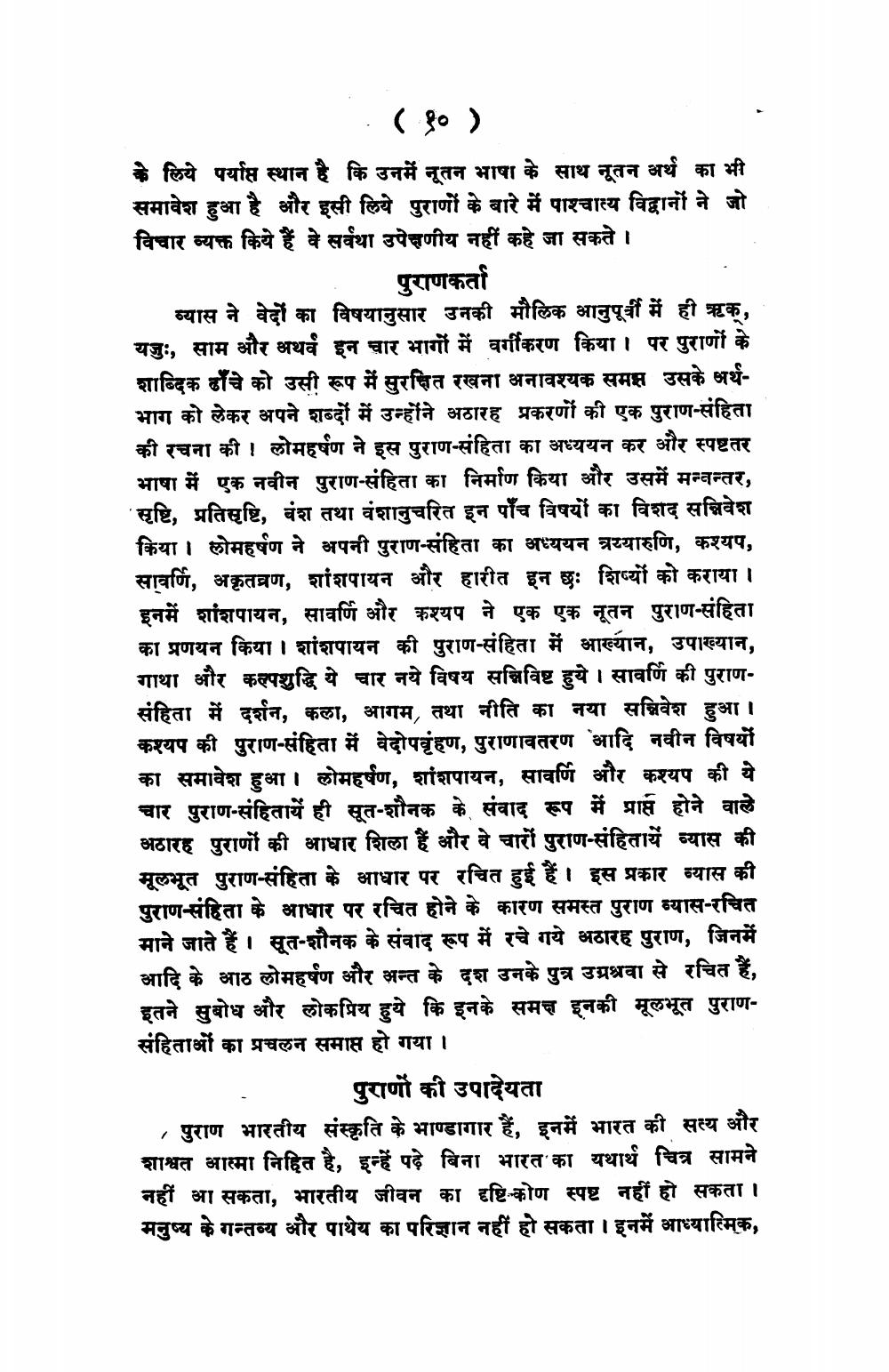________________ के लिये पर्याप्त स्थान है कि उनमें नूतन भाषा के साथ नूतन अर्थ का भी समावेश हुआ है और इसी लिये पुराणों के बारे में पाश्चात्य विद्वानों ने जो विचार व्यक्त किये हैं के सर्वथा उपेक्षणीय नहीं कहे जा सकते / पुराणकर्ता व्यास ने वेदों का विषयानुसार उनकी मौलिक आनुपूर्वी में ही ऋक, यजुः, साम और अथर्व इन चार भागों में वर्गीकरण किया। पर पुराणों के शाब्दिक ढाँचे को उसी रूप में सुरक्षित रखना अनावश्यक समझ उसके अर्थभाग को लेकर अपने शब्दों में उन्होंने अठारह प्रकरणों की एक पुराण-संहिता की रचना की। लोमहर्षण ने इस पुराण-संहिता का अध्ययन कर और स्पष्टतर भाषा में एक नवीन पुराण-संहिता का निर्माण किया और उसमें मन्वन्तर, सृष्टि, प्रतिसृष्टि, वंश तथा वंशानुचरित इन पाँच विषयों का विशद सन्निवेश किया। लोमहर्षण ने अपनी पुराण-संहिता का अध्ययन त्रय्यारुणि, कश्यप, सावर्णि, अकृतव्रण, शांशपायन और हारीत इन छः शिष्यों को कराया। इनमें शांशपायन, सावर्णि और कश्यप ने एक एक नूतन पुराण-संहिता का प्रणयन किया। शांशपायन की पुराण-संहिता में आख्यान, उपाख्यान, गाथा और कल्पशुद्धि ये चार नये विषय सन्निविष्ट हुये / सावर्णि की पुराणसंहिता में दर्शन, कला, आगम, तथा नीति का नया सन्निवेश हुआ। कश्यप की पुराण-संहिता में वेदोपवृंहण, पुराणावतरण आदि नवीन विषयों का समावेश हुआ। लोमहर्षण, शांशपायन, सावर्णि और कश्यप की ये चार पुराण-संहितायें ही सूत-शौनक के संवाद रूप में प्राप्त होने वाले अठारह पुराणों की आधार शिला हैं और वे चारों पुराण-संहितायें व्यास की मूलभूत पुराण-संहिता के आधार पर रचित हुई हैं। इस प्रकार व्यास की पुराण-संहिता के आधार पर रचित होने के कारण समस्त पुराण व्यास-रचित माने जाते हैं। सूत-शौनक के संवाद रूप में रचे गये अठारह पुराण, जिनमें आदि के आठ लोमहर्षण और अन्त के दश उनके पुत्र उग्रश्रवा से रचित हैं, इतने सुबोध और लोकप्रिय हुये कि इनके समक्ष इनकी मूलभूत पुराणसंहिताओं का प्रचलन समाप्त हो गया। . पुराणों की उपादेयता / पुराण भारतीय संस्कृति के भाण्डागार हैं, इनमें भारत की सत्य और शाश्वत आत्मा निहित है, इन्हें पढ़े बिना भारत' का यथार्थ चित्र सामने नहीं आ सकता, भारतीय जीवन का दृष्टिकोण स्पष्ट नहीं हो सकता। मनुष्य के गन्तव्य और पाथेय का परिज्ञान नहीं हो सकता। इनमें आध्यात्मिक,