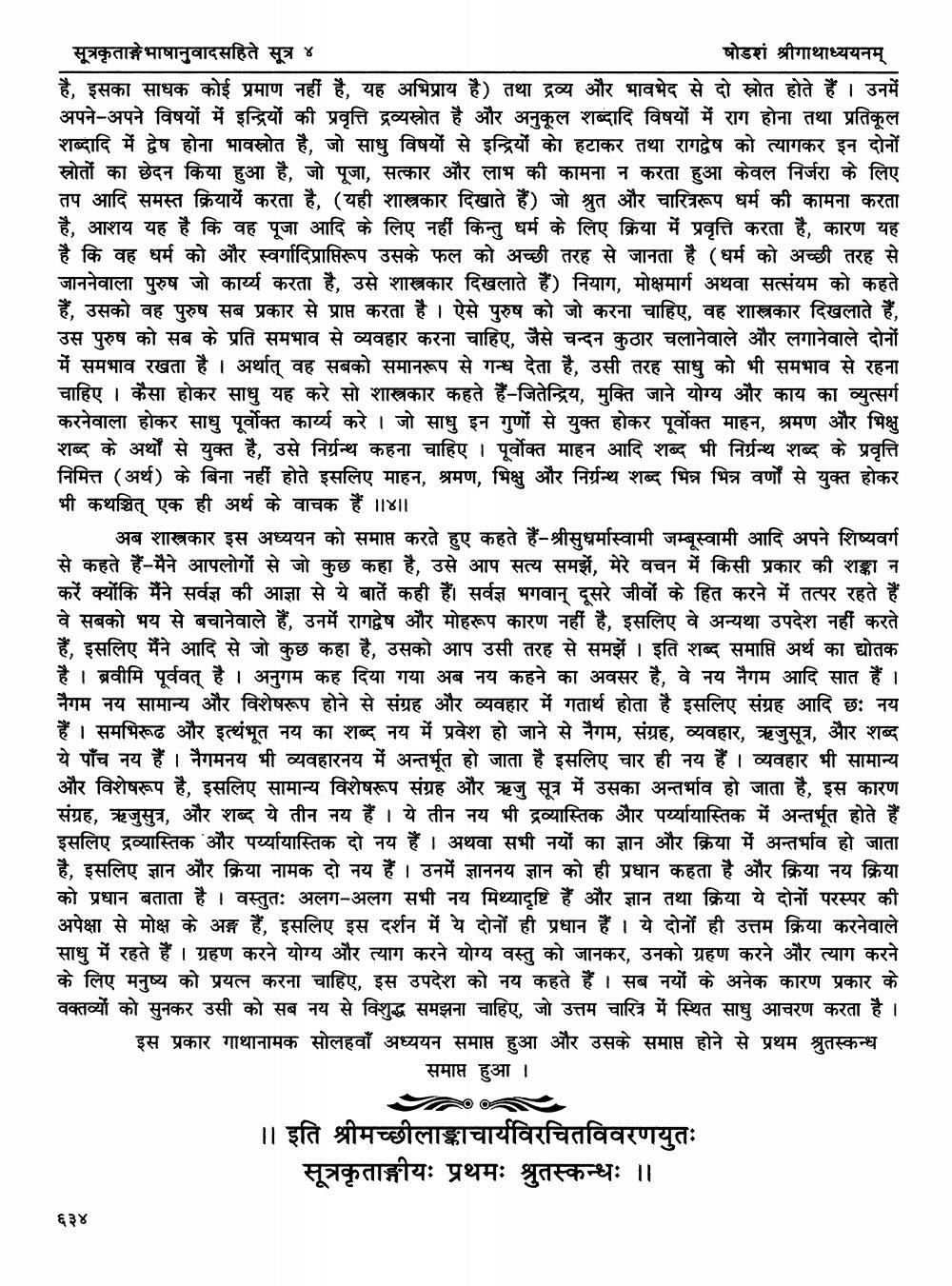________________
सूत्रकृताङ्गेभाषानुवादसहिते सूत्र ४
षोडशं श्रीगाथाध्ययनम् है, इसका साधक कोई प्रमाण नहीं है, यह अभिप्राय है) तथा द्रव्य और भावभेद से दो स्रोत होते हैं। उनमें अपने-अपने विषयों में इन्द्रियों की प्रवृत्ति द्रव्यस्रोत है और अनुकूल शब्दादि विषयों में राग होना तथा प्रतिकूल शब्दादि में द्वेष होना भावस्रोत है, जो साधु विषयों से इन्द्रियों को हटाकर तथा रागद्वेष को त्यागकर इन दोनों स्रोतों का छेदन किया हुआ है, जो पूजा, सत्कार और लाभ की कामना न करता हुआ केवल निर्जरा के लिए तप आदि समस्त क्रियायें करता है, (यही शास्त्रकार दिखाते हैं) जो श्रुत और चारित्ररूप धर्म की कामना करता है, आशय यह है कि वह पूजा आदि के लिए नहीं किन्तु धर्म के लिए क्रिया में प्रवृत्ति करता है, कारण यह है कि वह धर्म को और स्वर्गादिप्राप्तिरूप उसके फल को अच्छी तरह से जानता है (धर्म को अच्छी तरह से जाननेवाला पुरुष जो कार्य करता है, उसे शास्त्रकार दिखलाते हैं) नियाग, मोक्षमार्ग अथवा सत्संयम को कहते हैं, उसको वह पुरुष सब प्रकार से प्राप्त करता है। ऐसे पुरुष को जो करना चाहिए, वह शास्त्र उस पुरुष को सब के प्रति समभाव से व्यवहार करना चाहिए, जैसे चन्दन कुठार चलानेवाले और लगानेवाले दोनों में समभाव रखता है । अर्थात् वह सबको समानरूप से गन्ध देता है, उसी तरह साधु को भी समभाव से रहना चाहिए । कैसा होकर साधु यह करे सो शास्त्रकार कहते हैं-जितेन्द्रिय, मुक्ति जाने योग्य और काय का व्युत्सर्ग करनेवाला होकर साधु पूर्वोक्त कार्य करे । जो साधु इन गुणों से युक्त होकर पूर्वोक्त माहन, श्रमण और भिक्षु शब्द के अर्थों से युक्त है, उसे निर्ग्रन्थ कहना चाहिए । पूर्वोक्त माहन आदि शब्द भी निर्ग्रन्थ शब्द के प्रवृत्ति निमित्त (अर्थ) के बिना नहीं होते इसलिए माहन, श्रमण, भिक्षु और निर्ग्रन्थ शब्द भिन्न भिन्न वर्गों से युक्त होकर भी कथञ्चित् एक ही अर्थ के वाचक हैं ॥४॥
अब शास्त्रकार इस अध्ययन को समाप्त करते हुए कहते हैं-श्रीसुधर्मास्वामी जम्बूस्वामी आदि अपने शिष्यवर्ग से कहते हैं-मैने आपलोगों से जो कुछ कहा है, उसे आप सत्य समझें, मेरे वचन में किसी प्रकार की शङ्का न करें क्योंकि मैंने सर्वज्ञ की आज्ञा से ये बातें कही हैं। सर्वज्ञ भगवान् दूसरे जीवों के हित करने में तत्पर रहते हैं वे सबको भय से बचानेवाले हैं, उनमें रागद्वेष और मोहरूप कारण नहीं है, इसलिए वे अन्यथा उपदेश नहीं करते हैं, इसलिए मैंने आदि से जो कुछ कहा है, उसको आप उसी तरह से समझें । इति शब्द समाप्ति अर्थ का द्योतक है । ब्रवीमि पूर्ववत् है । अनुगम कह दिया गया अब नय कहने का अवसर है, वे नय नैगम आदि सात हैं। नैगम नय सामान्य और विशेषरूप होने से संग्रह और व्यवहार में गतार्थ होता है इसलिए संग्रह आदि छः नय हैं । समभिरूढ और इत्थंभूत नय का शब्द नय में प्रवेश हो जाने से नैगम, संग्रह, व्यवहार, ऋजुसूत्र, और शब्द ये पाँच नय हैं । नैगमनय भी व्यवहारनय में अन्तर्भूत हो जाता है इसलिए चार ही नय हैं । व्यवहार भी सामान्य और विशेषरूप है, इसलिए सामान्य विशेषरूप संग्रह और ऋजु सूत्र में उसका अन्तर्भाव हो जाता है, इस कारण संग्रह, ऋजुसुत्र, और शब्द ये तीन नय हैं । ये तीन नय भी द्रव्यास्तिक और पर्यायास्तिक में अन्तर्भूत होते हैं इसलिए द्रव्यास्तिक और पर्यायास्तिक दो नय हैं । अथवा सभी नयों का ज्ञान और क्रिया में अन्तर्भाव हो जाता है, इसलिए ज्ञान और क्रिया नामक दो नय हैं। उनमें ज्ञाननय ज्ञान को ही प्रधान कहता है और क्रिया नय क्रिया को प्रधान बताता है । वस्तुतः अलग-अलग सभी नय मिथ्यादष्टि हैं और ज्ञान तथा क्रिया ये दोनों परस्पर की अपेक्षा से मोक्ष के अङ्ग हैं, इसलिए इस दर्शन में ये दोनों ही प्रधान हैं। ये दोनों ही उत्तम क्रिया करनेवाले साधु में रहते हैं । ग्रहण करने योग्य और त्याग करने योग्य वस्तु को जानकर, उनको ग्रहण करने और त्याग करने के लिए मनुष्य को प्रयत्न करना चाहिए, इस उपदेश को नय कहते हैं । सब नयों के अनेक कारण प्रकार के वक्तव्यों को सुनकर उसी को सब नय से विशुद्ध समझना चाहिए, जो उत्तम चारित्र में स्थित साधु आचरण करता है। इस प्रकार गाथानामक सोलहवाँ अध्ययन समाप्त हुआ और उसके समाप्त होने से प्रथम श्रुतस्कन्ध
समाप्त हुआ ।
।। इति श्रीमच्छीलाङ्काचार्यविरचितविवरणयुतः
सूत्रकृताङ्गीयः प्रथमः श्रुतस्कन्धः ।।
६३४