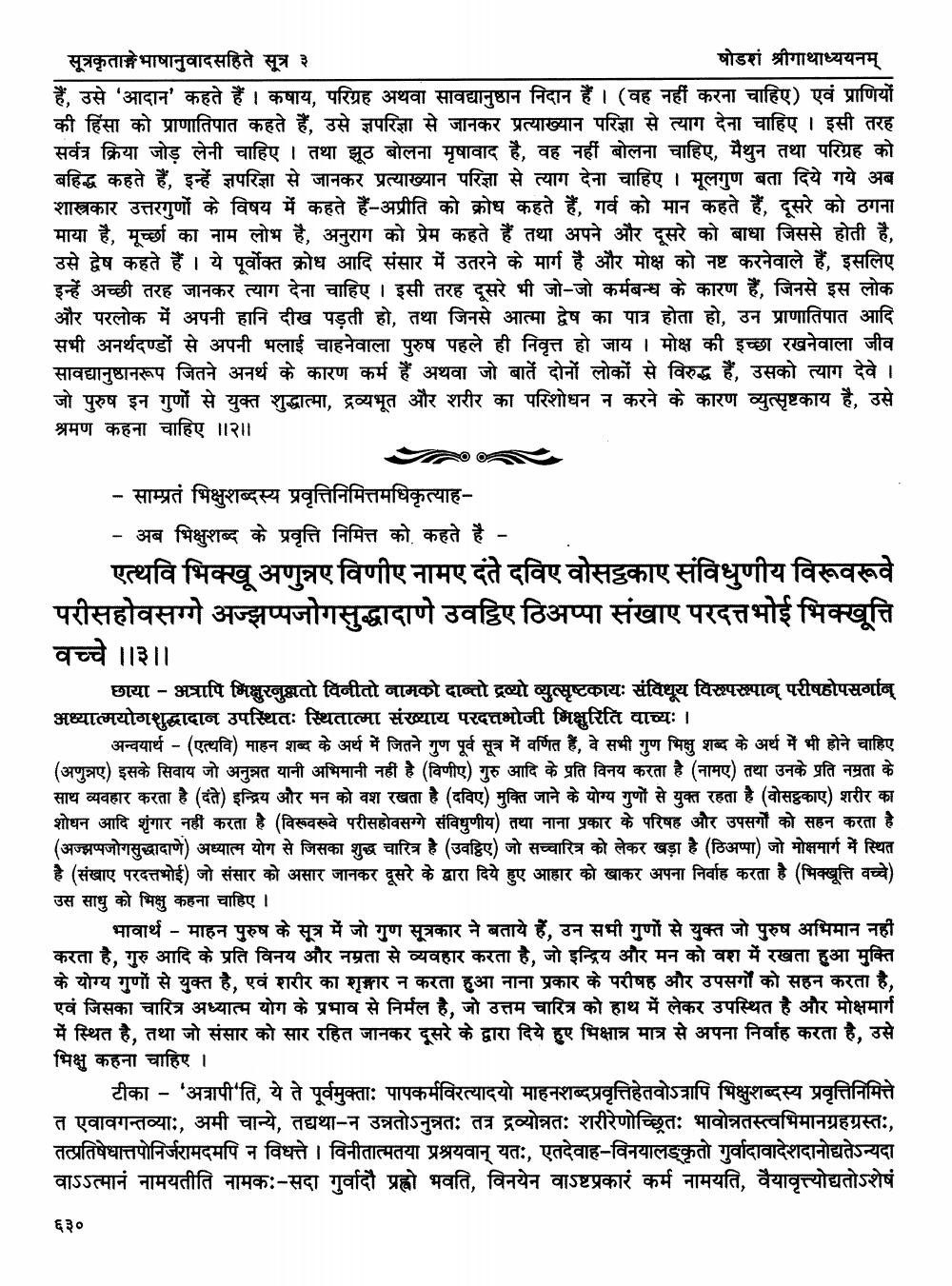________________
सूत्रकृताङ्गे भाषानुवादसहिते सूत्र ३
षोडशं श्रीगाथाध्ययनम्
हैं, उसे 'आदान' कहते हैं । कषाय, परिग्रह अथवा सावद्यानुष्ठान निदान हैं। ( वह नहीं करना चाहिए) एवं प्राणियों की हिंसा को प्राणातिपात कहते हैं, उसे ज्ञपरिज्ञा से जानकर प्रत्याख्यान परिज्ञा से त्याग देना चाहिए । इसी तरह सर्वत्र क्रिया जोड़ लेनी चाहिए । तथा झूठ बोलना मृषावाद है, वह नहीं बोलना चाहिए, मैथुन तथा परिग्रह को बहिद्ध कहते हैं, इन्हें ज्ञपरिज्ञा से जानकर प्रत्याख्यान परिज्ञा से त्याग देना चाहिए । मूलगुण बता दिये गये अब शास्त्रकार उत्तरगुणों के विषय में कहते हैं- अप्रीति को क्रोध कहते हैं, गर्व को मान कहते हैं, दूसरे को ठगना माया है, मूर्च्छा का नाम लोभ है, अनुराग को प्रेम कहते हैं तथा अपने और दूसरे को बाधा जिससे होती है, उसे द्वेष कहते हैं । ये पूर्वोक्त क्रोध आदि संसार में उतरने के मार्ग है और मोक्ष को नष्ट करनेवाले हैं, इसलिए इन्हें अच्छी तरह जानकर त्याग देना चाहिए । इसी तरह दूसरे भी जो-जो कर्मबन्ध के कारण हैं, जिनसे इस लोक और परलोक में अपनी हानि दीख पड़ती हो, तथा जिनसे आत्मा द्वेष का पात्र होता हो, उन प्राणातिपात आदि सभी अनर्थदण्डों से अपनी भलाई चाहनेवाला पुरुष पहले ही निवृत्त हो जाय । मोक्ष की इच्छा रखनेवाला जीव सावद्यानुष्ठानरूप जितने अनर्थ के कारण कर्म हैं अथवा जो बातें दोनों लोकों से विरुद्ध हैं, उसको त्याग देवे । जो पुरुष इन गुणों से युक्त शुद्धात्मा, द्रव्यभूत और शरीर का परिशोधन न करने के कारण व्युत्सृष्टकाय है, उसे श्रमण कहना चाहिए || २ ||
साम्प्रतं भिक्षुशब्दस्य प्रवृत्तिनिमित्तमधिकृत्याह
अब भिक्षुशब्द के प्रवृत्ति निमित्त को कहते है
एत्थवि भिक्खू अणुन्न विणीए नामए दंते दविए वोसट्टकाए संविधुणीय विरूवरूवे परीसहोवसग्गे अज्झप्पजोगसुद्धादाणे उवट्ठिए ठिअप्पा संखाए परदत्त भोई भिक्खुत्ति वच्चे ॥३॥
-
छाया - अत्रापि भिक्षुरनुन्नतो विनीतो नामको दान्तो द्रव्यो व्युत्सृष्टकायः संविधूय विरूपरूपान् परीषहोपसर्गान् अध्यात्मयोगशुद्धादान उपस्थितः स्थितात्मा संख्याय परदत्तभोजी भिक्षुरिति वाच्यः ।
अन्वयार्थ - (एत्थवि) माहन शब्द के अर्थ में जितने गुण पूर्व सूत्र में वर्णित हैं, वे सभी गुण भिक्षु शब्द के अर्थ में भी होने चाहिए (अन्न) इसके सिवाय जो अनुन्नत यानी अभिमानी नहीं है ( विणीए) गुरु आदि के प्रति विनय करता है ( नामए) तथा उनके प्रति नम्रता के साथ व्यवहार करता है (दंते) इन्द्रिय और मन को वश रखता है ( दविए) मुक्ति जाने के योग्य गुणों से युक्त रहता है (वोसट्टकाए) शरीर का शोधन आदि शृंगार नहीं करता है ( विरूवरूवे परीसहोवसग्गे संविधुणीय) तथा नाना प्रकार के परिषह और उपसर्गों को सहन करता है ( अज्झप्पजोगसुद्धादाणे) अध्यात्म योग से जिसका शुद्ध चारित्र है ( उवट्ठिए) जो सच्चारित्र को लेकर खड़ा है (ठिअप्पा) जो मोक्षमार्ग में स्थित है ( संखाए परदत्तभोई) जो संसार को असार जानकर दूसरे के द्वारा दिये हुए आहार को खाकर अपना निर्वाह करता है ( भिक्खुत्ति वच्चे) उस साधु को भिक्षु कहना चाहिए ।
भावार्थ - माहन पुरुष के सूत्र में जो गुण सूत्रकार ने बताये हैं, उन सभी गुणों से युक्त जो पुरुष अभिमान नहीं करता है, गुरु आदि के प्रति विनय और नम्रता से व्यवहार करता है, जो इन्द्रिय और मन को वश में रखता हुआ मुक्ति के योग्य गुणों से युक्त है, एवं शरीर का शृङ्गार न करता हुआ नाना प्रकार के परीषह और उपसर्गों को सहन करता है, एवं जिसका चारित्र अध्यात्म योग के प्रभाव से निर्मल है, जो उत्तम चारित्र को हाथ में लेकर उपस्थित है और मोक्षमार्ग में स्थित है, तथा जो संसार को सार रहित जानकर दूसरे के द्वारा दिये हुए भिक्षान्त्र मात्र से अपना निर्वाह करता है, उसे भिक्षु कहना चाहिए ।
टीका - ‘अत्रापी'ति, ये ते पूर्वमुक्ताः पापकर्मविरत्यादयो माहनशब्दप्रवृत्तिहेतवोऽत्रापि भिक्षुशब्दस्य प्रवृत्तिनिमित्ते त एवावगन्तव्याः, अमी चान्ये, तद्यथा- न उन्नतोऽनुन्नतः तत्र द्रव्योन्नतः शरीरेणोच्छ्रितः भावोन्नतस्त्वभिमानग्रहग्रस्तः, तत्प्रतिषेधात्तपोनिर्जरामदमपि न विधत्ते । विनीतात्मतया प्रश्रयवान् यतः, एतदेवाह - विनयालङ्कृतो गुर्वादावादेशदानोद्यतेऽन्यदा वाऽऽत्मानं नामयतीति नामकः - सदा गुर्वादौ प्रह्वो भवति, विनयेन वाऽष्टप्रकारं कर्म नामयति, वैयावृत्त्योद्यतोऽशेषं
६३०