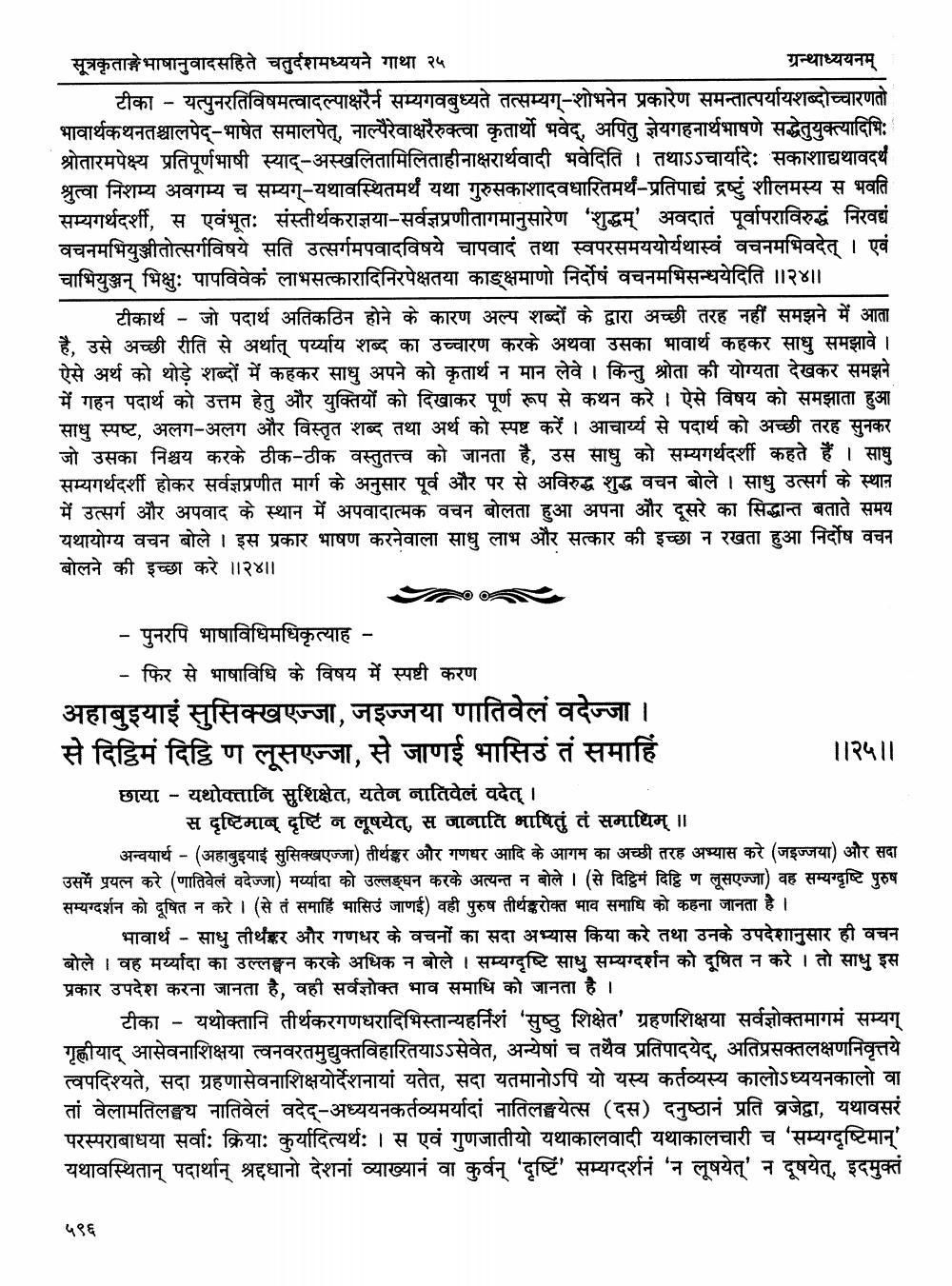________________
सूत्रकृताङ्गे भाषानुवादसहिते चतुर्दशमध्ययने गाथा २५
ग्रन्थाध्ययनम्
टीका - यत्पुनरतिविषमत्वादल्पाक्षरैर्न सम्यगवबुध्यते तत्सम्यग् - शोभनेन प्रकारेण समन्तात्पर्यायशब्दोच्चारणतो भावार्थकथनतःश्चालपेद्-भाषेत समालपेत्, नाल्पैरेवाक्षरैरुक्त्वा कृतार्थो भवेद्, अपितु ज्ञेयगहनार्थभाषणे सद्धेतुयुक्त्यादिभिः । श्रोतारमपेक्ष्य प्रतिपूर्ण भाषी स्याद्-अस्खलितामिलिताहीनाक्षरार्थवादी भवेदिति । तथाऽऽचार्यादेः सकाशाद्यथावदर्थं श्रुत्वा निशम्य अवगम्य च सम्यग् - यथावस्थितमर्थं यथा गुरुसकाशादवधारितमर्थं प्रतिपाद्यं द्रष्टुं शीलमस्य स भवति सम्यगर्थदर्शी, स एवंभूतः संस्तीर्थकराज्ञया - सर्वज्ञप्रणीतागमानुसारेण 'शुद्धम्' अवदातं पूर्वापराविरुद्धं निरवद्यं वचनमभियुञ्जीतोत्सर्गविषये सति उत्सर्गमपवादविषये चापवादं तथा स्वपरसमययोर्यथास्वं वचनमभिवदेत् । एवं चाभियुञ्जन् भिक्षुः पापविवेकं लाभसत्कारादिनिरपेक्षतया काङ्क्षमाणो निर्दोषं वचनमभिसन्धयेदिति ॥२४॥
टीकार्थ जो पदार्थ अतिकठिन होने के कारण अल्प शब्दों के द्वारा अच्छी तरह नहीं समझने में आता है, उसे अच्छी रीति से अर्थात् पर्य्याय शब्द का उच्चारण करके अथवा उसका भावार्थ कहकर साधु समझावे । ऐसे अर्थ को थोड़े शब्दों में कहकर साधु अपने को कृतार्थ न मान लेवे । किन्तु श्रोता की योग्यता देखकर समझने में गहन पदार्थ को उत्तम हेतु और युक्तियों को दिखाकर पूर्ण रूप से कथन करे। ऐसे विषय को समझाता हुआ साधु स्पष्ट, अलग-अलग और विस्तृत शब्द तथा अर्थ को स्पष्ट करें। आचार्य्य से पदार्थ को अच्छी तरह सुनकर जो उसका निश्चय करके ठीक-ठीक वस्तुतत्त्व को जानता है, उस साधु को सम्यगर्थदर्शी कहते हैं । साधु सम्यगर्थदर्शी होकर सर्वज्ञप्रणीत मार्ग के अनुसार पूर्व और पर से अविरुद्ध शुद्ध वचन बोले । साधु उत्सर्ग के स्थान में उत्सर्ग और अपवाद के स्थान में अपवादात्मक वचन बोलता हुआ अपना और दूसरे का सिद्धान्त बताते समय यथायोग्य वचन बोले । इस प्रकार भाषण करनेवाला साधु लाभ और सत्कार की इच्छा न रखता हुआ निर्दोष वचन बोलने की इच्छा करे ||२४||
पुनरपि भाषाविधिमधिकृत्याह -
-
फिर से भाषाविधि के विषय में स्पष्टी करण
अहाबुइयाई सुसिक्खएज्जा, जइज्जया णातिवेलं वदेज्जा ।
से दिट्ठिमं दिट्ठि ण लूसएज्जा, से जाणई भासिउं तं समाहिं
-
छाया -
यथोक्तानि सुशिक्षेत, यतेन नातिवेलं वदेत् ।
स दृष्टिमान् दृष्टि न लूषयेत्, स जानाति भाषितुं तं समाधिम् ॥
५९६
।।२५।।
अन्वयार्थ - ( अहाबुइयाई सुसिक्खएज्जा) तीर्थङ्कर और गणधर आदि के आगम का अच्छी तरह अभ्यास करे ( जइज्जया) और सदा उसमें प्रयत्न करे ( णातिवेलं वदेज्जा) मर्य्यादा को उल्लङ्घन करके अत्यन्त न बोले । ( से दिट्ठिमं दिट्ठि ण लूसएज्जा) वह सम्यग्दृष्टि पुरुष सम्यग्दर्शन को दूषित न करे । ( से तं समाहिं भासिउं जाणई) वही पुरुष तीर्थङ्करोक्त भाव समाधि को कहना जानता है ।
भावार्थ - साधु तीर्थंकर और गणधर के वचनों का सदा अभ्यास किया करे तथा उनके उपदेशानुसार ही वचन बोले । वह मर्य्यादा का उल्लङ्घन करके अधिक न बोले । सम्यग्दृष्टि साधु सम्यग्दर्शन को दूषित न करे । तो साधु इस प्रकार उपदेश करना जानता है, वही सर्वज्ञोक्त भाव समाधि को जानता है ।
टीका यथोक्तानि तीर्थकरगणधरादिभिस्तान्यहर्निशं 'सुष्ठु शिक्षेत ' ग्रहणशिक्षया सर्वज्ञोक्तमागमं सम्यग् गृह्णीयाद् आसेवनाशिक्षया त्वनवरतमुद्युक्तविहारितयाऽऽसेवेत, अन्येषां च तथैव प्रतिपादयेद्, अतिप्रसक्तलक्षणनिवृत्तये त्वपदिश्यते, सदा ग्रहणासेवनाशिक्षयोर्देशनायां यतेत, सदा यतमानोऽपि यो यस्य कर्तव्यस्य कालोऽध्ययनकालो वा तां वेलामतिलङ्घय नातिवेलं वदेद्-अध्ययनकर्तव्यमर्यादां नातिलङ्घयेत्स (दस) दनुष्ठानं प्रति व्रजेद्वा, यथावसरं परस्पराबाधया सर्वाः क्रियाः कुर्यादित्यर्थः । स एवं गुणजातीयो यथाकालवादी यथाकालचारी च 'सम्यग्दृष्टिमान्' यथावस्थितान् पदार्थान् श्रद्दधानो देशनां व्याख्यानं वा कुर्वन् 'दृष्टि' सम्यग्दर्शनं 'न लूषयेत्' न दूषयेत्, इदमुक्तं