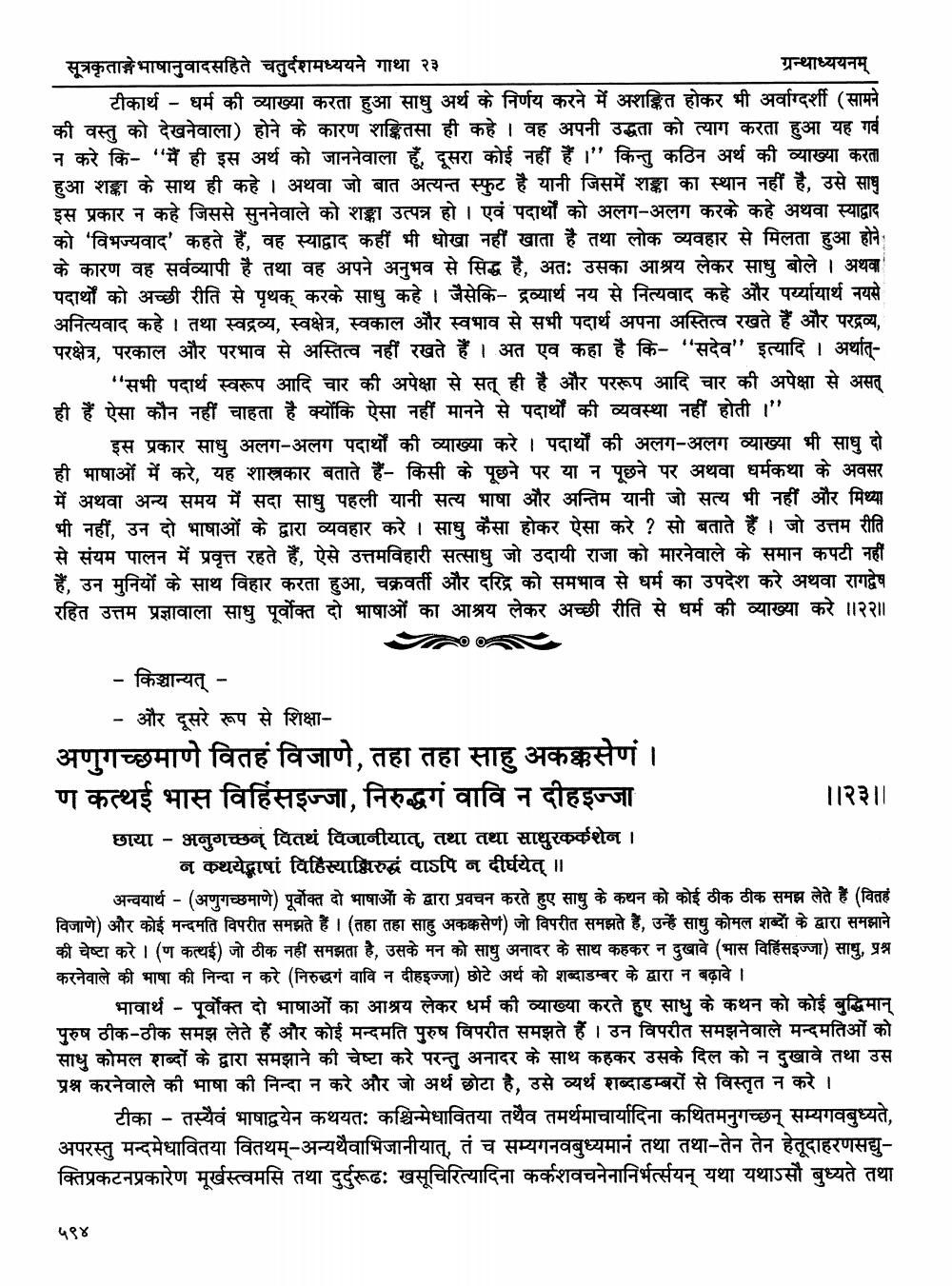________________
सूत्रकृताङ्गेभाषानुवादसहिते चतुर्दशमध्ययने गाथा २३
ग्रन्थाध्ययनम् टीकार्थ - धर्म की व्याख्या करता हुआ साधु अर्थ के निर्णय करने में अशङ्कित होकर भी अग्दिर्शी (सामने की वस्तु को देखनेवाला) होने के कारण शङ्कितसा ही कहे । वह अपनी उद्धता को त्याग करता हुआ यह गर्व न करे कि- "मैं ही इस अर्थ को जाननेवाला हूँ, दूसरा कोई नहीं हैं।" किन्तु कठिन अर्थ की व्याख्या करता हुआ शङ्का के साथ ही कहे । अथवा जो बात अत्यन्त स्फुट है यानी जिसमें शङ्का का स्थान नहीं है, उसे साधु इस प्रकार न कहे जिससे सुननेवाले को शङ्का उत्पन्न हो । एवं पदार्थों को अलग-अलग करके कहे अथवा स्याद्वाद को 'विभज्यवाद' कहते हैं, वह स्याद्वाद कहीं भी धोखा नहीं खाता है तथा लोक व्यवहार से मिलता हुआ होने के कारण वह सर्वव्यापी है तथा वह अपने अनुभव से सिद्ध है, अतः उसका आश्रय लेकर साधु बोले । अथवा पदार्थों को अच्छी रीति से पृथक् करके साधु कहे । जैसेकि- द्रव्यार्थ नय से नित्यवाद कहे और पर्यायार्थ नयसे अनित्यवाद कहे । तथा स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल और स्वभाव से सभी पदार्थ अपना अस्तित्व रखते हैं और परद्रव्य, परक्षेत्र, परकाल और परभाव से अस्तित्व नहीं रखते हैं । अत एव कहा है कि- "सदेव" इत्यादि । अर्थात्
__ "सभी पदार्थ स्वरूप आदि चार की अपेक्षा से सत् ही है और पररूप आदि चार की अपेक्षा से असत् ही हैं ऐसा कौन नहीं चाहता है क्योंकि ऐसा नहीं मानने से पदार्थों की व्यवस्था नहीं होती ।"
इस प्रकार साधु अलग-अलग पदार्थों की व्याख्या करे । पदार्थों की अलग-अलग व्याख्या भी साधु दो ही भाषाओं में करे, यह शास्त्रकार बताते हैं- किसी के पूछने पर या न पूछने पर अथवा धर्मकथा के अवसर में अथवा अन्य समय में सदा साधु पहली यानी सत्य भाषा और अन्तिम यानी जो सत्य भी नहीं और मिथ्या भी नहीं, उन दो भाषाओं के द्वारा व्यवहार करे । साधु कैसा होकर ऐसा करे ? सो बताते हैं। जो उत्तम रीति से संयम पालन में प्रवृत्त रहते हैं, ऐसे उत्तमविहारी सत्साधु जो उदायी राजा को मारनेवाले के समान कपटी नहीं हैं, उन मुनियों के साथ विहार करता हुआ, चक्रवर्ती और दरिद्र को समभाव से धर्म का उपदेश करे अथवा रागद्वेष रहित उत्तम प्रज्ञावाला साधु पूर्वोक्त दो भाषाओं का आश्रय लेकर अच्छी रीति से धर्म की व्याख्या करे ॥२२॥
- किञ्चान्यत् -
- और दूसरे रूप से शिक्षाअणुगच्छमाणे वितहं विजाणे, तहा तहा साहु अकक्कसेणं । ण कत्थई भास विहिंसइज्जा, निरुद्धगं वावि न दीहइज्जा
॥२३॥ छाया - अनुगच्छन् वितथं विजानीयात्, तथा तथा साधुरकर्कशेन ।
न कथयेद्वाषां विहिंस्याविरुद्धं वाऽपि न दीर्घयेत् ॥ अन्वयार्थ - (अणुगच्छमाणे) पूर्वोक्त दो भाषाओं के द्वारा प्रवचन करते हुए साधु के कथन को कोई ठीक ठीक समझ लेते हैं (वितह विजाणे) और कोई मन्दमति विपरीत समझते हैं । (तहा तहा साहु अकक्कसेणं) जो विपरीत समझते हैं, उन्हें साधु कोमल शब्दों के द्वारा समझाने की चेष्टा करे । (ण कत्थई) जो ठीक नहीं समझता है, उसके मन को साधु अनादर के साथ कहकर न दुखावे (भास विहिंसइज्जा) साधु, प्रश्न करनेवाले की भाषा की निन्दा न करे (निरुद्धगं वावि न दीहइज्जा) छोटे अर्थ को शब्दाडम्बर के द्वारा न बढ़ावे ।
भावार्थ - पूर्वोक्त दो भाषाओं का आश्रय लेकर धर्म की व्याख्या करते हुए साधु के कथन को कोई बुद्धिमान पुरुष ठीक-ठीक समझ लेते हैं और कोई मन्दमति पुरुष विपरीत समझते हैं । उन विपरीत समझनेवाले मन्दमतिओं को साधु कोमल शब्दों के द्वारा समझाने की चेष्टा करे परन्तु अनादर के साथ कहकर उसके दिल को न दुखावे तथा उस प्रश्न करनेवाले की भाषा की निन्दा न करे और जो अर्थ छोटा है, उसे व्यर्थ शब्दाडम्बरों से विस्तृत न करे ।
टीका - तस्यैवं भाषाद्वयेन कथयतः कश्चिन्मेधावितया तथैव तमर्थमाचार्यादिना कथितमनुगच्छन् सम्यगवबुध्यते, अपरस्तु मन्दमेधावितया वितथम्-अन्यथैवाभिजानीयात्, तं च सम्यगनवबुध्यमानं तथा तथा-तेन तेन हेतूदाहरणसधुक्तिप्रकटनप्रकारेण मूर्खस्त्वमसि तथा दुर्दुरूढः खसूचिरित्यादिना कर्कशवचनेनानिर्भर्त्सयन् यथा यथाऽसौ बुध्यते तथा
५९४