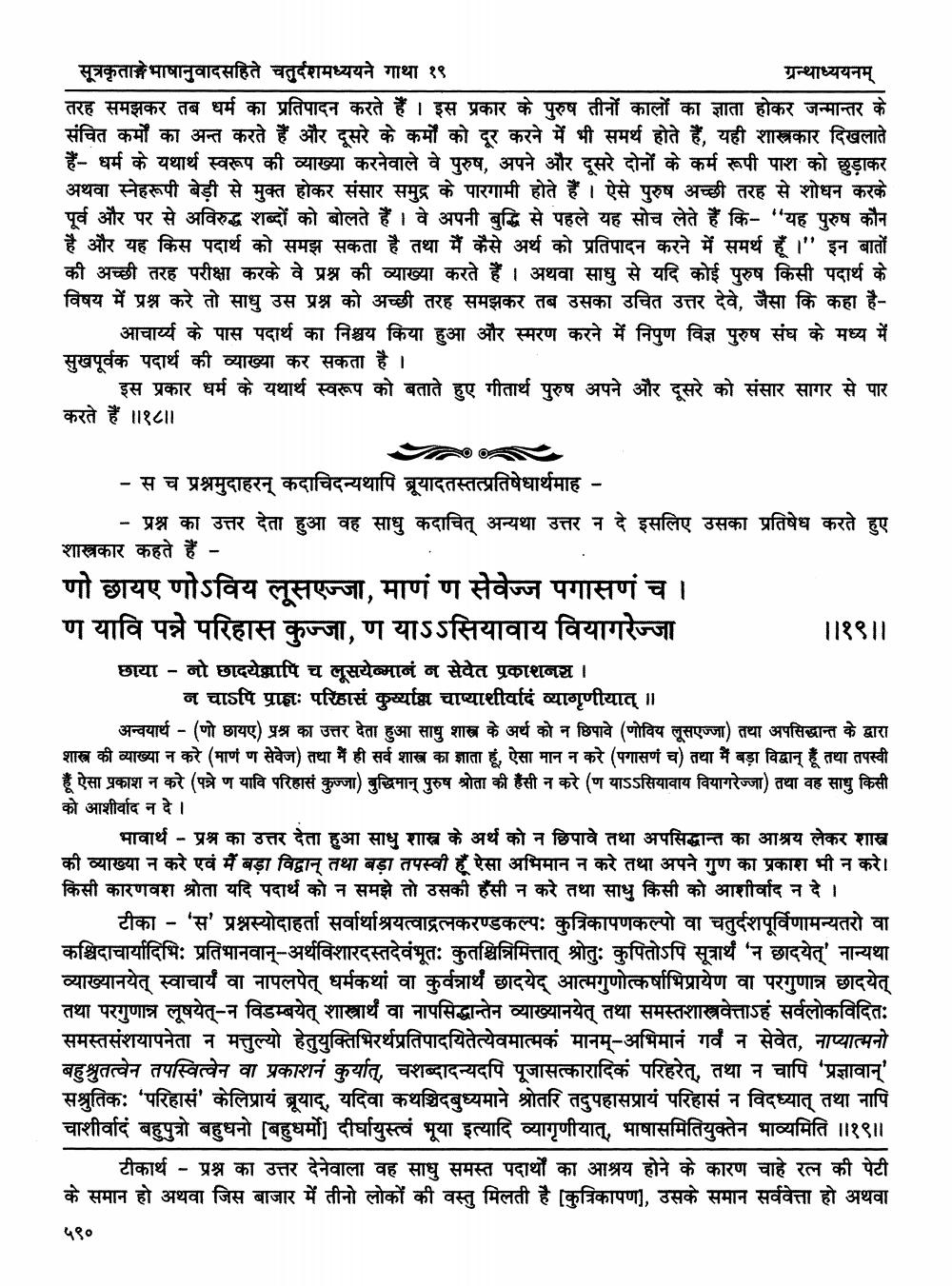________________
सूत्रकृताङ्गेभाषानुवादसहित चतुर्दशमध्ययने गाथा १९
ग्रन्थाध्ययनम् तरह समझकर तब धर्म का प्रतिपादन करते हैं । इस प्रकार के पुरुष तीनों कालों का ज्ञाता होकर जन्मान्तर के संचित कर्मों का अन्त करते हैं और दूसरे के कर्मों को दूर करने में भी समर्थ होते हैं, यही शास्त्रकार दिखलाते हैं- धर्म के यथार्थ स्वरूप की व्याख्या करनेवाले वे पुरुष, अपने और दूसरे दोनों के कर्म रूपी पाश को छुड़ाकर अथवा स्नेहरूपी बेड़ी से मुक्त होकर संसार समुद्र के पारगामी होते हैं। ऐसे पुरुष अच्छी तरह से शोधन करके पूर्व और पर से अविरुद्ध शब्दों को बोलते हैं। वे अपनी बुद्धि से पहले यह सोच लेते हैं कि- "यह पुरुष कौन है और यह किस पदार्थ को समझ सकता है तथा मैं कैसे अर्थ को प्रतिपादन करने में समर्थ हूँ।" इन बातों की अच्छी तरह परीक्षा करके वे प्रश्न की व्याख्या करते हैं । अथवा साधु से यदि कोई पुरुष किसी पदार्थ के विषय में प्रश्न करे तो साधु उस प्रश्न को अच्छी तरह समझकर तब उसका उचित उत्तर देवे, जैसा कि कहा है
आचार्य के पास पदार्थ का निश्चय किया हुआ और स्मरण करने में निपुण विज्ञ पुरुष संघ के मध्य में सुखपूर्वक पदार्थ की व्याख्या कर सकता है ।
इस प्रकार धर्म के यथार्थ स्वरूप को बताते हुए गीतार्थ पुरुष अपने और दूसरे को संसार सागर से पार करते हैं ॥१८॥
- स च प्रश्नमुदाहरन् कदाचिदन्यथापि ब्रूयादतस्तत्प्रतिषेधार्थमाह -
- प्रश्न का उत्तर देता हुआ वह साधु कदाचित् अन्यथा उत्तर न दे इसलिए उसका प्रतिषेध करते हुए शास्त्रकार कहते हैं - णो छायए णोऽविय लूसएज्जा, माणं ण सेवेज्ज पगासणं च । ण यावि पन्ने परिहास कुज्जा, ण याऽऽसियावाय वियागरेज्जा
॥१९॥ छाया - नो छादयेनापि च लूसयेब्मानं न सेवेत प्रकाशनश ।
न चाऽपि प्राज्ञः परिहासं कुर्य्याश चाप्याशीर्वादं व्यागणीयात् ॥ अन्वयार्थ - (णो छायए) प्रश्न का उत्तर देता हुआ साधु शास्त्र के अर्थ को न छिपावे (णोविय लूसएज्जा) तथा अपसिद्धान्त के द्वारा शास्त्र की व्याख्या न करे (माणं ण सेवेज) तथा मैं ही सर्व शास्त्र का ज्ञाता हूं, ऐसा मान न करे (पगासणं च) तथा मैं बड़ा विद्वान् हूँ तथा तपस्वी हूँ ऐसा प्रकाश न करे (पन्ने ण यावि परिहास कुज्जा) बुद्धिमान् पुरुष श्रोता की हसी न करे (ण याऽऽसियावाय वियागरेज्जा) तथा वह साधु किसी को आशीर्वाद न दे।
भावार्थ- प्रश्न का उत्तर देता हुआ साधु शास्त्र के अर्थ को न छिपावे तथा अपसिद्धान्त का आश्रय लेकर शास्त्र की व्याख्या न करे एवं मैं बड़ा विद्वान् तथा बड़ा तपस्वी हैं ऐसा अभिमान न करे तथा अपने गुण का प्रकाश भी न करे। किसी कारणवश श्रोता यदि पदार्थ को न समझे तो उसकी हँसी न करे तथा साधु किसी को आशीर्वाद न दे ।
__टीका - 'स' प्रश्नस्योदाहर्ता सर्वार्थाश्रयत्वाद्रत्नकरण्डकल्पः कुत्रिकापणकल्पो वा चतुर्दशपूर्विणामन्यतरो वा कश्चिदाचार्यादिभिः प्रतिभानवान्-अर्थविशारदस्तदेवंभूतः कुतश्चिन्निमित्तात् श्रोतुः कुपितोऽपि सूत्रार्थ 'न छादयेत्' नान्यथा व्याख्यानयेत् स्वाचार्यं वा नापलपेत् धर्मकथां वा कुर्वन्नार्थं छादयेद् आत्मगुणोत्कर्षाभिप्रायेण वा परगुणान्न छादयेत् तथा परगुणान्न लूषयेत्-न विडम्बयेत् शास्त्रार्थ वा नापसिद्धान्तेन व्याख्यानयेत् तथा समस्तशास्त्रवेत्ताऽहं सर्वलोकविदितः समस्तसंशयापनेता न मत्तुल्यो हेतुयुक्तिभिरर्थप्रतिपादयितेत्येवमात्मकं मानम्-अभिमानं गर्व न सेवेत, नाप्यात्मनो बहुश्रुतत्वेन तपस्वित्वेन वा प्रकाशनं कुर्यात्, चशब्दादन्यदपि पूजासत्कारादिकं परिहरेत्, तथा न चापि 'प्रज्ञावान्' सश्रुतिकः 'परिहासं' केलिप्रायं ब्रूयाद्, यदिवा कथञ्चिदबुध्यमाने श्रोतरि तदुपहासप्रायं परिहासं न विदध्यात् तथा नापि चाशीर्वादं बहुपुत्रो बहुधनो [बहुधर्मो] दीर्घायुस्त्वं भूया इत्यादि व्यागृणीयात्, भाषासमितियुक्तेन भाव्यमिति ॥१९॥
टीकार्थ - प्रश्न का उत्तर देनेवाला वह साधु समस्त पदार्थों का आश्रय होने के कारण चाहे रत्न की पेटी के समान हो अथवा जिस बाजार में तीनो लोकों की वस्तु मिलती है (कुत्रिकापण], उसके समान सर्ववेत्ता हो अथवा
५९०