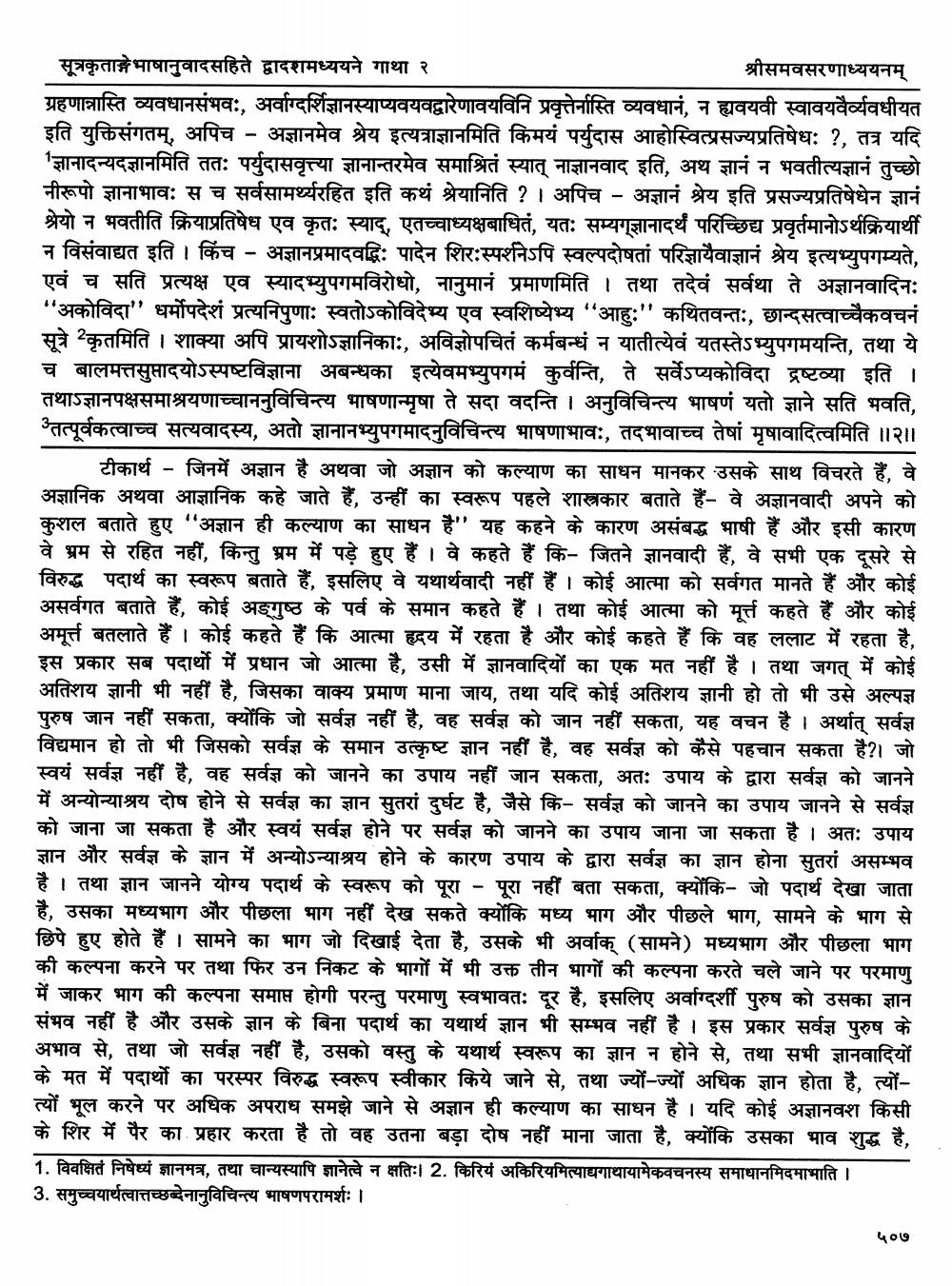________________
सूत्रकृताङ्गेभाषानुवादसहिते द्वादशमध्ययने गाथा २
श्रीसमवसरणाध्ययनम् ग्रहणान्नास्ति व्यवधानसंभवः, अर्वाग्दर्शिज्ञानस्याप्यवयवद्वारेणावयविनि प्रवृत्तेर्नास्ति व्यवधानं, न ह्यवयवी स्वावयवैर्व्यवधीयत इति युक्तिसंगतम्, अपिच - अज्ञानमेव श्रेय इत्यत्राज्ञानमिति किमयं पर्युदास आहोस्वित्प्रसज्यप्रतिषेधः ?, तत्र यदि 'ज्ञानादन्यदज्ञानमिति ततः पर्युदासवृत्त्या ज्ञानान्तरमेव समाश्रितं स्यात् नाज्ञानवाद इति, अथ ज्ञानं न भवतीत्यज्ञानं तुच्छो नीरूपो ज्ञानाभावः स च सर्वसामर्थ्यरहित इति कथं श्रेयानिति ? । अपिच - अज्ञानं श्रेय इति प्रसज्यप्रतिषेधेन ज्ञानं श्रेयो न भवतीति क्रियाप्रतिषेध एव कृतः स्याद्, एतच्चाध्यक्षबाधितं, यतः सम्यग्ज्ञानादर्थं परिच्छिद्य प्रवृर्तमानोऽर्थक्रियार्थी न विसंवाद्यत इति । किंच - अज्ञानप्रमादवद्भिः पादेन शिरःस्पर्शनेऽपि स्वल्पदोषतां परिज्ञायैवाज्ञानं श्रेय इत्यभ्युपगम्यते, एवं च सति प्रत्यक्ष एव स्यादभ्युपगमविरोधो, नानुमानं प्रमाणमिति । तथा तदेवं सर्वथा ते अज्ञानवादिनः "अकोविदा" धर्मोपदेशं प्रत्यनिपुणाः स्वतोऽकोविदेभ्य एव स्वशिष्येभ्य "आहुः" कथितवन्तः, छान्दसत्वाच्चैकवचनं सूत्रे कृतमिति । शाक्या अपि प्रायशोऽज्ञानिकाः, अविज्ञोपचितं कर्मबन्धं न यातीत्येवं यतस्तेऽभ्युपगमयन्ति, तथा ये च बालमत्तसुप्तादयोऽस्पष्टविज्ञाना अबन्धका इत्येवमभ्युपगमं कुर्वन्ति, ते सर्वेऽप्यकोविदा द्रष्टव्या इति । तथाऽज्ञानपक्षसमाश्रयणाच्चाननुविचिन्त्य भाषणान्मृषा ते सदा वदन्ति । अनुविचिन्त्य भाषणं यतो ज्ञाने सति भवति, तत्पूर्वकत्वाच्च सत्यवादस्य, अतो ज्ञानानभ्युपगमादनुविचिन्त्य भाषणाभावः, तदभावाच्च तेषां मृषावादित्वमिति ॥२॥
टीकार्थ - जिनमें अज्ञान है अथवा जो अज्ञान को कल्याण का साधन मानकर उसके साथ विचरते हैं, वे अज्ञानिक अथवा आज्ञानिक कहे जाते हैं, उन्हीं का स्वरूप पहले शास्त्रकार बताते हैं- वे अज्ञानवादी अपने को कुशल बताते हुए "अज्ञान ही कल्याण का साधन है" यह कहने के कारण असंबद्ध भाषी हैं और इसी कारण वे भ्रम से रहित नहीं, किन्तु भ्रम में पड़े हुए हैं। वे कहते हैं कि- जितने ज्ञानवादी हैं, वे सभी एक दूसरे से विरुद्ध पदार्थ का स्वरूप बताते हैं, इसलिए वे यथार्थवादी नहीं हैं। कोई आत्मा को सर्वगत मानते हैं और कोई असर्वगत बताते हैं, कोई अङ्गुष्ठ के पर्व के समान कहते हैं । तथा कोई आत्मा को मूर्त कहते हैं और कोई अमूर्त बतलाते हैं । कोई कहते हैं कि आत्मा हृदय में रहता है और कोई कहते हैं कि वह ललाट में रहता है, इस प्रकार सब पदार्थों में प्रधान जो आत्मा है, उसी में ज्ञानवादियों का एक मत नहीं है । तथा जगत् में कोई अतिशय ज्ञानी भी नहीं है. जिसका वाक्य प्रमाण माना जाय. तथा यदि कोई अतिशय ज्ञानी हो तो भी उस पुरुष जान नहीं सकता, क्योंकि जो सर्वज्ञ नहीं है, वह सर्वज्ञ को जान नहीं सकता, यह वचन है । अर्थात् सर्वज्ञ विद्यमान हो तो भी जिसको सर्वज्ञ के समान उत्कृष्ट ज्ञान नहीं है, वह सर्वज्ञ को कैसे पहचान सकता है? जो स्वयं सर्वज्ञ नहीं है, वह सर्वज्ञ को जानने का उपाय नहीं जान सकता, अतः उपाय के द्वारा सर्वज्ञ को जानने में अन्योन्याश्रय दोष होने से सर्वज्ञ का ज्ञान सुतरां दुर्घट है, जैसे कि- सर्वज्ञ को जानने का उपाय जानने से सर्वज्ञ को जाना जा सकता है और स्वयं सर्वज्ञ होने पर सर्वज्ञ को जानने का उपाय जाना जा सकता है। अतः उपाय ज्ञान और सर्वज्ञ के ज्ञान में अन्योऽन्याश्रय होने के कारण उपाय के द्वारा सर्वज्ञ का ज्ञान होना सुतरां असम्भव है । तथा ज्ञान जानने योग्य पदार्थ के स्वरूप को पूरा - पूरा नहीं बता सकता, क्योंकि- जो पदार्थ देखा जाता है, उसका मध्यभाग और पीछला भाग नहीं देख सकते क्योंकि मध्य भाग और पीछले भाग, सामने के भाग से छिपे हुए होते हैं । सामने का भाग जो दिखाई देता है, उसके भी अर्वाक् (सामने) मध्यभाग और पीछला भाग की कल्पना करने पर तथा फिर उन निकट के भागों में भी उक्त तीन भागों की कल्पना करते चले जाने पर परमाणु में जाकर भाग की कल्पना समाप्त होगी परन्तु परमाणु स्वभावतः दूर है, इसलिए अर्वाग्दी पुरुष को उसका ज्ञान संभव नहीं है और उसके ज्ञान के बिना पदार्थ का यथार्थ ज्ञान भी सम्भव नहीं है । इस प्रकार सर्वज्ञ पुरुष के अभाव से, तथा जो सर्वज्ञ नहीं है, उसको वस्तु के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान न होने से, तथा सभी ज्ञानवादियों के मत में पदार्थो का परस्पर विरुद्ध स्वरूप स्वीकार किये जाने से, तथा ज्यों-ज्यों अधिक ज्ञान होता है, त्योंत्यों भूल करने पर अधिक अपराध समझे जाने से अज्ञान ही कल्याण का साधन है । यदि कोई अज्ञानवश किसी
करता है तो वह उतना बड़ा दोष नहीं माना जाता है, क्योंकि उसका भाव शुद्ध है, 1. विवक्षितं निषेध्यं ज्ञानमत्र, तथा चान्यस्यापि ज्ञानेत्वे न क्षतिः। 2. किरियं अकिरियमित्याधगाथायामेकवचनस्य समाधानमिदमाभाति । 3. समुच्चयार्थत्वात्तच्छब्देनानुविचिन्त्य भाषणपरामर्शः।
५०७