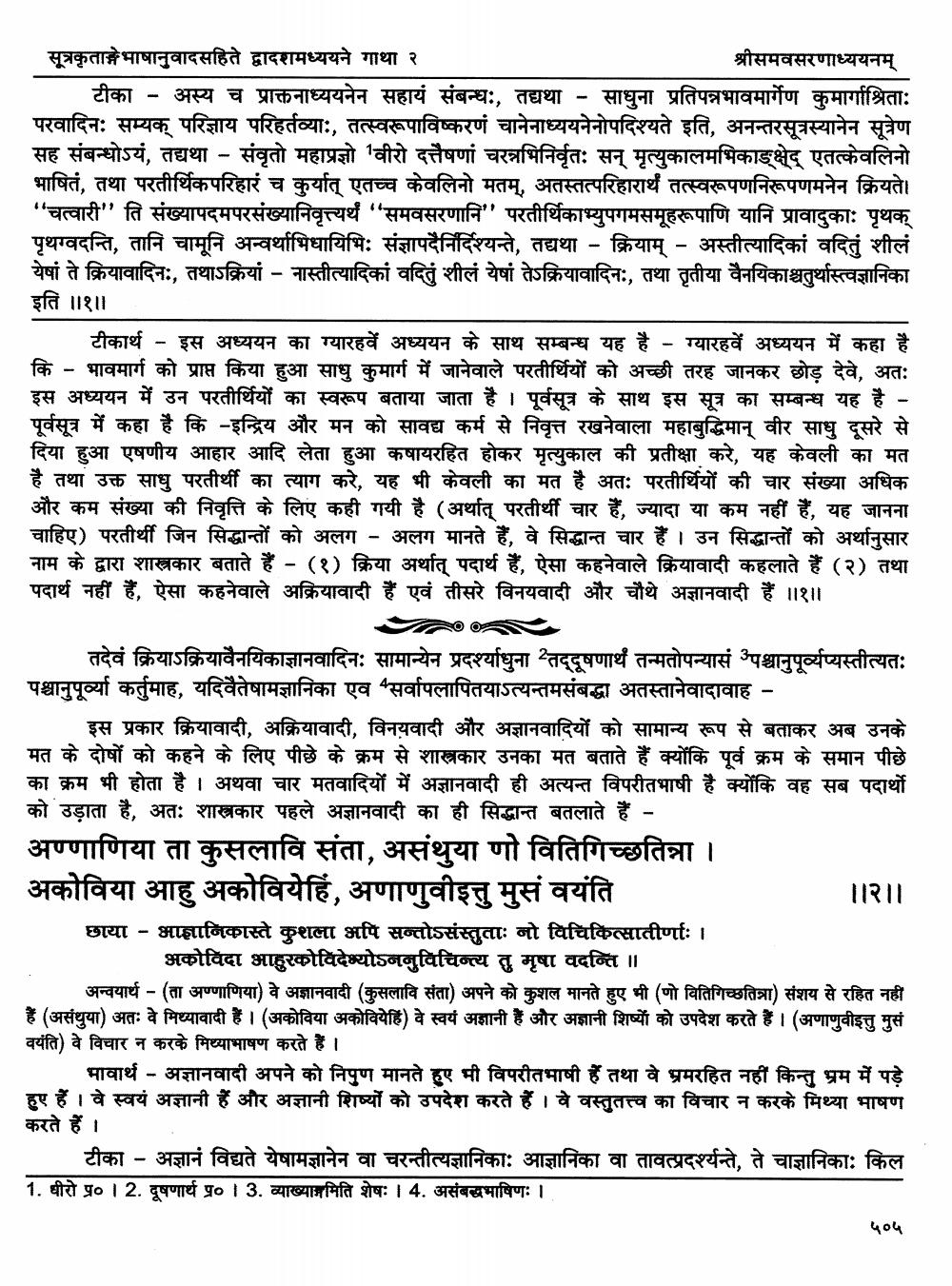________________
सूत्रकृताङ्गेभाषानुवादसहिते द्वादशमध्ययने गाथा २
श्रीसमवसरणाध्ययनम् टीका - अस्य च प्राक्तनाध्ययनेन सहायं संबन्धः, तद्यथा - साधुना प्रतिपन्नभावमार्गेण कुमार्गाश्रिताः परवादिनः सम्यक् परिज्ञाय परिहर्तव्याः, तत्स्वरूपाविष्करणं चानेनाध्ययनेनोपदिश्यते इति, अनन्तरसूत्रस्यानेन सूत्रेण सह संबन्धोऽयं, तद्यथा - संवृतो महाप्रज्ञो 'वीरो दत्तैषणां चरन्नभिनिर्वृतः सन् मृत्युकालमभिकाक्षेद् एतत्केवलिनो भाषितं, तथा परतीर्थिकपरिहारं च कुर्यात् एतच्च केवलिनो मतम्, अतस्तत्परिहारार्थ तत्स्वरूपणनिरूपणमनेन क्रियते। "चत्वारी" ति संख्यापदमपरसंख्यानिवृत्त्यर्थं "समवसरणानि" परतीर्थिकाभ्युपगमसमूहरूपाणि यानि प्रावादुकाः पृथक् पृथग्वदन्ति, तानि चामूनि अन्वर्थाभिधायिभिः संज्ञापदैनिर्दिश्यन्ते, तद्यथा – क्रियाम् - अस्तीत्यादिकां वदितुं शीलं येषां ते क्रियावादिनः, तथाऽक्रियां - नास्तीत्यादिकां वदितुं शीलं येषां तेऽक्रियावादिनः, तथा तृतीया वैनयिकाश्चतुर्थास्त्वज्ञानिका इति ॥१॥
टीकार्थ - इस अध्ययन का ग्यारहवें अध्ययन के साथ सम्बन्ध यह है - ग्यारहवें अध्ययन में कहा है कि - भावमार्ग को प्राप्त किया हुआ साधु कुमार्ग में जानेवाले परतीर्थियों को अच्छी तरह जानकर छोड़ देवे, अतः इस अध्ययन में उन परतीर्थियों का स्वरूप बताया जाता है। पूर्वसूत्र के साथ इस सूत्र का सम्बन्ध यह है - पूर्वसूत्र में कहा है कि -इन्द्रिय और मन को सावध कर्म से निवृत्त रखनेवाला महाबुद्धिमान् वीर साधु दूसरे से दिया हुआ एषणीय आहार आदि लेता हुआ कषायरहित होकर मृत्युकाल की प्रतीक्षा करे, यह केवली का मत है तथा उक्त साधु परतीर्थी का त्याग करे, यह भी केवली का मत है अतः परतीर्थियों की चार संख्या अधिक और कम संख्या की निवृत्ति के लिए कही गयी है (अर्थात् परतीर्थी चार हैं, ज्यादा या कम नहीं हैं, यह जानना चाहिए) परतीर्थी जिन सिद्धान्तों को अलग - अलग मानते हैं, वे सिद्धान्त चार हैं। उन सिद्धान्तों को अर्थानुसार नाम के द्वारा शास्त्रकार बताते हैं - (१) क्रिया अर्थात् पदार्थ हैं, ऐसा कहनेवाले क्रियावादी कहलाते हैं (२) तथा पदार्थ नहीं हैं, ऐसा कहनेवाले अक्रियावादी हैं एवं तीसरे विनयवादी और चौथे अज्ञानवादी हैं ॥१॥
॥२॥
तदेवं क्रियाऽक्रियावैनयिकाज्ञानवादिनः सामान्येन प्रदाधुना तदुषणार्थं तन्मतोपन्यासं पश्चानुपूर्व्यप्यस्तीत्यतः पश्चानुपूर्व्या कर्तुमाह, यदिवैतेषामज्ञानिका एव 'सर्वापलापितयाऽत्यन्तमसंबद्धा अतस्तानेवादावाह -
इस प्रकार क्रियावादी, अक्रियावादी, विनयवादी और अज्ञानवादियों को सामान्य रूप से बताकर अब उनके मत के दोषों को कहने के लिए पीछे के क्रम से शास्त्रकार उनका मत बताते हैं क्योंकि पूर्व क्रम के समान पीछे का क्रम भी होता है। अथवा चार मतवादियों में अज्ञानवादी ही अत्यन्त विपरीतभाषी है क्योंकि वह सब पदार्थो को उड़ाता है, अतः शास्त्रकार पहले अज्ञानवादी का ही सिद्धान्त बतलाते हैं - अण्णाणिया ता कुसलावि संता, असंथुया णो वितिगिच्छतिन्ना । अकोविया आहु अकोवियेहिं, अणाणुवीइत्तु मुसं वयंति छाया - भाज्ञानिकास्ते कुशला अपि सन्तोऽसंस्तुताः नो विचिकित्सातीर्णाः ।
अकोविदा माहुरकोविदेभ्योऽननुविचिन्त्य तु मृषा वदन्ति | अन्वयार्थ - (ता अण्णाणिया) वे अज्ञानवादी (कुसलावि संता) अपने को कुशल मानते हुए भी (णो वितिगिच्छतित्रा) संशय से रहित नहीं हैं (असंथुया) अतः वे मिथ्यावादी हैं। (अकोविया अकोवियेहिं) वे स्वयं अज्ञानी हैं और अज्ञानी शिष्यों को उपदेश करते हैं । (अणाणुवीइत्तु मुसं वयंति) वे विचार न करके मिथ्याभाषण करते हैं।
भावार्थ - अज्ञानवादी अपने को निपुण मानते हुए भी विपरीतभाषी हैं तथा वे भ्रमरहित नहीं किन्तु भ्रम में पड़े हुए हैं। वे स्वयं अज्ञानी हैं और अज्ञानी शिष्यों को उपदेश करते हैं। वे वस्तुतत्त्व का विचार न करके मिथ्या भाषण करते हैं।
टीका - अज्ञानं विद्यते येषामज्ञानेन वा चरन्तीत्यज्ञानिकाः आज्ञानिका वा तावत्प्रदर्श्यन्ते. ते चाज्ञानिकाः किल 1. धीरो प्र०। 2. दूषणार्थ प्र०। 3. व्याख्यानमिति शेषः । 4. असंबद्धभाषिणः ।
५०५