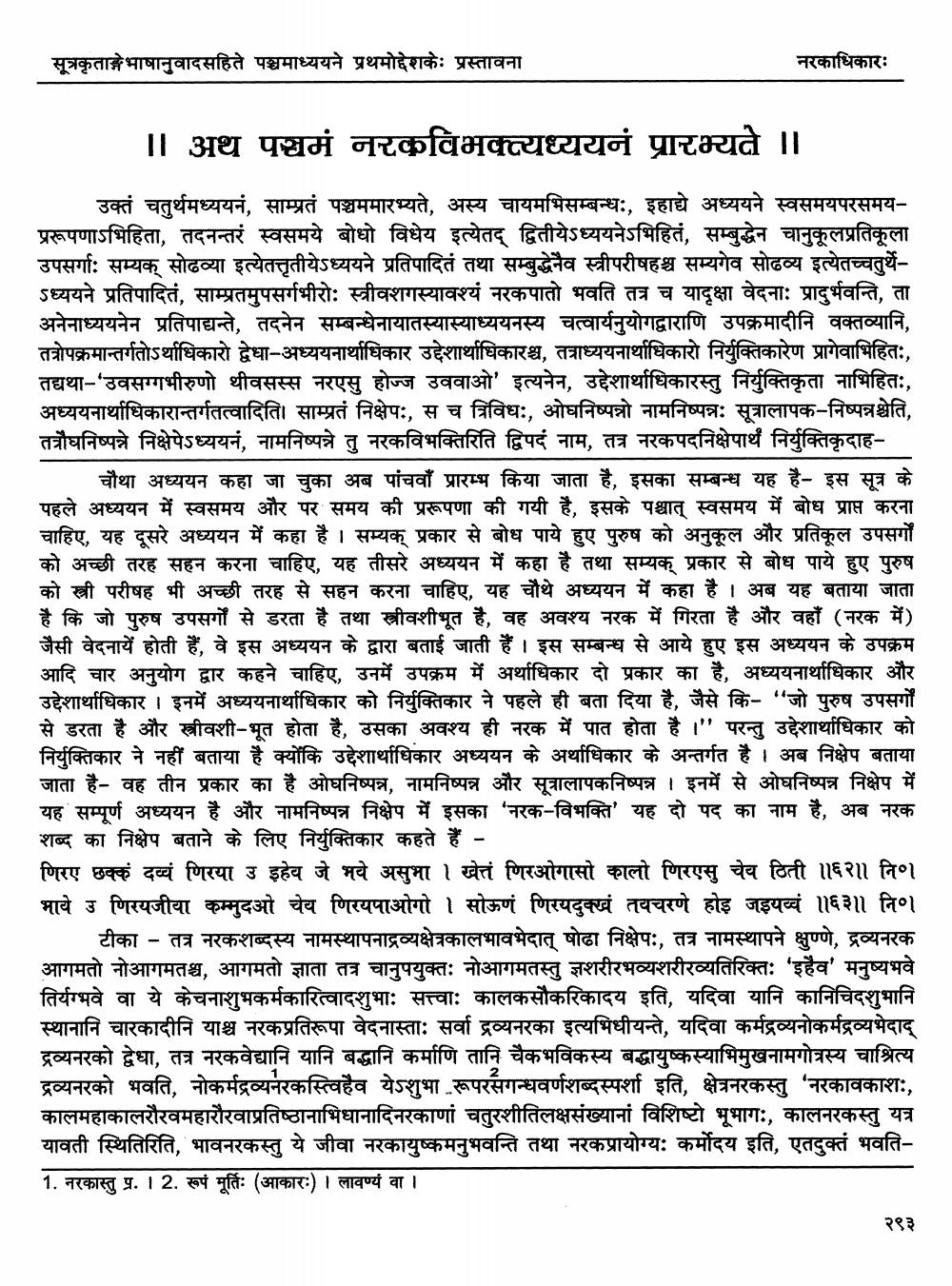________________
सूत्रकृताङ्गेभाषानुवादसहिते पञ्चमाध्ययने प्रथमोद्देशकेः प्रस्तावना
नरकाधिकारः
|| अथ पञ्चमं नरकविभक्त्यध्ययनं प्रारभ्यते ।।
उक्तं चतुर्थमध्ययनं, साम्प्रतं पञ्चममारभ्यते, अस्य चायमभिसम्बन्धः, इहाद्ये अध्ययने स्वसमयपरसमयप्ररूपणाऽभिहिता, तदनन्तरं स्वसमये बोधो विधेय इत्येतद् द्वितीयेऽध्ययनेऽभिहितं, सम्बुद्धेन चानुकूलप्रतिकूला उपसर्गाः सम्यक् सोढव्या इत्येतत्तृतीयेऽध्ययने प्रतिपादितं तथा सम्बुद्धेनैव स्त्रीपरीषहश्च सम्यगेव सोढव्य इत्येतच्चतुर्थेऽध्ययने प्रतिपादितं, साम्प्रतमुपसर्गभीरोः स्त्रीवशगस्यावश्यं नरकपातो भवति तत्र च यादृक्षा वेदनाः प्रादुर्भवन्ति, ता अनेनाध्ययनेन प्रतिपाद्यन्ते, तदनेन सम्बन्धेनायातस्यास्याध्ययनस्य चत्वार्यनुयोगद्वाराणि उपक्रमादीनि वक्तव्यानि, तत्रोपक्रमान्तर्गतोऽर्थाधिकारो द्वेधा-अध्ययनार्थाधिकार उद्देशार्थाधिकारश्च, तत्राध्ययनार्थाधिकारो नियुक्तिकारेण प्रागेवाभिहितः, तद्यथा-'उवसग्गभीरुणो थीवसस्स नरएसु होज्ज उववाओ' इत्यनेन, उद्देशार्थाधिकारस्तु नियुक्तिकृता नाभिहितः, अध्ययनार्थाधिकारान्तर्गतत्वादिति। साम्प्रतं निक्षेपः, स च त्रिविधः, ओघनिष्पन्नो नामनिष्पन्नः सूत्रालापक-निष्पन्नश्चेति, तत्रौघनिष्पन्ने निक्षेपेऽध्ययनं, नामनिष्पन्ने तु नरकविभक्तिरिति द्विपदं नाम, तत्र नरकपदनिक्षेपार्थं नियुक्तिकृदाह
चौथा अध्ययन कहा जा चुका अब पांचवाँ प्रारम्भ किया जाता है, इसका सम्बन्ध यह है- इस सूत्र के पहले अध्ययन में स्वसमय और पर समय की प्ररूपणा की गयी है, इसके पश्चात् स्वसमय में बोध प्राप्त करना चाहिए, यह दूसरे अध्ययन में कहा है । सम्यक् प्रकार से बोध पाये हुए पुरुष को अनुकूल और प्रतिकूल उपसर्गों को अच्छी तरह सहन करना चाहिए, यह तीसरे अध्ययन में कहा है तथा सम्यक् प्रकार से बोध पाये हुए पुरुष को स्त्री परीषह भी अच्छी तरह से सहन करना चाहिए, यह चौथे अध्ययन में कहा है। अब यह बताया जाता है कि जो पुरुष उपसगों से डरता है तथा स्त्रीवशीभूत है, वह अवश्य नरक में गिरता है और वहाँ (नरक में) जैसी वेदनायें होती हैं, वे इस अध्ययन के द्वारा बताई जाती हैं। इस सम्बन्ध से आये हुए इस अध्ययन के उपक्रम आदि चार अनुयोग द्वार कहने चाहिए, उनमें उपक्रम में अधिकार दो प्रकार का है, अध्ययनार्थाधिकार और उद्देशार्थाधिकार । इनमें अध्ययनार्थाधिकार को नियुक्तिकार ने पहले ही बता दिया है, जैसे कि- "जो पुरुष उपसर्गों से डरता है और स्त्रीवशी-भूत होता है, उसका अवश्य ही नरक में पात होता है ।" परन्तु उद्देशार्थाधिकार को नियुक्तिकार ने नहीं बताया है क्योंकि उद्देशार्थाधिकार अध्ययन के अधिकार के अन्तर्गत है । अब निक्षेप बताया जाता है- वह तीन प्रकार का है ओघनिष्पन्न, नामनिष्पन्न और सूत्रालापकनिष्पन्न । इनमें से ओघनिष्पन्न निक्षेप में यह सम्पूर्ण अध्ययन है और नामनिष्पन्न निक्षेप में इसका 'नरक-विभक्ति' यह दो पद का नाम है, अब नरक शब्द का निक्षेप बताने के लिए नियुक्तिकार कहते हैं - णिरए छक्कं दव्यं णिरया उ इहेव जे भवे असुभा । खेतं णिरओगासो कालो णिरएसु चेव ठिती ॥६२॥ नि० भावे उ णिरयजीया कम्मुदओ चेय णिरयपाओगो । सोऊणं णिरयदुक्खं तवचरणे होड़ जइयव्वं ॥६३॥ नि।
टीका - तत्र नरकशब्दस्य नामस्थापनाद्रव्यक्षेत्रकालभावभेदात् षोढा निक्षेपः, तत्र नामस्थापने क्षुण्णे, द्रव्यनरक आगमतो नोआगमतश्च, आगमतो ज्ञाता तत्र चानुपयुक्तः नोआगमतस्तु ज्ञशरीरभव्यशरीरव्यतिरिक्तः ‘इहैव' मनुष्यभवे तियग्भवे वा ये कंचनाशुभकर्मकारित्वादशुभाः सत्त्वाः कालकसौकरिकादय इति, यदिवा यानि कानिचिदशभानि स्थानानि चारकादीनि याश्च नरकप्रतिरूपा वेदनास्ताः सर्वा द्रव्यनरका इत्यभिधीयन्ते, यदिवा कर्मद्रव्यनोकर्मद्रव्यभेदाद द्रव्यनरको द्वेधा, तत्र नरकवेद्यानि यानि बद्धानि कर्माणि तानि चैकभविकस्य बद्धायुष्कस्याभिमुखनामगोत्रस्य चाश्रित्य द्रव्यनरको भवति, नोकर्मद्रव्यनरकस्त्विहैव येऽशुभा .रूपरसंगन्धवर्णशब्दस्पर्शा इति, क्षेत्रनरकस्तु 'नरकावकाशः, कालमहाकालरौरवमहारौरवाप्रतिष्ठानाभिधानादिनरकाणां चतुरशीतिलक्षसंख्यानां विशिष्टो भूभागः, कालनरकस्तु यत्र यावती स्थितिरिति, भावनरकस्तु ये जीवा नरकायुष्कमनुभवन्ति तथा नरकप्रायोग्यः कर्मोदय इति, एतदुक्तं भवति1. नरकास्तु प्र. । 2. रूपं मूर्तिः (आकारः) । लावण्यं वा ।
२९३