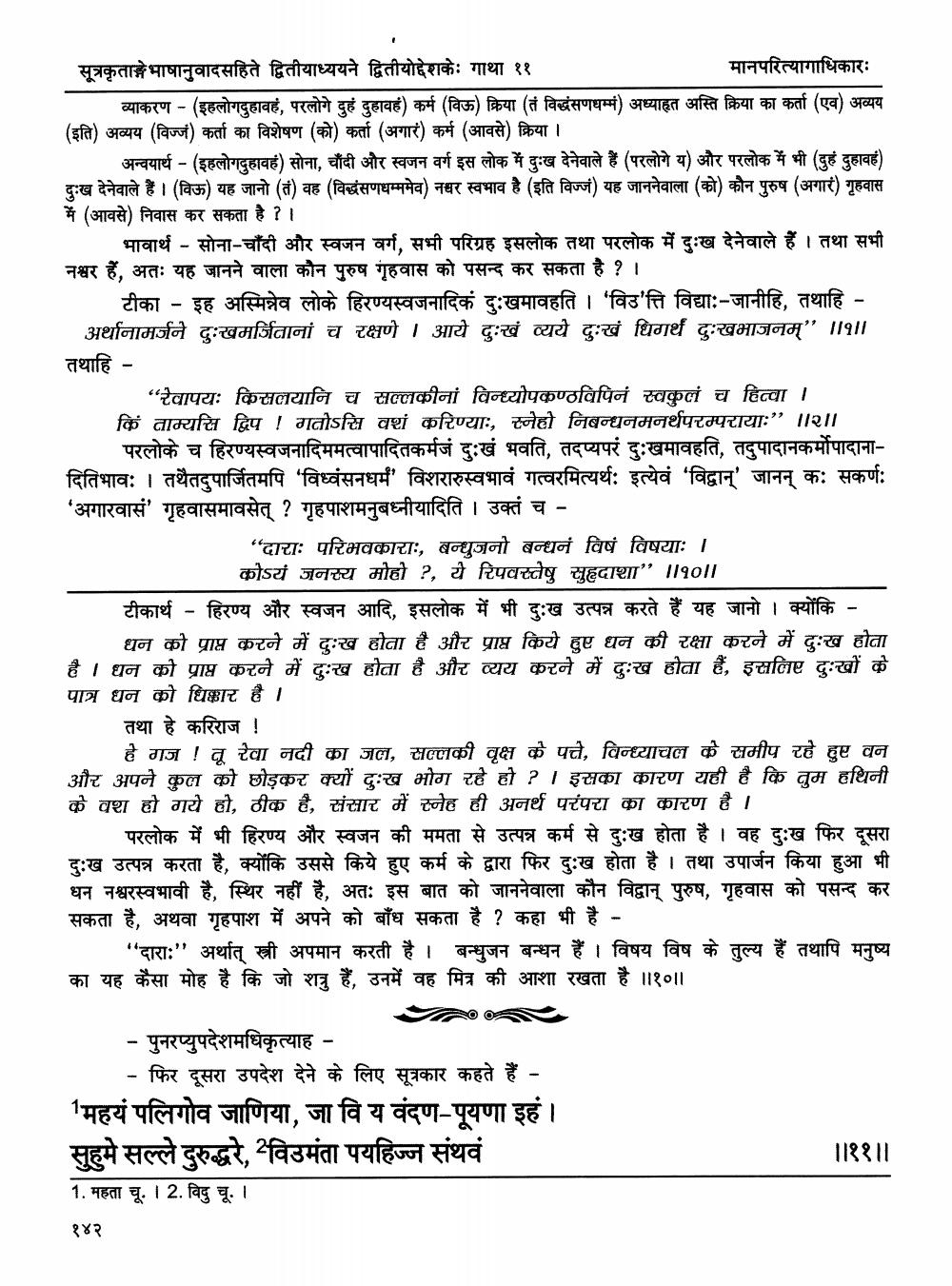________________
सूत्रकृताङ्गेभाषानुवादसहिते द्वितीयाध्ययने द्वितीयोद्देशकेः गाथा ११
मानपरित्यागाधिकारः __व्याकरण - (इहलोगदुहावहं, परलोगे दुहं दुहावह) कर्म (विऊ) क्रिया (तं विद्धंसणधम्म) अध्याहृत अस्ति क्रिया का कर्ता (एव) अव्यय (इति) अव्यय (विज्ज) कर्ता का विशेषण (को) कर्ता (अगारं) कर्म (आवसे) क्रिया ।
____ अन्वयार्थ - (इहलोगदुहावह) सोना, चाँदी और स्वजन वर्ग इस लोक में दुःख देनेवाले हैं (परलोगे य) और परलोक में भी (दुहं दुहावह) दुःख देनेवाले हैं । (विऊ) यह जानो (तं) वह (विद्धंसणधम्ममेव) नधर स्वभाव है (इति विज्ज) यह जाननेवाला (को) कौन पुरुष (अगार) गृहवास में (आवसे) निवास कर सकता है ?।
भावार्थ - सोना-चाँदी और स्वजन वर्ग, सभी परिग्रह इसलोक तथा परलोक में दुःख देनेवाले हैं। तथा सभी नश्वर हैं, अतः यह जानने वाला कौन पुरुष गृहवास को पसन्द कर सकता है ? ।
___टीका - इह अस्मिन्नेव लोके हिरण्यस्वजनादिकं दुःखमावहति । 'विउ'त्ति विद्याः-जानीहि, तथाहि - अर्थानामर्जने दुःखमर्जितानां च रक्षणे । आये दुःखं व्यये दुःखं धिगर्थ दुःखभाजनम्" ||१|| तथाहि -
"रेवापयः किसलयानि च सल्लकीनां विन्ध्योपकण्ठविपिनं स्वकुलं च हित्वा । किं ताम्यसि द्विप । गतोऽसि वशं करिण्याः, स्नेहो निबन्धनमनर्थपरम्परायाः" ||२||
परलोके च हिरण्यस्वजनादिममत्वापादितकर्मजं दुःखं भवति, तदप्यपरं दुःखमावहति, तदुपादानकर्मोपादानादितिभावः । तथैतदुपार्जितमपि 'विध्वंसनधर्म' विशरारुस्वभावं गत्वरमित्यर्थः इत्येवं 'विद्वान्' जानन् कः सकर्णः 'अगारवासं' गृहवासमावसेत् ? गृहपाशमनुबध्नीयादिति । उक्तं च -
"दाराः परिभवकाराः, बन्धुजनो बन्धनं विषं विषयाः ।
कोऽयं जनस्य मोहो ?, ये रिपवस्तेषु सुहृदाशा" ||१०|| टीकार्थ - हिरण्य और स्वजन आदि, इसलोक में भी दुःख उत्पन्न करते हैं यह जानो । क्योंकि -
धन को प्राप्त करने में दुःख होता है और प्राप्त किये हुए धन की रक्षा करने में दुःख होता है । धन को प्राप्त करने में दुःख होता है और व्यय करने में दुःख होता हैं, इसलिए दुःखों के पात्र धन को धिक्कार है।
तथा हे करिराज !
हे गज ! तू रेवा नदी का जल, सल्लकी वृक्ष के पत्ते, विन्ध्याचल के समीप रहे हुए वन और अपने कुल को छोड़कर क्यों दुःख भोग रहे हो ? | इसका कारण यही है कि तुम हथिनी के वश हो गये हो, ठीक है, संसार में स्नेह ही अनर्थ परंपरा का कारण है।
परलोक में भी हिरण्य और स्वजन की ममता से उत्पन्न कर्म से दुःख होता है । वह दुःख फिर दूसरा दुःख उत्पन्न करता है, क्योंकि उससे किये हुए कर्म के द्वारा फिर दुःख होता है । तथा उपार्जन किया हुआ भी धन नश्वरस्वभावी है, स्थिर नहीं है, अतः इस बात को जाननेवाला कौन विद्वान् पुरुष, गृहवास को पसन्द कर सकता है, अथवा गृहपाश में अपने को बाँध सकता है ? कहा भी है -
"दाराः" अर्थात् स्त्री अपमान करती है । बन्धुजन बन्धन हैं । विषय विष के तुल्य हैं तथापि मनुष्य का यह कैसा मोह है कि जो शत्र हैं, उनमें वह मित्र की आशा रखता है ॥१०॥
- पुनरप्युपदेशमधिकृत्याह -
- फिर दूसरा उपदेश देने के लिए सूत्रकार कहते हैं - 'महयं पलिगोव जाणिया, जा वि य वंदण-पूयणा इहं। सुहमे सल्ले दुरुद्धरे, विउमंता पयहिज्ज संथवं 1. महता चू. । 2. विदु चू. । १४२
॥११॥