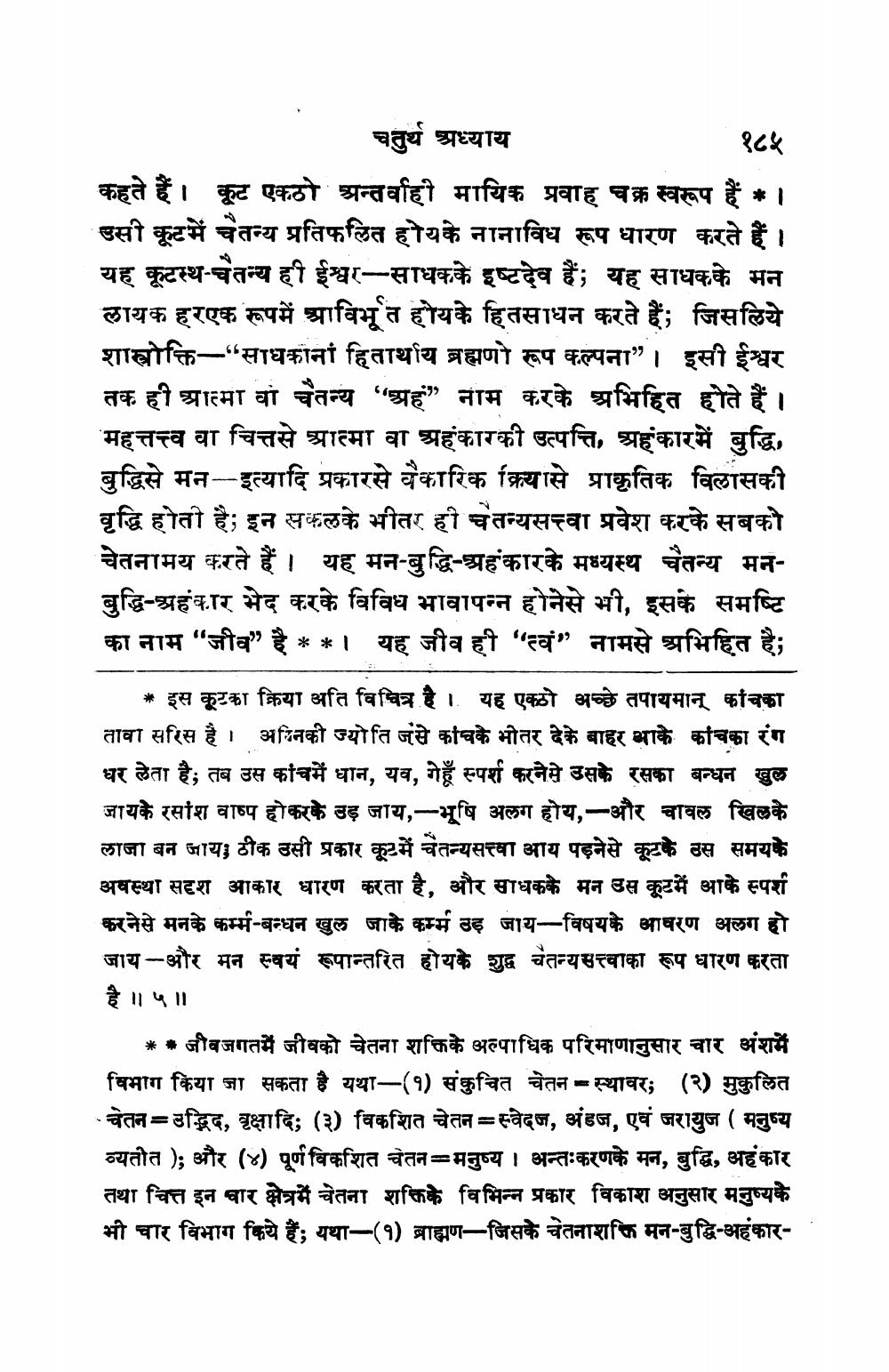________________
चतुर्थ अध्याय
१८५ कहते हैं। कूट एकठो अन्तर्वाही मायिक प्रवाह चक्र स्वरूप हैं * । उसी कूटमें चैतन्य प्रतिफलित होयके नानाविध रूप धारण करते हैं । यह कूटस्थ-चैतन्य ही ईश्वर-साधकके इष्टदेव हैं; यह साधकके मन लायक हरएक रूपमें आविर्भूत होयके हितसाधन करते हैं; जिसलिये शास्त्रोक्ति-“साधकानां हितार्थाय ब्रह्मणो रूप कल्पना"। इसी ईश्वर तक ही आत्मा वा चैतन्य "अहं" नाम करके अभिहित होते हैं । महत्तत्त्व वा चित्तसे आत्मा वा अहंकारकी उत्पत्ति, अहंकारमें बुद्धि, बुद्धिसे मन-इत्यादि प्रकारसे वैकारिक क्रियासे प्राकृतिक विलासकी वृद्धि होती है। इन सकलके भीतर ही चैतन्यसत्त्वा प्रवेश करके सबको चेतनामय करते हैं। यह मन-बुद्धि-अहंकारके मध्यस्थ चैतन्य मनबुद्धि-अहंकार भेद करके विविध भावापन्न होनेसे भी, इसके समष्टि का नाम "जीव" है * *। यह जीव ही "त्वं" नामसे अभिहित है;
* इस कूटका क्रिया अति विचित्र है। यह एकठो अच्छे तपायमान् कांचका तावा सरिस है। अग्निकी ज्योति जसे कांचके भीतर देके बाहर भाके कांचका रंग धर लेता है, तब उस कांचमें धान, यव, गेहूँ स्पर्श करनेसे उसके रसका बन्धन खुल जायके रसांश वाष्प होकरके उड़ जाय,-भूषि अलग होय, और चावल खिलके लाजा बन जाय, ठीक उसी प्रकार कूटमें चैतन्यसत्त्वा आय पड़नेसे कूटके उस समयके अवस्था सदृश आकार धारण करता है, और साधकके मन उस कूटमें आके स्पर्श करनेसे मनके कर्म-बन्धन खुल जाके कर्म उड़ जाय-विषयके आवरण अलग हो जाय-और मन स्वयं रूपान्तरित होयके शुद्ध चैतन्यसत्त्वाका रूप धारण करता
* * जीवजगतमें जीवको चेतना शक्तिके अल्पाधिक परिमाणानुसार चार अंशमें विभाग किया जा सकता है यथा-(१) संकुचित चेतन = स्थावर; (२) मुकुलित
चेतन= उद्भिद, वृक्षादि; (३) विकशित चेतन =स्वेदज, अंडज, एवं जरायुज ( मनुष्य व्यतीत ); और (४) पूर्ण विकशित चेतन-मनुष्य । अन्तःकरणके मन, बुद्धि, अहंकार तथा चित्त इन चार क्षेत्रमें चेतना शक्तिके विभिन्न प्रकार विकाश अनुसार मनुष्यके भी चार विभाग किये हैं; यथा-(१) ब्राह्मण-जिसके चेतनाशक्ति मन-बुद्धि-अहंकार