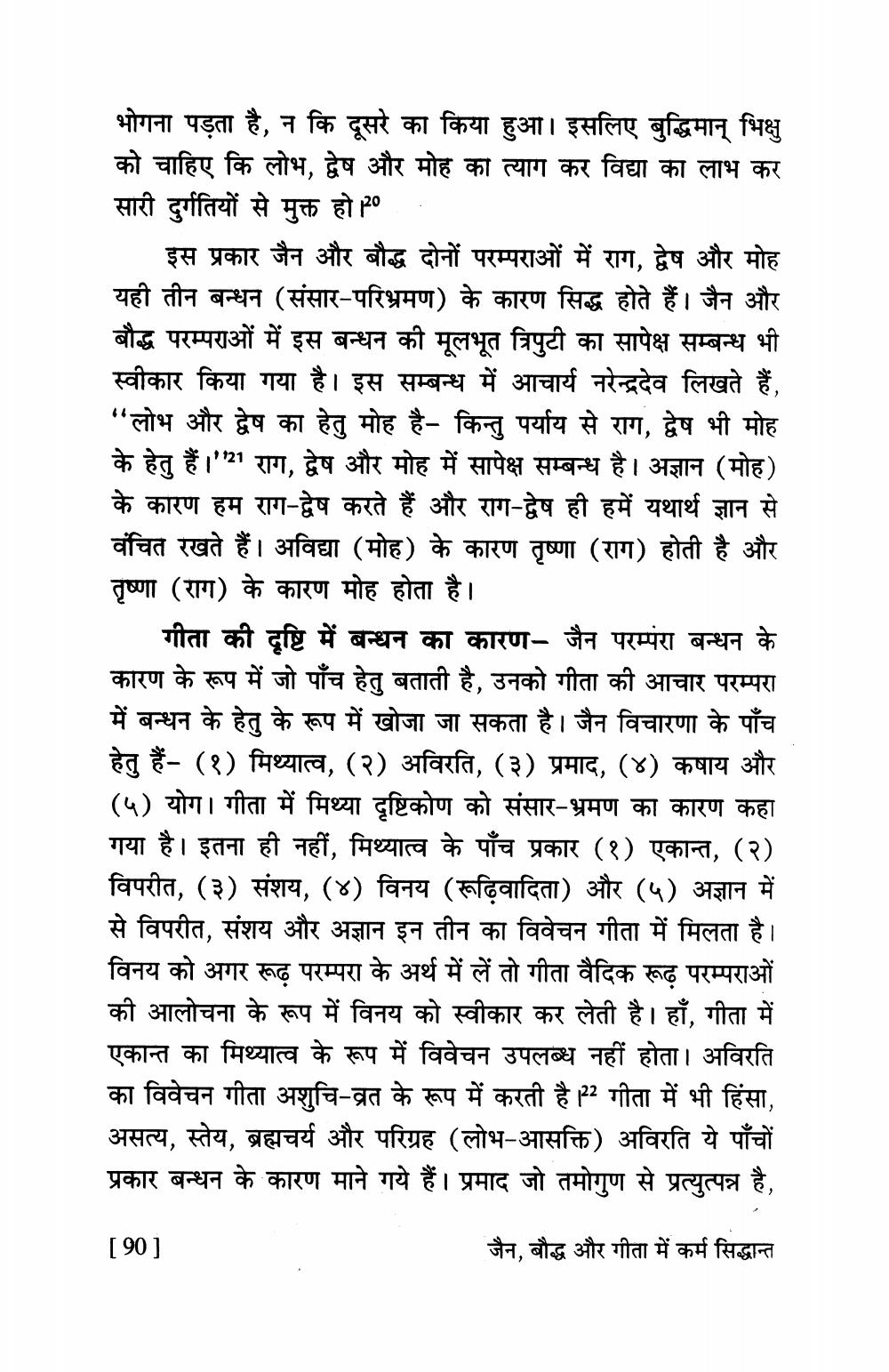________________
भोगना पड़ता है, न कि दूसरे का किया हुआ। इसलिए बुद्धिमान् भिक्षु को चाहिए कि लोभ, द्वेष और मोह का त्याग कर विद्या का लाभ कर सारी दुर्गतियों से मुक्त हो।
इस प्रकार जैन और बौद्ध दोनों परम्पराओं में राग, द्वेष और मोह यही तीन बन्धन (संसार-परिभ्रमण) के कारण सिद्ध होते हैं। जैन और बौद्ध परम्पराओं में इस बन्धन की मूलभूत त्रिपुटी का सापेक्ष सम्बन्ध भी स्वीकार किया गया है। इस सम्बन्ध में आचार्य नरेन्द्रदेव लिखते हैं, "लोभ और द्वेष का हेतु मोह है- किन्तु पर्याय से राग, द्वेष भी मोह के हेतु हैं।''21 राग, द्वेष और मोह में सापेक्ष सम्बन्ध है। अज्ञान (मोह) के कारण हम राग-द्वेष करते हैं और राग-द्वेष ही हमें यथार्थ ज्ञान से वंचित रखते हैं। अविद्या (मोह) के कारण तृष्णा (राग) होती है और तृष्णा (राग) के कारण मोह होता है।
गीता की दृष्टि में बन्धन का कारण- जैन परम्परा बन्धन के कारण के रूप में जो पाँच हेतु बताती है, उनको गीता की आचार परम्परा में बन्धन के हेतु के रूप में खोजा जा सकता है। जैन विचारणा के पाँच हेतु हैं- (१) मिथ्यात्व, (२) अविरति, (३) प्रमाद, (४) कषाय और (५) योग। गीता में मिथ्या दृष्टिकोण को संसार-भ्रमण का कारण कहा गया है। इतना ही नहीं, मिथ्यात्व के पाँच प्रकार (१) एकान्त, (२) विपरीत, (३) संशय, (४) विनय (रूढ़िवादिता) और (५) अज्ञान में से विपरीत, संशय और अज्ञान इन तीन का विवेचन गीता में मिलता है। विनय को अगर रूढ़ परम्परा के अर्थ में लें तो गीता वैदिक रूढ़ परम्पराओं की आलोचना के रूप में विनय को स्वीकार कर लेती है। हाँ, गीता में एकान्त का मिथ्यात्व के रूप में विवेचन उपलब्ध नहीं होता। अविरति का विवेचन गीता अशुचि-व्रत के रूप में करती है। गीता में भी हिंसा, असत्य, स्तेय, ब्रह्मचर्य और परिग्रह (लोभ-आसक्ति) अविरति ये पाँचों प्रकार बन्धन के कारण माने गये हैं। प्रमाद जो तमोगुण से प्रत्युत्पन्न है,
[90]
जैन, बौद्ध और गीता में कर्म सिद्धान्त