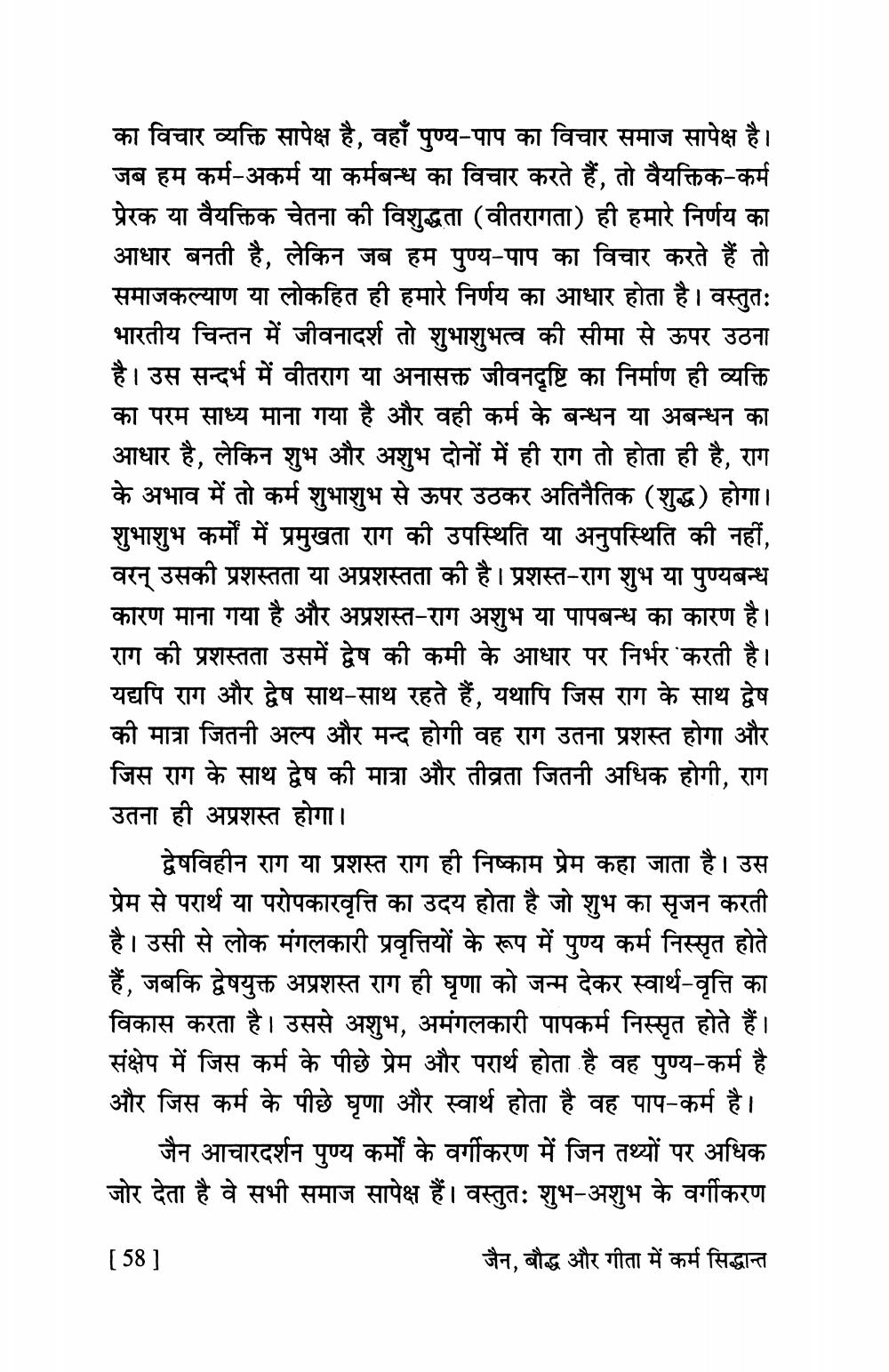________________
का विचार व्यक्ति सापेक्ष है, वहाँ पुण्य-पाप का विचार समाज सापेक्ष है। जब हम कर्म-अकर्म या कर्मबन्ध का विचार करते हैं, तो वैयक्तिक-कर्म प्रेरक या वैयक्तिक चेतना की विशुद्धता (वीतरागता) ही हमारे निर्णय का आधार बनती है, लेकिन जब हम पुण्य-पाप का विचार करते हैं तो समाजकल्याण या लोकहित ही हमारे निर्णय का आधार होता है। वस्तुतः भारतीय चिन्तन में जीवनादर्श तो शुभाशुभत्व की सीमा से ऊपर उठना है। उस सन्दर्भ में वीतराग या अनासक्त जीवनदृष्टि का निर्माण ही व्यक्ति का परम साध्य माना गया है और वही कर्म के बन्धन या अबन्धन का आधार है, लेकिन शुभ और अशुभ दोनों में ही राग तो होता ही है, राग के अभाव में तो कर्म शुभाशुभ से ऊपर उठकर अतिनैतिक (शुद्ध) होगा। शुभाशुभ कर्मों में प्रमुखता राग की उपस्थिति या अनुपस्थिति की नहीं, वरन् उसकी प्रशस्तता या अप्रशस्तता की है। प्रशस्त-राग शुभ या पुण्यबन्ध कारण माना गया है और अप्रशस्त-राग अशुभ या पापबन्ध का कारण है। राग की प्रशस्तता उसमें द्वेष की कमी के आधार पर निर्भर करती है। यद्यपि राग और द्वेष साथ-साथ रहते हैं, यथापि जिस राग के साथ द्वेष की मात्रा जितनी अल्प और मन्द होगी वह राग उतना प्रशस्त होगा और जिस राग के साथ द्वेष की मात्रा और तीव्रता जितनी अधिक होगी, राग उतना ही अप्रशस्त होगा।
द्वेषविहीन राग या प्रशस्त राग ही निष्काम प्रेम कहा जाता है। उस प्रेम से परार्थ या परोपकारवृत्ति का उदय होता है जो शुभ का सृजन करती है। उसी से लोक मंगलकारी प्रवृत्तियों के रूप में पुण्य कर्म निस्सृत होते हैं, जबकि द्वेषयुक्त अप्रशस्त राग ही घृणा को जन्म देकर स्वार्थ-वृत्ति का विकास करता है। उससे अशुभ, अमंगलकारी पापकर्म निस्सृत होते हैं। संक्षेप में जिस कर्म के पीछे प्रेम और परार्थ होता है वह पुण्य-कर्म है और जिस कर्म के पीछे घृणा और स्वार्थ होता है वह पाप-कर्म है।
जैन आचारदर्शन पुण्य कर्मों के वर्गीकरण में जिन तथ्यों पर अधिक जोर देता है वे सभी समाज सापेक्ष हैं। वस्तुतः शुभ-अशुभ के वर्गीकरण
[58]
जैन, बौद्ध और गीता में कर्म सिद्धान्त