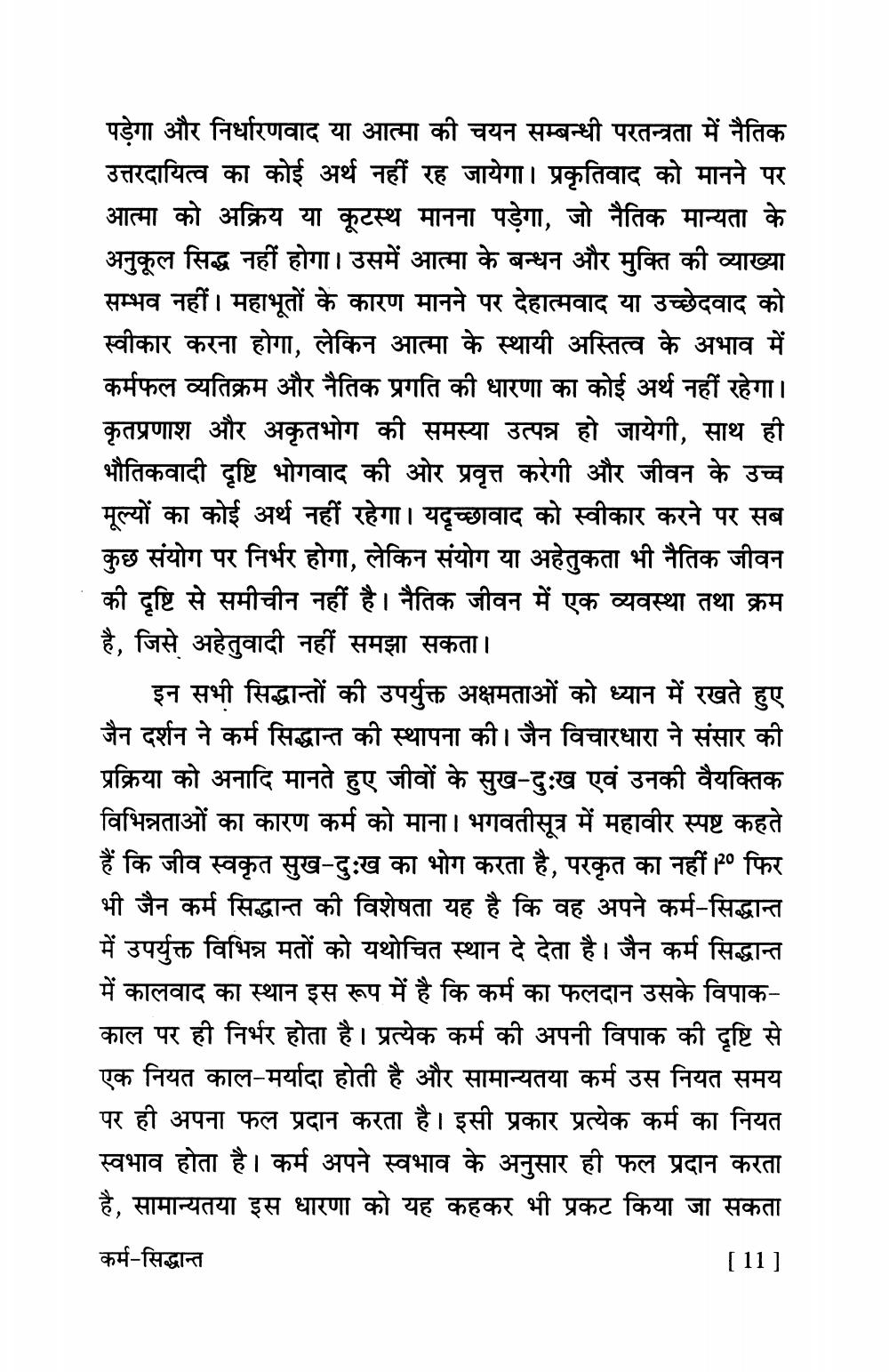________________
पड़ेगा और निर्धारणवाद या आत्मा की चयन सम्बन्धी परतन्त्रता में नैतिक उत्तरदायित्व का कोई अर्थ नहीं रह जायेगा । प्रकृतिवाद को मानने पर आत्मा को अक्रिय या कूटस्थ मानना पड़ेगा, जो नैतिक मान्यता के अनुकूल सिद्ध नहीं होगा । उसमें आत्मा के बन्धन और मुक्ति की व्याख्या सम्भव नहीं । महाभूतों के कारण मानने पर देहात्मवाद या उच्छेदवाद को स्वीकार करना होगा, लेकिन आत्मा के स्थायी अस्तित्व के अभाव में कर्मफल व्यतिक्रम और नैतिक प्रगति की धारणा का कोई अर्थ नहीं रहेगा। कृतप्रणाश और अकृतभोग की समस्या उत्पन्न हो जायेगी, साथ ही भौतिकवादी दृष्टि भोगवाद की ओर प्रवृत्त करेगी और जीवन के उच्च मूल्यों का कोई अर्थ नहीं रहेगा । यदृच्छावाद को स्वीकार करने पर सब कुछ संयोग पर निर्भर होगा, लेकिन संयोग या अहेतुकता भी नैतिक जीवन की दृष्टि से समीचीन नहीं है। नैतिक जीवन में एक व्यवस्था तथा क्रम है, जिसे अहेतुवादी नहीं समझा सकता ।
इन सभी सिद्धान्तों की उपर्युक्त अक्षमताओं को ध्यान में रखते हुए जैन दर्शन ने कर्म सिद्धान्त की स्थापना की। जैन विचारधारा ने संसार की प्रक्रिया को अनादि मानते हुए जीवों के सुख-दुःख एवं उनकी वैयक्तिक विभिन्नताओं का कारण कर्म को माना । भगवतीसूत्र में महावीर स्पष्ट कहते हैं कि जीव स्वकृत सुख - दुःख का भोग करता है, परकृत का नहीं 120 फिर भी जैन कर्म सिद्धान्त की विशेषता यह है कि वह अपने कर्म - सिद्धान्त में उपर्युक्त विभिन्न मतों को यथोचित स्थान दे देता है। जैन कर्म सिद्धान्त में कालवाद का स्थान इस रूप में है कि कर्म का फलदान उसके विपाककाल पर ही निर्भर होता है । प्रत्येक कर्म की अपनी विपाक की दृष्टि से एक नियत काल-मर्यादा होती है और सामान्यतया कर्म उस नियत समय पर ही अपना फल प्रदान करता है । इसी प्रकार प्रत्येक कर्म का नियत स्वभाव होता है। कर्म अपने स्वभाव के अनुसार ही फल प्रदान करता है, सामान्यतया इस धारणा को यह कहकर भी प्रकट किया जा सकता कर्म-सिद्धान्त
[11]