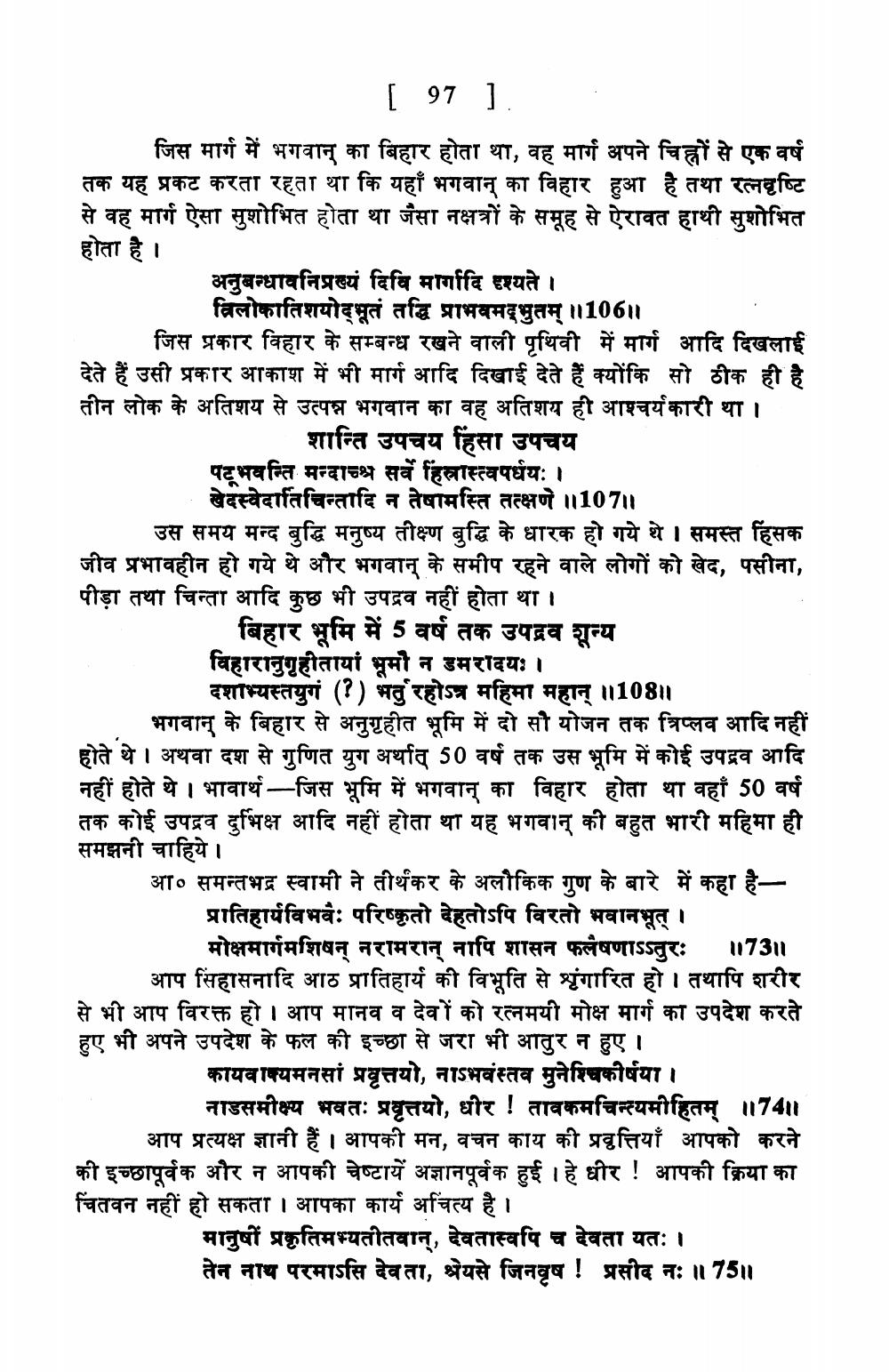________________
[
97 ].
जिस मार्ग में भगवान् का बिहार होता था, वह मार्ग अपने चिह्नों से एक वर्ष तक यह प्रकट करता रहता था कि यहाँ भगवान् का विहार हुआ है तथा रत्नवृष्टि से वह मार्ग ऐसा सुशोभित होता था जैसा नक्षत्रों के समूह से ऐरावत हाथी सुशोभित होता है।
अनुबन्धावनिप्रख्यं दिवि मार्गादि दृश्यते ।
त्रिलोकातिशयोद्भूतं तद्धि प्राभवमद्भुतम् ॥106॥ __ जिस प्रकार विहार के सम्बन्ध रखने वाली पृथिवी में मार्ग आदि दिखलाई देते हैं उसी प्रकार आकाश में भी मार्ग आदि दिखाई देते हैं क्योंकि सो ठीक ही है तीन लोक के अतिशय से उत्पन्न भगवान का वह अतिशय ही आश्चर्यकारी था।
शान्ति उपचय हिंसा उपचय पटूभवन्ति मन्दाच्श्र सर्वे हिंस्त्रास्त्वपर्धयः ।
खेदस्वेदातिचिन्तादि न तेषामस्ति तत्क्षणे ॥107॥ उस समय मन्द बुद्धि मनुष्य तीक्ष्ण बुद्धि के धारक हो गये थे । समस्त हिंसक जीव प्रभावहीन हो गये थे और भगवान् के समीप रहने वाले लोगों को खेद, पसीना, पीड़ा तथा चिन्ता आदि कुछ भी उपद्रव नहीं होता था।
बिहार भूमि में 5 वर्ष तक उपद्रव शून्य विहारानुगृहीतायां भूमौ न उमरादयः।
दशाभ्यस्तयुगं (?) भर्तुरहोऽत्र महिमा महान् ॥108॥ भगवान् के बिहार से अनुगृहीत भूमि में दो सौ योजन तक विप्लव आदि नहीं होते थे। अथवा दश से गुणित युग अर्थात् 50 वर्ष तक उस भूमि में कोई उपद्रव आदि नहीं होते थे। भावार्थ-जिस भूमि में भगवान् का विहार होता था वहाँ 50 वर्ष तक कोई उपद्रव दुर्भिक्ष आदि नहीं होता था यह भगवान् की बहुत भारी महिमा ही समझनी चाहिये। आ० समन्तभद्र स्वामी ने तीर्थंकर के अलौकिक गुण के बारे में कहा है
प्रातिहार्यविभवः परिष्कृतो देहतोऽपि विरतो भवानभूत् ।
मोक्षमार्गमशिषन् नरामरान् नापि शासन फलेषणाऽऽतुरः ॥73॥ आप सिंहासनादि आठ प्रातिहार्य की विभूति से शृंगारित हो । तथापि शरीर से भी आप विरक्त हो । आप मानव व देवों को रत्नमयी मोक्ष मार्ग का उपदेश करते हुए भी अपने उपदेश के फल की इच्छा से जरा भी आतुर न हुए।
कायवाक्यमनसां प्रवृत्तयो, नाऽभवंस्तव मुनेश्चिकीर्षया।
नाडसमीक्ष्य भवतः प्रवृत्तयो, धीर ! तावकमचिन्त्यमीहितम् ॥74॥ आप प्रत्यक्ष ज्ञानी हैं । आपकी मन, वचन काय की प्रवृत्तियाँ आपको करने की इच्छापूर्वक और न आपकी चेष्टायें अज्ञानपूर्वक हुई । हे धीर ! आपकी क्रिया का चितवन नहीं हो सकता। आपका कार्य अचित्य है।
मानुषी प्रकृतिमभ्यतीतवान्, देवतास्वपि च देवता यतः ।। तेन नाथ परमाऽसि देवता, श्रेयसे जिनवृष ! प्रसीद नः ॥15॥