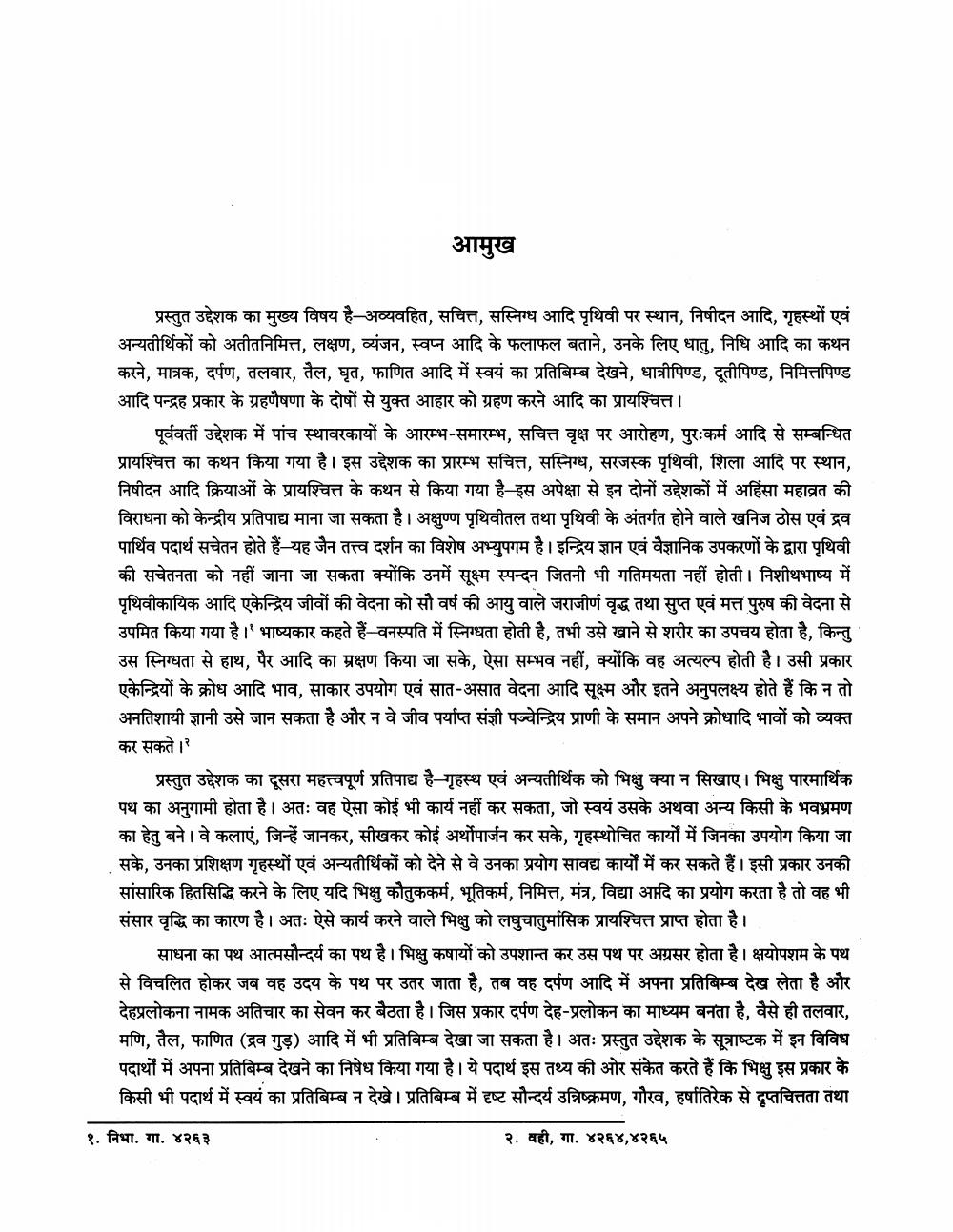________________
आमुख
प्रस्तुत उद्देशक का मुख्य विषय है- अव्यवहित, सचित्त, सस्निग्ध आदि पृथिवी पर स्थान, निषीदन आदि, गृहस्थों एवं अन्यतीर्थिकों को अतीतनिमित्त, लक्षण, व्यंजन, स्वप्न आदि के फलाफल बताने, उनके लिए धातु, निधि आदि का कथन करने, मात्रक, दर्पण, तलवार, तेल, घृत, फाणित आदि में स्वयं का प्रतिविम्ब देखने, धात्रीपिण्ड, दूतीपिण्ड, निमित्तपिण्ड आदि पन्द्रह प्रकार के ग्रहणैषणा के दोषों से युक्त आहार को ग्रहण करने आदि का प्रायश्चित्त ।
पूर्ववर्ती उद्देशक में पांच स्थावरकायों के आरम्भ समारम्भ, सचित्त वृक्ष पर आरोहण, पुरः कर्म आदि से सम्बन्धित प्रायश्चित्त का कथन किया गया है। इस उद्देशक का प्रारम्भ सचित्त, सस्निग्ध, सरजस्क पृथिवी, शिला आदि पर स्थान, निषीदन आदि क्रियाओं के प्रायश्चित्त के कथन से किया गया है - इस अपेक्षा से इन दोनों उद्देशकों में अहिंसा महाव्रत की विराधना को केन्द्रीय प्रतिपाद्य माना जा सकता है। अक्षुण्ण पृथिवीतल तथा पृथिवी के अंतर्गत होने वाले खनिज ठोस एवं द्रव पार्थिव पदार्थ सचेतन होते हैं- यह जैन तत्त्व दर्शन का विशेष अभ्युपगम है। इन्द्रिय ज्ञान एवं वैज्ञानिक उपकरणों के द्वारा पृथिवी की सचेतनता को नहीं जाना जा सकता क्योंकि उनमें सूक्ष्म स्पन्दन जितनी भी गतिमयता नहीं होती । निशीथभाष्य में पृथिवीकायिक आदि एकेन्द्रिय जीवों की वेदना को सौ वर्ष की आयु वाले जराजीर्ण वृद्ध तथा सुप्त एवं मत्त पुरुष की वेदना से उपमित किया गया है।' भाष्यकार कहते हैं - वनस्पति में स्निग्धता होती है, तभी उसे खाने से शरीर का उपचय होता है, किन्तु उस स्निग्धता से हाथ, पैर आदि का प्रक्षण किया जा सके, ऐसा सम्भव नहीं, क्योंकि वह अत्यल्प होती है उसी प्रकार एकेन्द्रियों के क्रोध आदि भाव, साकार उपयोग एवं सात असात वेदना आदि सूक्ष्म और इतने अनुपलक्ष्य होते हैं कि न तो अनतिशायी ज्ञानी उसे जान सकता है और न वे जीव पर्याप्त संशी पञ्चेन्द्रिय प्राणी के समान अपने क्रोधादि भावों को व्यक्त कर सकते ।
T
प्रस्तुत उद्देशक का दूसरा महत्त्वपूर्ण प्रतिपाद्य है- गृहस्थ एवं अन्यतीर्थिक को भिक्षु क्या न सिखाए। भिक्षु पारमार्थिक पथ का अनुगामी होता है । अतः वह ऐसा कोई भी कार्य नहीं कर सकता, जो स्वयं उसके अथवा अन्य किसी के भवभ्रमण का हेतु बने । वे कलाएं, जिन्हें जानकर, सीखकर कोई अर्थोपार्जन कर सके, गृहस्थोचित कार्यों में जिनका उपयोग किया जा सके, उनका प्रशिक्षण गृहस्थों एवं अन्यतीर्थिकों को देने से वे उनका प्रयोग सावद्य कार्यों में कर सकते हैं। इसी प्रकार उनकी सांसारिक हितसिद्धि करने के लिए यदि भिक्षु कौतुककर्म, भूतिकर्म, निमित्त, मंत्र, विद्या आदि का प्रयोग करता है तो वह भी संसार वृद्धि का कारण है अतः ऐसे कार्य करने वाले भिक्षु को लघुचातुर्मासिक प्रायश्चित्त प्राप्त होता है।
साधना का पथ आत्मसौन्दर्य का पथ है। भिक्षु कषायों को उपशान्त कर उस पथ पर अग्रसर होता है। क्षयोपशम के पथ से विचलित होकर जब वह उदय के पथ पर उतर जाता है, तब वह दर्पण आदि में अपना प्रतिबिम्ब देख लेता है और देहप्रलोकना नामक अतिचार का सेवन कर बैठता है। जिस प्रकार दर्पण देह प्रलोकन का माध्यम बनता है, वैसे ही तलवार, मणि, तैल, फाणित (द्रव गुड़) आदि में भी प्रतिबिम्ब देखा जा सकता है। अतः प्रस्तुत उद्देशक के सूत्राष्टक में इन विविध पदार्थों में अपना प्रतिबिम्ब देखने का निषेध किया गया है। ये पदार्थ इस तथ्य की ओर संकेत करते हैं कि भिक्षु इस प्रकार के किसी भी पदार्थ में स्वयं का प्रतिबिम्ब न देखे । प्रतिबिम्ब में दृष्ट सौन्दर्य उन्निष्क्रमण, गौरव, हर्षातिरेक से दृप्तचित्तता तथा १. निभा. गा. ४२६३
२. वही, गा. ४२६४, ४२६५