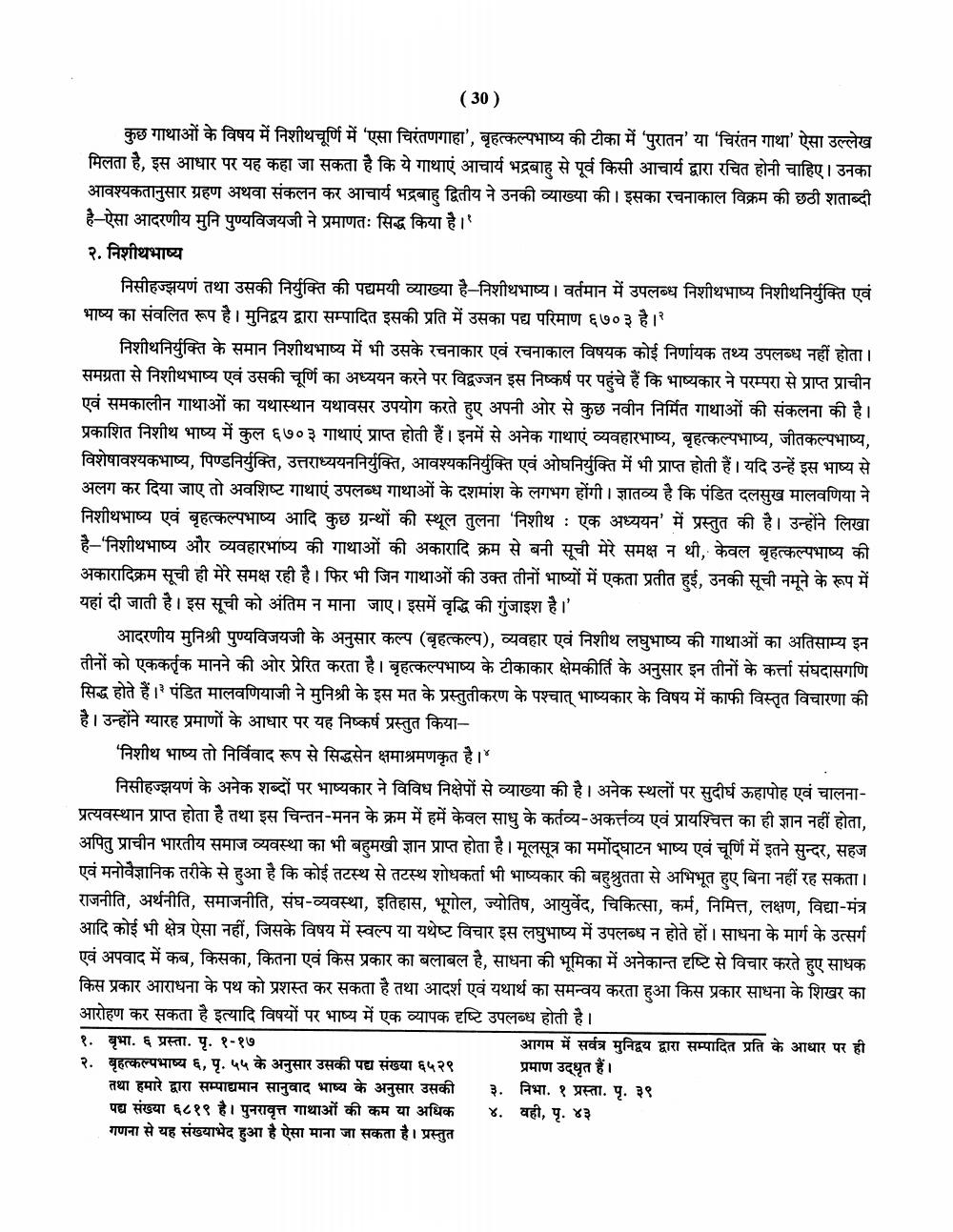________________
(30)
कुछ गाथाओं के विषय में निशीथचूर्णि में 'एसा चिरंतणगाहा', बृहत्कल्पभाष्य की टीका में 'पुरातन' या 'चिरंतन गाथा' ऐसा उल्लेख मिलता है, इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि ये गाथाएं आचार्य भद्रबाहु से पूर्व किसी आचार्य द्वारा रचित होनी चाहिए। उनका आवश्यकतानुसार ग्रहण अथवा संकलन कर आचार्य भद्रबाहु द्वितीय ने उनकी व्याख्या की। इसका रचनाकाल विक्रम की छठी शताब्दी है-ऐसा आदरणीय मुनि पुण्यविजयजी ने प्रमाणतः सिद्ध किया है।' २. निशीथभाष्य
निसीहज्झयणं तथा उसकी नियुक्ति की पद्यमयी व्याख्या है-निशीथभाष्य । वर्तमान में उपलब्ध निशीथभाष्य निशीथनियुक्ति एवं भाष्य का संवलित रूप है। मुनिद्वय द्वारा सम्पादित इसकी प्रति में उसका पद्य परिमाण ६७०३ है।२
निशीथनियुक्ति के समान निशीथभाष्य में भी उसके रचनाकार एवं रचनाकाल विषयक कोई निर्णायक तथ्य उपलब्ध नहीं होता। समग्रता से निशीथभाष्य एवं उसकी चूर्णि का अध्ययन करने पर विद्वज्जन इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि भाष्यकार ने परम्परा से प्राप्त प्राचीन एवं समकालीन गाथाओं का यथास्थान यथावसर उपयोग करते हुए अपनी ओर से कुछ नवीन निर्मित गाथाओं की संकलना की है। प्रकाशित निशीथ भाष्य में कुल ६७०३ गाथाएं प्राप्त होती हैं। इनमें से अनेक गाथाएं व्यवहारभाष्य, बृहत्कल्पभाष्य, जीतकल्पभाष्य,
शेषावश्यकभाष्य, पिण्डनियुक्ति, उत्तराध्ययननियुक्ति, आवश्यकनियुक्ति एवं ओघनियुक्ति में भी प्राप्त होती हैं। यदि उन्हें इस भाष्य से अलग कर दिया जाए तो अवशिष्ट गाथाएं उपलब्ध गाथाओं के दशमांश के लगभग होंगी। ज्ञातव्य है कि पंडित दलसुख मालवणिया ने निशीथभाष्य एवं बृहत्कल्पभाष्य आदि कुछ ग्रन्थों की स्थूल तुलना 'निशीथ : एक अध्ययन' में प्रस्तुत की है। उन्होंने लिखा है-'निशीथभाष्य और व्यवहारभाष्य की गाथाओं की अकारादि क्रम से बनी सूची मेरे समक्ष न थी, केवल बृहत्कल्पभाष्य की अकारादिक्रम सूची ही मेरे समक्ष रही है। फिर भी जिन गाथाओं की उक्त तीनों भाष्यों में एकता प्रतीत हुई, उनकी सूची नमूने के रूप में यहां दी जाती है। इस सूची को अंतिम न माना जाए। इसमें वृद्धि की गुंजाइश है।'
आदरणीय मुनिश्री पुण्यविजयजी के अनुसार कल्प (बृहत्कल्प), व्यवहार एवं निशीथ लघुभाष्य की गाथाओं का अतिसाम्य इन तीनों को एककर्तृक मानने की ओर प्रेरित करता है। बृहत्कल्पभाष्य के टीकाकार क्षेमकीर्ति के अनुसार इन तीनों के कर्ता संघदासगणि सिद्ध होते हैं। पंडित मालवणियाजी ने मुनिश्री के इस मत के प्रस्तुतीकरण के पश्चात् भाष्यकार के विषय में काफी विस्तृत विचारणा की है। उन्होंने ग्यारह प्रमाणों के आधार पर यह निष्कर्ष प्रस्तुत किया
'निशीथ भाष्य तो निर्विवाद रूप से सिद्धसेन क्षमाश्रमणकृत है।'
निसीहज्झयणं के अनेक शब्दों पर भाष्यकार ने विविध निक्षेपों से व्याख्या की है। अनेक स्थलों पर सुदीर्घ ऊहापोह एवं चालनाप्रत्यवस्थान प्राप्त होता है तथा इस चिन्तन-मनन के क्रम में हमें केवल साधु के कर्तव्य-अकर्त्तव्य एवं प्रायश्चित्त का ही ज्ञान नहीं होता, अपितु प्राचीन भारतीय समाज व्यवस्था का भी बहुमखी ज्ञान प्राप्त होता है । मूलसूत्र का मर्मोद्घाटन भाष्य एवं चूर्णि में इतने सुन्दर, सहज एवं मनोवैज्ञानिक तरीके से हुआ है कि कोई तटस्थ से तटस्थ शोधकर्ता भी भाष्यकार की बहुश्रुतता से अभिभूत हुए बिना नहीं रह सकता। राजनीति, अर्थनीति, समाजनीति, संघ-व्यवस्था, इतिहास, भूगोल, ज्योतिष, आयुर्वेद, चिकित्सा, कर्म, निमित्त, लक्षण, विद्या-मंत्र आदि कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं, जिसके विषय में स्वल्प या यथेष्ट विचार इस लघुभाष्य में उपलब्ध न होते हों। साधना के मार्ग के उत्सर्ग एवं अपवाद में कब, किसका, कितना एवं किस प्रकार का बलाबल है, साधना की भूमिका में अनेकान्त दृष्टि से विचार करते हुए साधक किस प्रकार आराधना के पथ को प्रशस्त कर सकता है तथा आदर्श एवं यथार्थ का समन्वय करता हुआ किस प्रकार साधना के शिखर का आरोहण कर सकता है इत्यादि विषयों पर भाष्य में एक व्यापक दृष्टि उपलब्ध होती है। १. बृभा. ६ प्रस्ता. पृ. १-१७
आगम में सर्वत्र मुनिद्वय द्वारा सम्पादित प्रति के आधार पर ही २. बृहत्कल्पभाष्य ६, पृ. ५५ के अनुसार उसकी पद्य संख्या ६५२९ प्रमाण उद्धृत हैं।
तथा हमारे द्वारा सम्पाद्यमान सानुवाद भाष्य के अनुसार उसकी ३. निभा. १ प्रस्ता. पृ. ३९ पद्य संख्या ६८१९ है। पुनरावृत्त गाथाओं की कम या अधिक ४. वही, पृ. ४३ गणना से यह संख्याभेद हुआ है ऐसा माना जा सकता है। प्रस्तुत