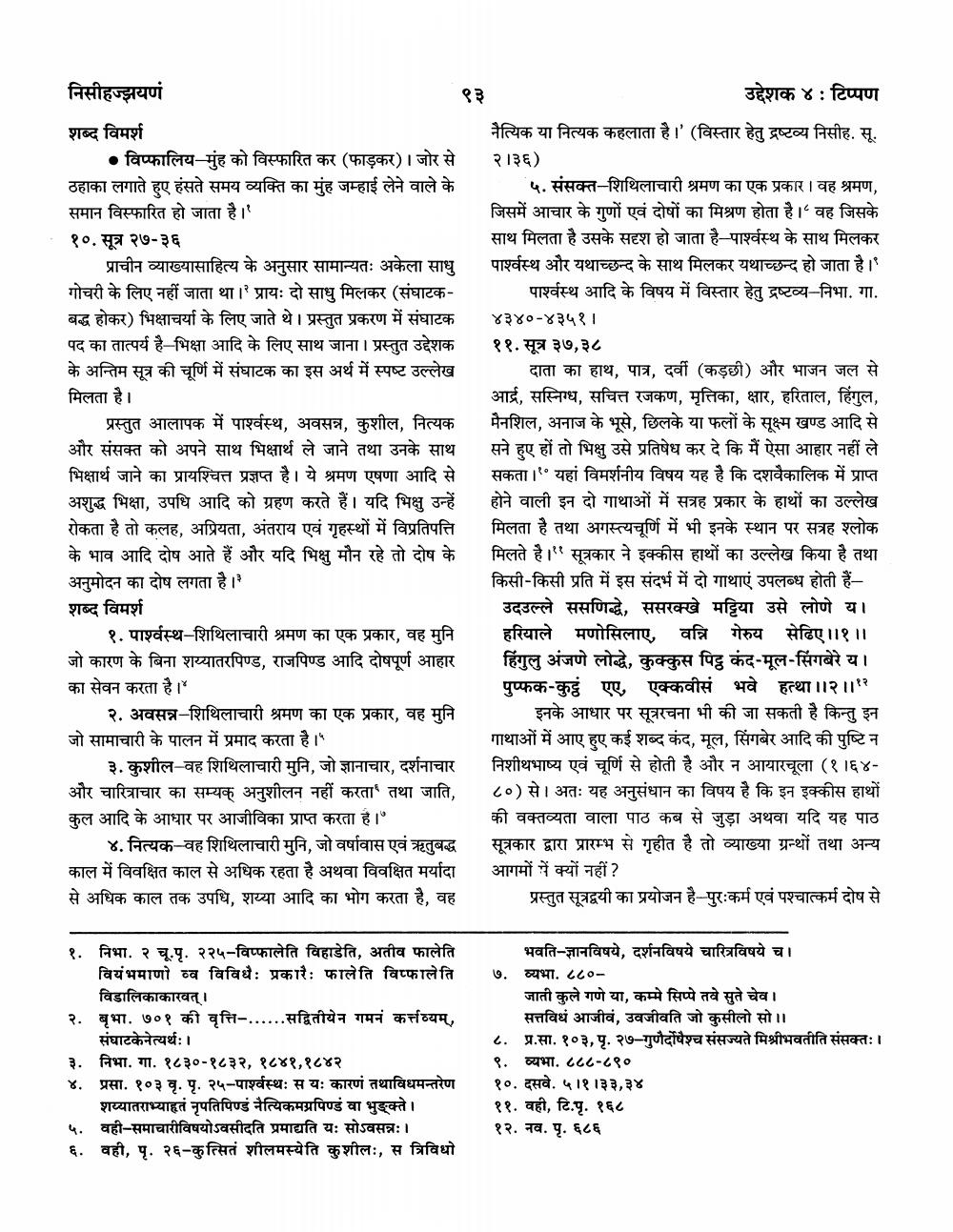________________
निसीहज्झयणं
शब्द विमर्श
•विप्फालिय-मुंह को विस्फारित कर (फाड़कर)। जोर से ठहाका लगाते हुए हंसते समय व्यक्ति का मुंह जम्हाई लेने वाले के समान विस्फारित हो जाता है। १०. सूत्र २७-३६
प्राचीन व्याख्यासाहित्य के अनुसार सामान्यतः अकेला साधु गोचरी के लिए नहीं जाता था। प्रायः दो साधु मिलकर (संघाटकबद्ध होकर) भिक्षाचर्या के लिए जाते थे। प्रस्तुत प्रकरण में संघाटक पद का तात्पर्य है-भिक्षा आदि के लिए साथ जाना। प्रस्तुत उद्देशक के अन्तिम सूत्र की चूर्णि में संघाटक का इस अर्थ में स्पष्ट उल्लेख मिलता है।
प्रस्तुत आलापक में पार्श्वस्थ, अवसन्न, कुशील, नित्यक और संसक्त को अपने साथ भिक्षार्थ ले जाने तथा उनके साथ भिक्षार्थ जाने का प्रायश्चित्त प्रज्ञप्त है। ये श्रमण एषणा आदि से अशुद्ध भिक्षा, उपधि आदि को ग्रहण करते हैं। यदि भिक्षु उन्हें रोकता है तो कलह, अप्रियता, अंतराय एवं गृहस्थों में विप्रतिपत्ति के भाव आदि दोष आते हैं और यदि भिक्षु मौन रहे तो दोष के अनुमोदन का दोष लगता है। शब्द विमर्श
१. पार्श्वस्थ-शिथिलाचारी श्रमण का एक प्रकार, वह मुनि जो कारण के बिना शय्यातरपिण्ड, राजपिण्ड आदि दोषपूर्ण आहार का सेवन करता है।
२. अवसन्न-शिथिलाचारी श्रमण का एक प्रकार, वह मुनि जो सामाचारी के पालन में प्रमाद करता है।
३. कुशील-वह शिथिलाचारी मुनि, जो ज्ञानाचार, दर्शनाचार । और चारित्राचार का सम्यक् अनुशीलन नहीं करता तथा जाति, कुल आदि के आधार पर आजीविका प्राप्त करता है।
४.नित्यक-वह शिथिलाचारी मुनि, जो वर्षावास एवं ऋतुबद्ध काल में विवक्षित काल से अधिक रहता है अथवा विवक्षित मर्यादा से अधिक काल तक उपधि, शय्या आदि का भोग करता है, वह
उद्देशक ४ : टिप्पण नैत्यिक या नित्यक कहलाता है।' (विस्तार हेतु द्रष्टव्य निसीह. सू. २।३६)
५.संसक्त-शिथिलाचारी श्रमण का एक प्रकार । वह श्रमण, जिसमें आचार के गुणों एवं दोषों का मिश्रण होता है। वह जिसके साथ मिलता है उसके सदृश हो जाता है-पार्श्वस्थ के साथ मिलकर पार्श्वस्थ और यथाच्छन्द के साथ मिलकर यथाच्छन्द हो जाता है।
पार्श्वस्थ आदि के विषय में विस्तार हेतु द्रष्टव्य-निभा. गा. ४३४०-४३५१। ११. सूत्र ३७,३८
दाता का हाथ, पात्र, दर्वी (कड़छी) और भाजन जल से आर्द्र, सस्निग्ध, सचित्त रजकण, मृत्तिका, क्षार, हरिताल, हिंगुल, मैनशिल, अनाज के भूसे, छिलके या फलों के सूक्ष्म खण्ड आदि से सने हुए हों तो भिक्षु उसे प्रतिषेध कर दे कि मैं ऐसा आहार नहीं ले सकता। यहां विमर्शनीय विषय यह है कि दशवैकालिक में प्राप्त होने वाली इन दो गाथाओं में सत्रह प्रकार के हाथों का उल्लेख मिलता है तथा अगस्त्यचूर्णि में भी इनके स्थान पर सत्रह श्लोक मिलते है। सूत्रकार ने इक्कीस हाथों का उल्लेख किया है तथा किसी-किसी प्रति में इस संदर्भ में दो गाथाएं उपलब्ध होती हैंउदउल्ले ससणिद्धे, ससरक्खे मट्टिया उसे लोणे य। हरियाले मणोसिलाए, वन्नि गेरुय सेढिए।।१।। हिंगुलु अंजणे लोद्धे, कुक्कुस पिट्ठ कंद-मूल-सिंगबेरे य। पुप्फक-कुटुं एए, एक्कवीसं भवे हत्था ॥२॥१२
इनके आधार पर सूत्ररचना भी की जा सकती है किन्तु इन गाथाओं में आए हुए कई शब्द कंद, मूल, सिंगबेर आदि की पुष्टि न निशीथभाष्य एवं चूर्णि से होती है और न आयारचूला (१६४८०) से। अतः यह अनुसंधान का विषय है कि इन इक्कीस हाथों की वक्तव्यता वाला पाठ कब से जुड़ा अथवा यदि यह पाठ सूत्रकार द्वारा प्रारम्भ से गृहीत है तो व्याख्या ग्रन्थों तथा अन्य आगमों में क्यों नहीं?
प्रस्तुत सूत्रद्वयी का प्रयोजन है-पुरःकर्म एवं पश्चात्कर्म दोष से
१. निभा. २ चू.पृ. २२५-विप्फालेति विहाडेति, अतीव फालेति
वियंभमाणो व्व विविधैः प्रकारैः फाले ति विष्फाले ति विडालिकाकारवत्। बृभा. ७०१ की वृत्ति-......सद्वितीयेन गमनं कर्त्तव्यम्, संघाटकेनेत्यर्थः।
निभा. गा. १८३०-१८३२, १८४१,१८४२ ४. प्रसा. १०३ वृ. पृ. २५-पार्श्वस्थः स यः कारणं तथाविधमन्तरेण
शय्यातराभ्याहृतं नृपतिपिण्डं नैत्यिकमनपिण्डं वा भुङ्क्ते।
वही-समाचारीविषयोऽवसीदति प्रमाद्यति यः सोऽवसन्नः। ६. वही, पृ. २६-कुत्सितं शीलमस्येति कुशीलः, स त्रिविधो
भवति-ज्ञानविषये, दर्शनविषये चारित्रविषये च। ७. व्यभा. ८८०
जाती कुले गणे या, कम्मे सिप्पे तवे सुते चेव।
सत्तविधं आजीवं, उवजीवति जो कुसीलो सो।। ८. प्र.सा. १०३, पृ. २७-गुणैर्दोषैश्च संसज्यते मिश्रीभवतीति संसक्तः। ९. व्यभा. ८८८-८९० १०. दसवे. ५॥१॥३३,३४ ११. वही, टि.पृ. १६८ १२. नव. पृ. ६८६