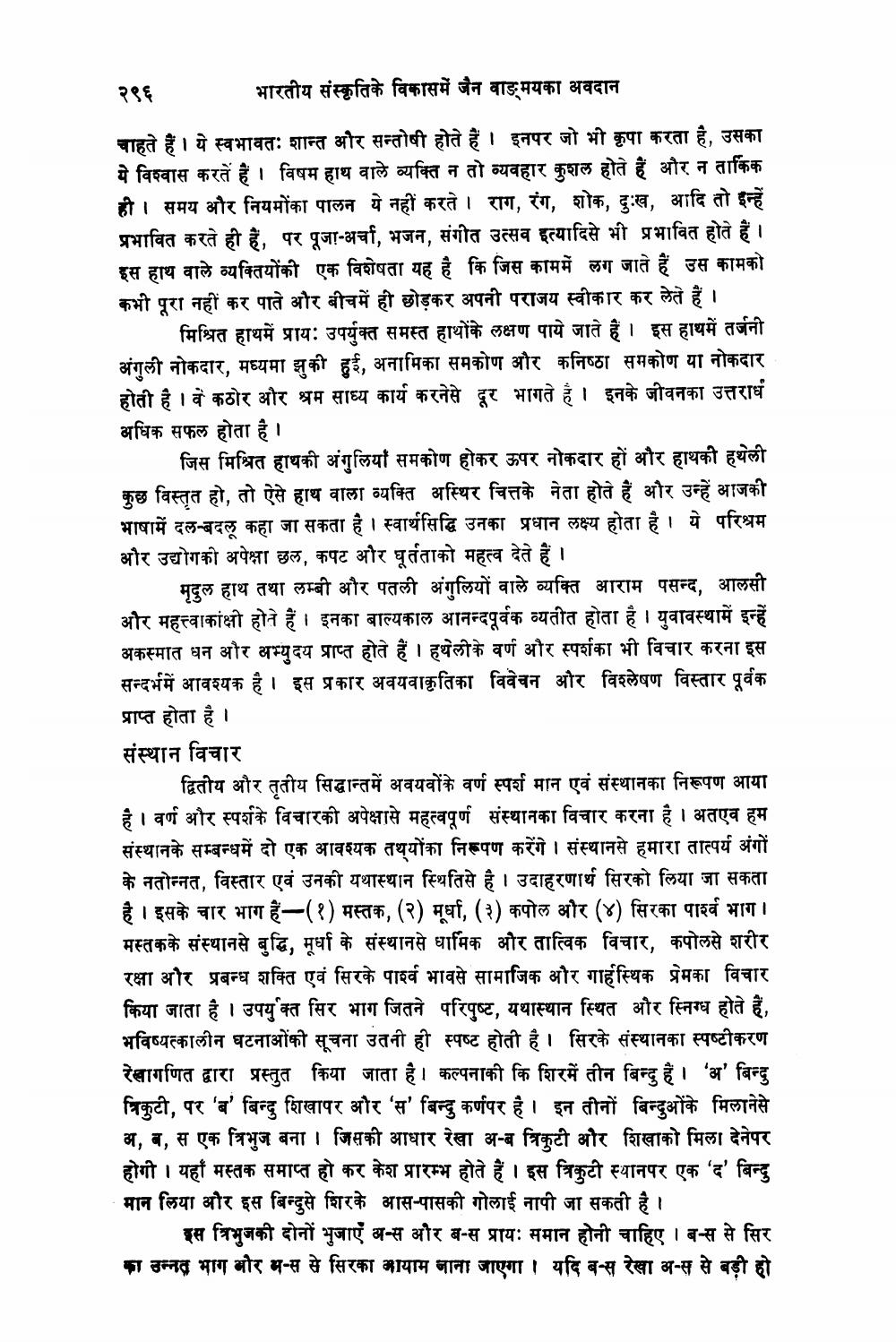________________
२९६
भारतीय संस्कृतिके विकासमें जैन वाङ्मयका अवदान
चाहते हैं। ये स्वभावतः शान्त और सन्तोषी होते हैं । इनपर जो भी कृपा करता है, उसका ये विश्वास करते हैं । विषम हाथ वाले व्यक्ति न तो व्यवहार कुशल होते हैं और न तार्किक ही। समय और नियमोंका पालन ये नहीं करते । राग, रंग, शोक, दुःख, आदि तो इन्हें प्रभावित करते ही हैं, पर पूजा-अर्चा, भजन, संगीत उत्सव इत्यादिसे भी प्रभावित होते हैं । इस हाथ वाले व्यक्तियोंकी एक विशेषता यह है कि जिस काममें लग जाते हैं उस कामको कभी पूरा नहीं कर पाते और बीचमें ही छोड़कर अपनी पराजय स्वीकार कर लेते हैं ।
मिश्रित हाथमें प्रायः उपर्युक्त समस्त हाथोंके लक्षण पाये जाते हैं। इस हाथमें तर्जनी अंगुली नोकदार, मध्यमा झुकी हुई, अनामिका समकोण और कनिष्ठा समकोण या नोकदार होती है । वे कठोर और श्रम साध्य कार्य करनेसे दूर भागते हैं। इनके जीवनका उत्तरार्ध अधिक सफल होता है।
जिस मिश्रित हाथकी अंगुलियाँ समकोण होकर ऊपर नोकदार हों और हाथकी हथेली कुछ विस्तृत हो, तो ऐसे हाथ वाला व्यक्ति अस्थिर चित्तके नेता होते हैं और उन्हें आजकी भाषामें दल-बदलू कहा जा सकता है । स्वार्थसिद्धि उनका प्रधान लक्ष्य होता है। ये परिश्रम और उद्योगको अपेक्षा छल, कपट और घूर्तताको महत्व देते हैं ।
___ मृदुल हाथ तथा लम्बी और पतली अंगुलियों वाले व्यक्ति आराम पसन्द, आलसी और महत्त्वाकांक्षी होते हैं। इनका बाल्यकाल आनन्दपूर्वक व्यतीत होता है । युवावस्थामें इन्हें अकस्मात धन और अभ्युदय प्राप्त होते हैं । हथेलीके वर्ण और स्पर्शका भी विचार करना इस सन्दर्भ में आवश्यक है। इस प्रकार अवयवाकृतिका विवेचन और विश्लेषण विस्तार पूर्वक प्राप्त होता है। संस्थान विचार
द्वितीय और तृतीय सिद्धान्तमें अवयवोंके वर्ण स्पर्श मान एवं संस्थानका निरूपण आया है । वर्ण और स्पर्शके विचारकी अपेक्षासे महत्वपूर्ण संस्थानका विचार करना है । अतएव हम संस्थानके सम्बन्धमें दो एक आवश्यक तथ्योंका निरूपण करेंगे । संस्थानसे हमारा तात्पर्य अंगों के नतोन्नत, विस्तार एवं उनकी यथास्थान स्थितिसे है । उदाहरणार्थ सिरको लिया जा सकता है । इसके चार भाग हैं-(१) मस्तक, (२) मूर्धा, (३) कपोल और (४) सिरका पार्श्व भाग। मस्तकके संस्थानसे बुद्धि, मूर्धा के संस्थानसे धार्मिक और तात्विक विचार, कपोलसे शरीर रक्षा और प्रबन्ध शक्ति एवं सिरके पार्श्व भावसे सामाजिक और गार्हस्थिक प्रेमका विचार किया जाता है । उपर्युक्त सिर भाग जितने परिपुष्ट, यथास्थान स्थित और स्निग्ध होते हैं, भविष्यत्कालीन घटनाओंको सूचना उतनी ही स्पष्ट होती है। सिरके संस्थानका स्पष्टीकरण रेखागणित द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। कल्पनाकी कि शिरमें तीन बिन्दु हैं । 'अ' बिन्दु त्रिकुटी, पर 'ब' बिन्दु शिखापर और 'स' बिन्दु कर्णपर है। इन तीनों बिन्दुओंके मिलानेसे अ, ब, स एक त्रिभुज बना । जिसकी आधार रेखा अ-ब त्रिकुटी और शिखाको मिला देनेपर होगी । यहाँ मस्तक समाप्त हो कर केश प्रारम्भ होते हैं । इस त्रिकुटी स्थानपर एक 'द' बिन्दु मान लिया और इस बिन्दुसे शिरके आस-पासको गोलाई नापी जा सकती है।
इस त्रिभुजकी दोनों भुजाएं अ-स और ब-स प्रायः ममान होनी चाहिए । ब-स से सिर का उन्नत भाग भोर भ-स से सिरका आयाम नाना जाएगा। यदि ब-स रेखा अ-स से बड़ी हो