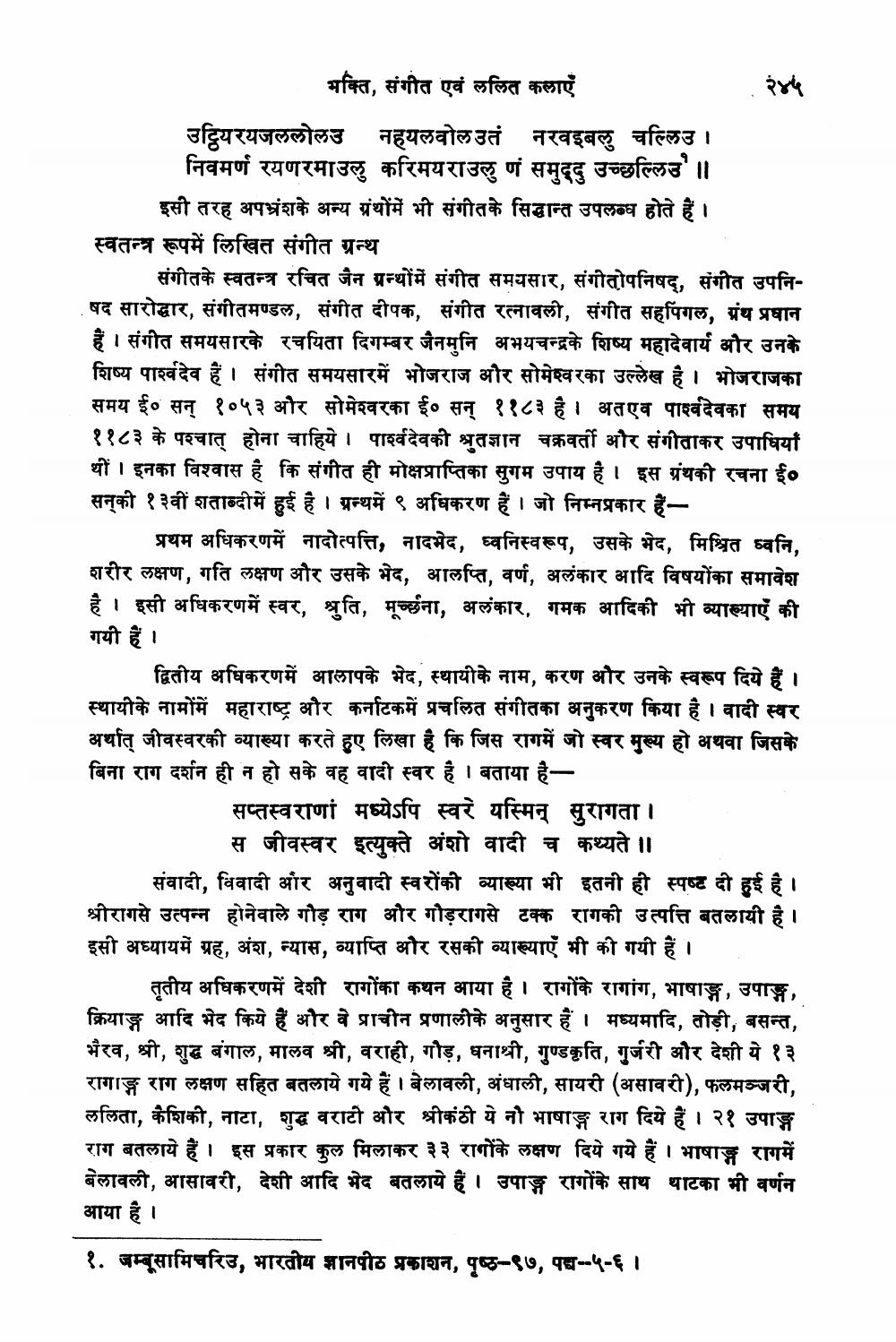________________
भक्ति, संगीत एवं ललित कलाएं उट्टियरयजललोलउ नहयलवोल उतं नरवइबलु चल्लिउ । निवमर्ण रयणरमाउलु करिमयराउलु णं समुदु उच्छल्लिउ ।
इसी तरह अपभ्रंशके अन्य ग्रंथों में भी संगीतके सिद्धान्त उपलब्ध होते हैं। स्वतन्त्र रूपमें लिखित संगीत ग्रन्थ
संगीतके स्वतन्त्र रचित जैन ग्रन्थों में संगीत समयसार, संगीतोपनिषद्, संगीत उपनिषद सारोद्धार, संगीतमण्डल, संगीत दीपक, संगीत रत्नावली, संगीत सहपिंगल, ग्रंथ प्रधान हैं । संगीत समयसारके रचयिता दिगम्बर जैनमुनि अभयचन्द्रके शिष्य महादेवार्य और उनके शिष्य पार्श्वदेव हैं। संगीत समयसारमें भोजराज और सोमेश्वरका उल्लेख है। भोजराजका समय ई० सन् १०५३ और सोमेश्वरका ई० सन् १९८३ है। अतएव पाश्वदेवका समय ११८३ के पश्चात् होना चाहिये । पार्श्वदेवकी श्रुतज्ञान चक्रवर्ती और संगीताकर उपाधियाँ थीं । इनका विश्वास है कि संगीत ही मोक्षप्राप्तिका सुगम उपाय है। इस ग्रंथकी रचना ई० सन्की १३वीं शताब्दीमें हुई है । ग्रन्थमें ९ अधिकरण हैं । जो निम्नप्रकार हैं
प्रथम अधिकरणमें नादोत्पत्ति, नादभेद, ध्वनिस्वरूप, उसके भेद, मिश्रित ध्वनि, शरीर लक्षण, गति लक्षण और उसके भेद, आलप्ति, वर्ण, अलंकार आदि विषयोंका समावेश है । इसी अधिकरणमें स्वर, श्रुति, मूर्च्छना, अलंकार, गमक आदिकी भी व्याख्याएँ की गयी हैं।
द्वितीय अधिकरणमें आलापके भेद, स्थायीके नाम, करण और उनके स्वरूप दिये हैं। स्थायीके नामोंमें महाराष्ट्र और कर्नाटकमें प्रचलित संगीतका अनुकरण किया है । वादी स्वर अर्थात् जीवस्वरकी व्याख्या करते हुए लिखा है कि जिस रागमें जो स्वर मुख्य हो अथवा जिसके बिना राग दर्शन ही न हो सके वह वादी स्वर है । बताया है
___ सप्तस्वराणां मध्येऽपि स्वरे यस्मिन् सुरागता।
स जीवस्वर इत्युक्ते अंशो वादी च कथ्यते ॥ संवादी, विवादी और अनुवादी स्वरोंकी व्याख्या भी इतनी ही स्पष्ट दी हुई है। श्रीरागसे उत्पन्न होनेवाले गौड़ राग और गौड़रागसे टक्क रागकी उत्पत्ति बतलायी है । इसी अध्यायमें ग्रह, अंश, न्यास, व्याप्ति और रसकी व्याख्याएँ भी की गयी हैं ।
तृतीय अधिकरणमें देशी रागोंका कथन आया है। रागोंके रागांग, भाषाङ्ग, उपाङ्ग, क्रियाङ्ग आदि भेद किये हैं और वे प्राचीन प्रणालीके अनुसार हैं । मध्यमादि, तोड़ी, बसन्त, भैरव, श्री, शुद्ध बंगाल, मालव श्री, वराही, गौड़, धनाश्री, गुण्डकृति, गुर्जरी और देशी ये १३ रागाङ्ग राग लक्षण सहित बतलाये गये हैं । बेलावली, अंधाली, सायरी (असावरी), फलमञ्जरी, ललिता, कैशिकी, नाटा, शुद्ध वराटी और श्रीकंठी ये नौ भाषाङ्ग राग दिये हैं । २१ उपाङ्ग राग बतलाये हैं। इस प्रकार कुल मिलाकर ३३ रागोंके लक्षण दिये गये हैं । भाषाङ्ग रागमें बेलावली, आसावरी, देशी आदि भेद बतलाये हैं । उपाङ्ग रागोंके साथ थाटका भी वर्णन आया है। १. जम्बूसामिचरिउ, भारतीय ज्ञानपीठ प्रकाशन, पृष्ठ-९७, पच-५-६ ।