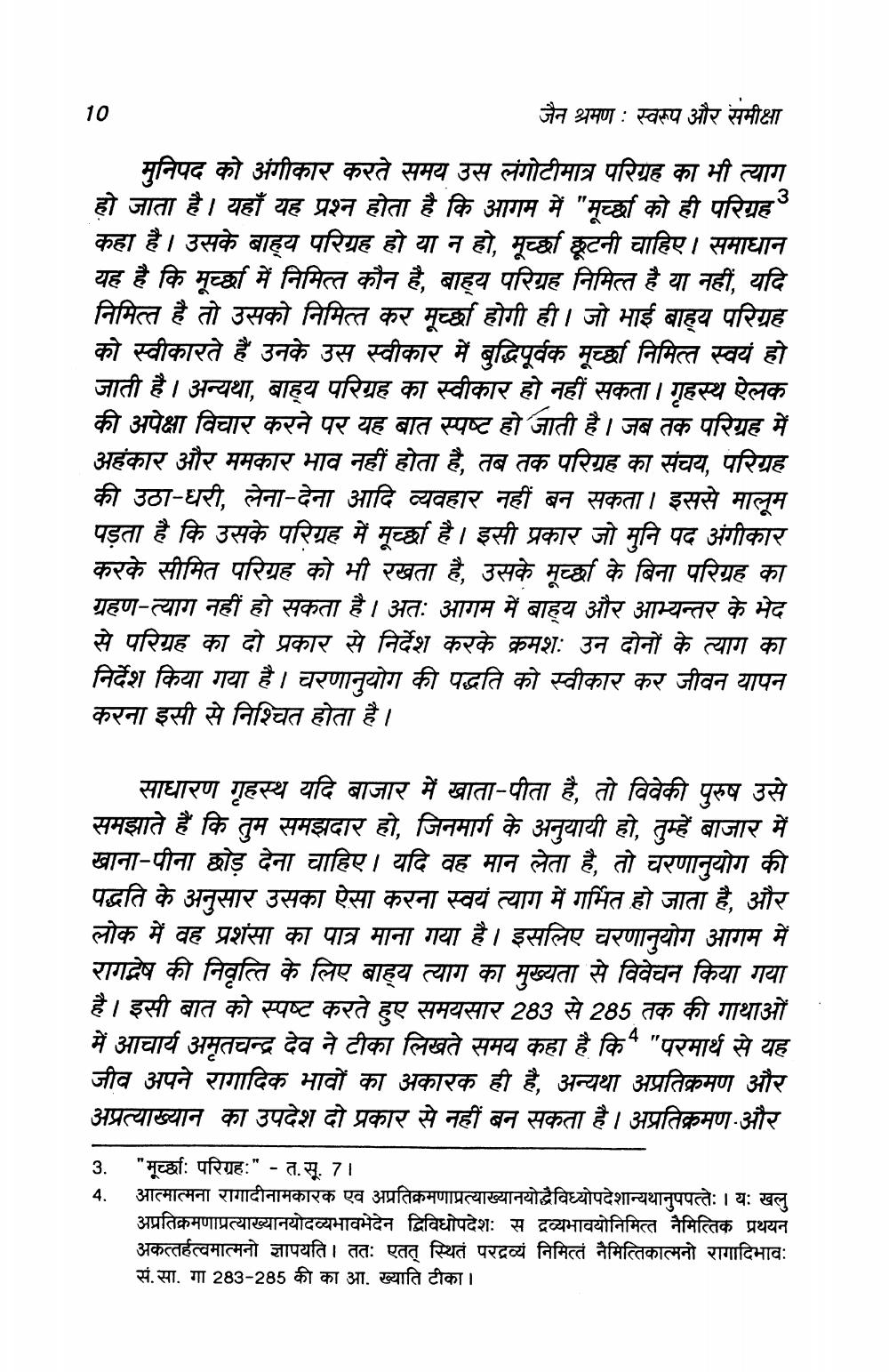________________
जैन श्रमण : स्वरूप और समीक्षा
मुनिपद को अंगीकार करते समय उस लंगोटीमात्र परिग्रह का भी त्याग हो जाता है। यहाँ यह प्रश्न होता है कि आगम में "मूच्र्छा को ही परिग्रह कहा है। उसके बाह्य परिग्रह हो या न हो, मूच्र्छा छूटनी चाहिए। समाधान यह है कि मूच्र्छा में निमित्त कौन है, बाह्य परिग्रह निमित्त है या नहीं, यदि निमित्त है तो उसको निमित्त कर मूच्छी होगी ही। जो भाई बाह्य परिग्रह को स्वीकारते हैं उनके उस स्वीकार में बुद्धिपूर्वक मूच्र्छा निमित्त स्वयं हो जाती है। अन्यथा, बाह्य परिग्रह का स्वीकार हो नहीं सकता। गृहस्थ ऐलक की अपेक्षा विचार करने पर यह बात स्पष्ट हो जाती है। जब तक परिग्रह में अहंकार और ममकार भाव नहीं होता है, तब तक परिग्रह का संचय, परिग्रह की उठा-धरी, लेना-देना आदि व्यवहार नहीं बन सकता। इससे मालूम पड़ता है कि उसके परिग्रह में मूच्र्छा है। इसी प्रकार जो मुनि पद अंगीकार करके सीमित परिग्रह को भी रखता है, उसके मूच्छा के बिना परिग्रह का ग्रहण-त्याग नहीं हो सकता है। अतः आगम में बाह्य और आभ्यन्तर के भेद से परिग्रह का दो प्रकार से निर्देश करके क्रमशः उन दोनों के त्याग का निर्देश किया गया है। चरणानुयोग की पद्धति को स्वीकार कर जीवन यापन करना इसी से निश्चित होता है।
साधारण गृहस्थ यदि बाजार में खाता-पीता है, तो विवेकी परुष उसे समझाते हैं कि तुम समझदार हो, जिनमार्ग के अनुयायी हो, तुम्हें बाजार में खाना-पीना छोड़ देना चाहिए। यदि वह मान लेता है, तो चरणानुयोग की पद्धति के अनुसार उसका ऐसा करना स्वयं त्याग में गर्भित हो जाता है, और लोक में वह प्रशंसा का पात्र माना गया है। इसलिए चरणानुयोग आगम में रागद्वेष की निवृत्ति के लिए बाह्य त्याग का मुख्यता से विवेचन किया गया है। इसी बात को स्पष्ट करते हुए समयसार 283 से 285 तक की गाथाओं में आचार्य अमृतचन्द्र देव ने टीका लिखते समय कहा है कि "परमार्थ से यह जीव अपने रागादिक भावों का अकारक ही है, अन्यथा अप्रतिक्रमण और अप्रत्याख्यान का उपदेश दो प्रकार से नहीं बन सकता है। अप्रतिक्रमण और
3. "मूर्छाः परिग्रहः" - त.सू. 7 । 4. आत्मात्मना रागादीनामकारक एव अप्रतिक्रमणाप्रत्याख्यानयोद्धैविध्योपदेशान्यथानुपपत्तेः । यः खलु
अप्रतिक्रमणाप्रत्याख्यानयोदव्यभावभेदेन द्विविधोपदेशः स द्रव्यभावयोनिमित्त नैमित्तिक प्रथयन अकत्तहत्वमात्मनो ज्ञापयति। ततः एतत स्थितं परद्रव्यं निमित्तं नैमित्तिकात्मनो रागादिभाव: सं.सा. गा 283-285 की का आ. ख्याति टीका।