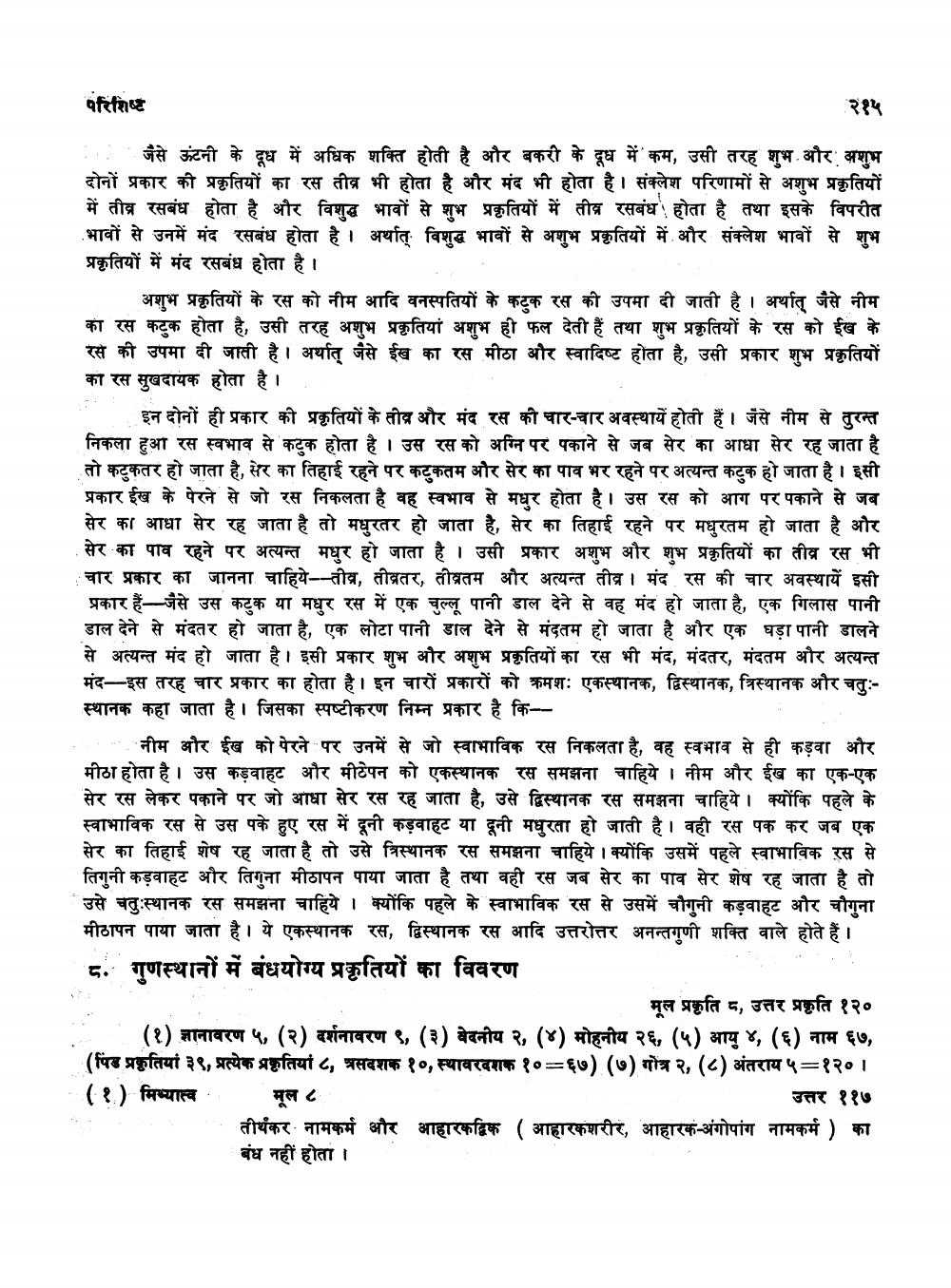________________
परिशिष्ट
जैसे ऊंटनी के दूध में अधिक दोनों प्रकार की प्रकृतियों का रस तीव्र में तीव्र रसबंध होता है और विशुद्ध भावों से उनमें मंद रसबंध होता है। प्रकृतियों में मंद रसबंध होता है।
२१५
शक्ति होती है और बकरी के दूध में कम, उसी तरह शुभ और अशुभ भी होता है और मंद भी होता है । संक्लेश परिणामों से अशुभ प्रकृतियों भावों से शुभ प्रकृतियों में तीव्र रसबंध होता है तथा इसके विपरीत अर्थात् विशुद्ध भावों से अशुभ प्रकृतियों में और संक्लेश भावों से शुभ
अशुभ प्रकृतियों के रस को नीम आदि वनस्पतियों के कटुक रस की उपमा दी जाती है। अर्थात् जैसे नीम का रस कटुक होता है, उसी तरह अशुभ प्रकृतियां अशुभ ही फल देती हैं तथा शुभ प्रकृतियों के रस को ईख के रस की उपमा दी जाती है। अर्थात् जैसे ईख का रस मीठा और स्वादिष्ट होता है, उसी प्रकार शुभ प्रकृतियों का रस सुखदायक होता है ।
निकला
तो
इन दोनों ही प्रकार की प्रकृतियों के तीव्र और मंद रस की चार-चार अवस्थायें होती हैं जैसे नीम से तुरन्त 'हुआ रस स्वभाव से कटुक होता है। उस रस को अग्नि पर पकाने से जब सेर का आधा सेर रह जाता है कटुकतर हो जाता है, सेर का तिहाई रहने पर कटुकतम और सेर का पाव भर रहने पर अत्यन्त कटुक हो जाता है । इसी प्रकार ईख के पेरने से जो रस निकलता है वह स्वभाव से मधुर होता है उस रस को आग पर पकाने से जब सेर का आधा सेर रह जाता तो मधुरतर हो जाता है, सेर का तिहाई रहने पर मधुरतम हो जाता है और सेर का पाव रहने पर अत्यन्त मधुर हो जाता है। उसी प्रकार अशुभ और शुभ प्रकृतियों का तीव्र रस भी चार प्रकार का जानना चाहिये तीव्र, तीव्रतर तीव्रतम और अत्यन्त तीव्र मंद रस की चार अवस्थायें इसी प्रकार हैं——जैसे उस कटुक या मधुर रस में एक चुल्लू पानी डाल देने से वह मंद हो जाता है, एक गिलास पानी डाल देने से मंदतर हो जाता है, एक लोटा पानी डाल देने से मंदतम हो जाता है और एक पड़ा पानी डालने
है
अत्यन्त मंद हो जाता है। इसी प्रकार शुभ और अशुभ प्रकृतियों का रस भी मंद, मंदतर, मंदतम और अत्यन्त मंद — इस तरह चार प्रकार का होता है। इन चारों प्रकारों को क्रमश: एकस्थानक, द्विस्थानक, निस्थानक और चतु:स्थानक कहा जाता है। जिसका स्पष्टीकरण निम्न प्रकार है कि
--
नीम और ईख को पैरने पर उनमें से जो स्वाभाविक रस निकलता है, वह स्वभाव से ही कड़वा और मीठा होता है। उस कडवाहट और मीटेपन को एकस्थानक रस समझना चाहिये। नीम और ईख का एक-एक सेर रस लेकर पकाने पर जो आधा सेर रस रह जाता है, उसे द्विस्थानक रस समझना चाहिये। क्योंकि पहले के स्वाभाविक रस से उस पके हुए रस में दूनी कड़वाहट या दूनी मधुरता हो जाती है । वही रस पक कर जब एक सेर का तिहाई शेष रह जाता है तो उसे त्रिस्थानक रस समझना चाहिये । क्योंकि उसमें पहले स्वाभाविक रस से तिनी कड़वाहट और तिगुना मीठापन पाया जाता है तथा वही रस जब सेर का पाव सेर शेष रह जाता है तो उसे चतुःस्थानक रस समझना चाहिये। क्योंकि पहले के स्वाभाविक रस से मीठापन पाया जाता है। ये एकस्थानक रस, द्विस्थानक रस आदि उत्तरोत्तर ८. गुणस्थानों में बंधयोग्य प्रकृतियों का विवरण
उसमें चौगुनी कड़वाहट और चौगुना अनन्तगुणी शक्ति वाले होते हैं।
मूल प्रकृति ८, उत्तर प्रकृति १२०
(१) ज्ञानावरण ५ (२) दर्शनावरण ९, (३) वेदनीय २, (४) मोहनीय २६, (५) आयु ४, (६) नाम ६७, (पिंड प्रकृतियां ३९, प्रत्येक प्रकृतियां ८, श्रसदशक १०, स्थावरदशक १० = ६७) (७) गोत्र २, (८) अंतराय ५ = १२० । (१) मिध्यात्व
मूल ८ उत्तर ११७ तीर्थंकर नामकर्म और आहारकद्विक ( आहारकशरीर, आहारक अंगोपांग नामकर्म ) का बंध नहीं होता ।