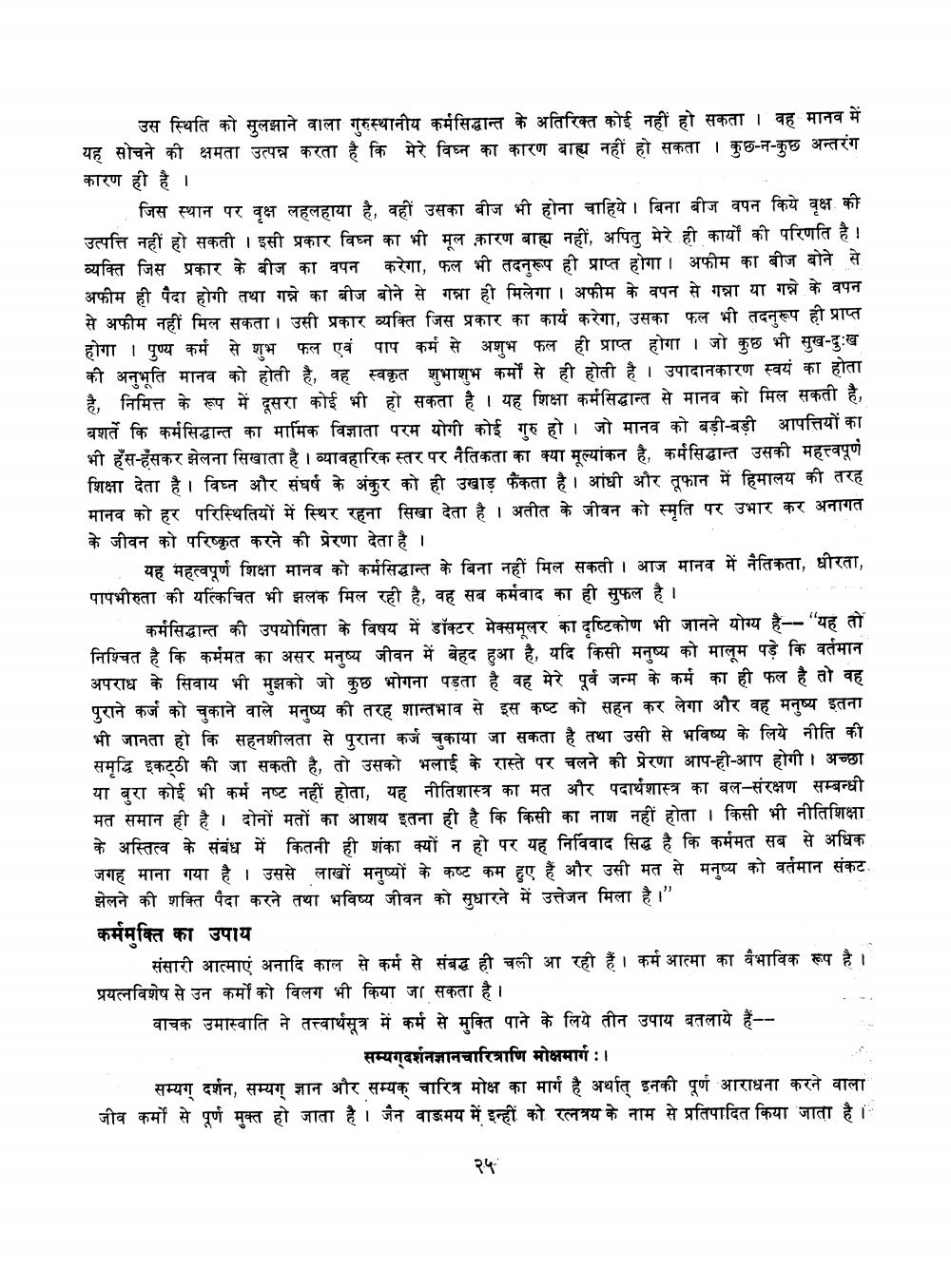________________
उस स्थिति को सुलझाने वाला गुरुस्थानीय कर्मसिद्धान्त के अतिरिक्त कोई नहीं हो सकता । वह मानव में यह सोचने की क्षमता उत्पन्न करता है कि मेरे विघ्न का कारण बाह्य नहीं हो सकता । कुछ-न-कुछ अन्तरंग कारण ही है ।
जिस स्थान पर वृक्ष लहलहाया है, वहीं उसका बीज भी होना चाहिये। बिना बीज वपन किये वृक्ष की उत्पत्ति नहीं हो सकती । इसी प्रकार विघ्न का भी मूल कारण बाह्य नहीं, अपितु मेरे ही कार्यों की परिणति है।
जिस प्रकार के बीज का वपन करेगा, फल भी तदनरूप ही प्राप्त होगा। अफीम का बीज बोने से अफीम ही पैदा होगी तथा गन्ने का बीज बोने से गन्ना ही मिलेगा। अफीम के वपन से गन्ना या गन्ने के वपन से अफीम नहीं मिल सकता। उसी प्रकार व्यक्ति जिस प्रकार का कार्य करेगा, उसका फल भी तदनुरूप ही प्राप्त होगा । पुण्य कर्म से शुभ फल एवं पाप कर्म से अशुभ फल ही प्राप्त होगा । जो कुछ भी सुख-दुःख की अनुभूति मानव को होती है, वह स्वकृत शुभाशुभ कर्मों से ही होती है । उपादानकारण स्वयं का होता है, निमित्त के रूप में दूसरा कोई भी हो सकता है । यह शिक्षा कर्मसिद्धान्त से मानव को मिल सकती है, बशर्ते कि कर्मसिद्धान्त का मार्मिक विज्ञाता परम योगी कोई गुरु हो। जो मानव को बड़ी-बड़ी आपत्तियों का भी हँस-हँसकर झेलना सिखाता है । व्यावहारिक स्तर पर नैतिकता का क्या मूल्यांकन है, कर्मसिद्धान्त उसकी महत्त्वपूर्ण शिक्षा देता है। विघ्न और संघर्ष के अंकुर को ही उखाड़ फैकता है। आंधी और तूफान में हिमालय की तरह मानव को हर परिस्थितियों में स्थिर रहना सिखा देता है । अतीत के जीवन को स्मृति पर उभार कर अनागत के जीवन को परिष्कृत करने की प्रेरणा देता है ।
. यह महत्वपूर्ण शिक्षा मानव को कर्मसिद्धान्त के बिना नहीं मिल सकती। आज मानव में नैतिकता, धीरता, पापभीरुता की यत्किचित भी झलक मिल रही है, वह सब कर्मवाद का ही सुफल है।
कर्मसिद्धान्त की उपयोगिता के विषय में डॉक्टर मेक्समूलर का दृष्टिकोण भी जानने योग्य है--"यह तों निश्चित है कि कर्ममत का असर मनुष्य जीवन में बेहद हआ है, यदि किसी मनुष्य को मालूम पड़े कि वर्तमान अपराध के सिवाय भी मुझको जो कुछ भोगना पड़ता है वह मेरे पूर्व जन्म के कर्म का ही फल है तो वह पुराने कर्ज को चुकाने वाले मनुष्य की तरह शान्तभाव से इस कष्ट को सहन कर लेगा और वह मनुष्य इतना भी जानता हो कि सहनशीलता से पुराना कर्ज चुकाया जा सकता है तथा उसी से भविष्य के लिये नीति की समृद्धि इकट्ठी की जा सकती है, तो उसको भलाई के रास्ते पर चलने की प्रेरणा आप-ही-आप होगी। अच्छा या बुरा कोई भी कर्म नष्ट नहीं होता, यह नीतिशास्त्र का मत और पदार्थशास्त्र का बल-संरक्षण सम्बन्धी मत समान ही है। दोनों मतों का आशय इतना ही है कि किसी का नाश नहीं होता । किसी भी नीतिशिक्षा के अस्तित्व के संबंध में कितनी ही शंका क्यों न हो पर यह निर्विवाद सिद्ध है कि कर्ममत सब से अधिक जगह माना गया है । उससे लाखों मनुष्यों के कष्ट कम हुए हैं और उसी मत से मनुष्य को वर्तमान संकट झेलने की शक्ति पैदा करने तथा भविष्य जीवन को सुधारने में उत्तेजन मिला है।" कर्ममुक्ति का उपाय
संसारी आत्माएं अनादि काल से कर्म से संबद्ध ही चली आ रही हैं। कर्म आत्मा का वैभाविक रूप है। प्रयत्नविशेष से उन कर्मों को विलग भी किया जा सकता है। वाचक उमास्वाति ने तत्त्वार्थसूत्र में कर्म से मुक्ति पाने के लिये तीन उपाय बतलाये हैं--
सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्राणि मोक्षमार्ग :। सम्यग् दर्शन, सम्यग् ज्ञान और सम्यक् चारित्र मोक्ष का मार्ग है अर्थात् इनकी पूर्ण आराधना करने वाला जीव कर्मों से पूर्ण मुक्त हो जाता है। जैन वाङमय में इन्हीं को रत्नत्रय के नाम से प्रतिपादित किया जाता है।
२५