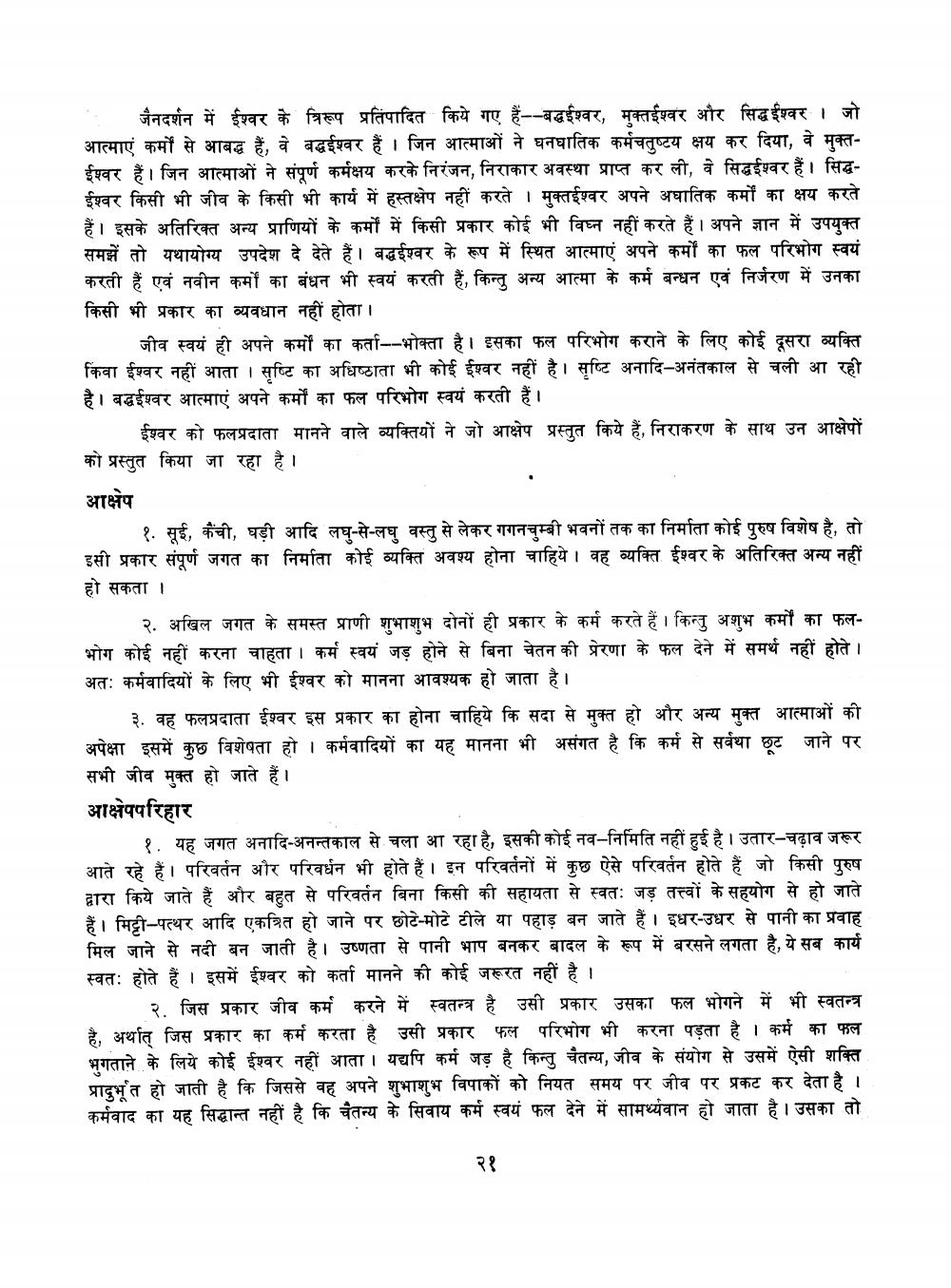________________
जैनदर्शन में ईश्वर के त्रिरूप प्रतिपादित किये गए हैं--बद्धईश्वर, मुक्तईश्वर और सिद्ध ईश्वर । जो आत्माएं कर्मों से आबद्ध हैं, वे बद्धईश्वर हैं । जिन आत्माओं ने घनघातिक कर्मचतुष्टय क्षय कर दिया, वे मुक्तईश्वर हैं। जिन आत्माओं ने संपूर्ण कर्मक्षय करके निरंजन, निराकार अवस्था प्राप्त कर ली, वे सिद्धईश्वर हैं। सिद्धईश्वर किसी भी जीव के किसी भी कार्य में हस्तक्षेप नहीं करते । मुक्तईश्वर अपने अघातिक कर्मों का क्षय करते हैं। इसके अतिरिक्त अन्य प्राणियों के कर्मों में किसी प्रकार कोई भी विघ्न नहीं करते हैं। अपने ज्ञान में उपयुक्त समझें तो यथायोग्य उपदेश दे देते हैं। बद्धईश्वर के रूप में स्थित आत्माएं अपने कर्मों का फल परिभोग स्वयं करती हैं एवं नवीन कर्मों का बंधन भी स्वयं करती हैं, किन्तु अन्य आत्मा के कर्म बन्धन एवं निर्जरण में उनका किसी भी प्रकार का व्यवधान नहीं होता।
जीव स्वयं ही अपने कर्मों का कर्ता--भोक्ता है। इसका फल परिभोग कराने के लिए कोई दूसरा व्यक्ति किंवा ईश्वर नहीं आता । सृष्टि का अधिष्ठाता भी कोई ईश्वर नहीं है। सृष्टि अनादि-अनंतकाल से चली आ रही है। बद्धईश्वर आत्माएं अपने कर्मों का फल परिभोग स्वयं करती हैं।
ईश्वर को फलप्रदाता मानने वाले व्यक्तियों ने जो आक्षेप प्रस्तुत किये हैं, निराकरण के साथ उन आक्षेपों को प्रस्तुत किया जा रहा है। आक्षेप
१. सूई, कैंची, घड़ी आदि लघु-से-लघु वस्तु से लेकर गगनचुम्बी भवनों तक का निर्माता कोई पुरुष विशेष है, तो इसी प्रकार संपूर्ण जगत का निर्माता कोई व्यक्ति अवश्य होना चाहिये। वह व्यक्ति ईश्वर के अतिरिक्त अन्य नहीं हो सकता ।
२. अखिल जगत के समस्त प्राणी शुभाशुभ दोनों ही प्रकार के कर्म करते हैं । किन्तु अशुभ कर्मों का फलभोग कोई नहीं करना चाहता। कर्म स्वयं जड़ होने से बिना चेतन की प्रेरणा के फल देने में समर्थ नहीं होते। अतः कर्मवादियों के लिए भी ईश्वर को मानना आवश्यक हो जाता है।
३. वह फलप्रदाता ईश्वर इस प्रकार का होना चाहिये कि सदा से मुक्त हो और अन्य मुक्त आत्माओं की अपेक्षा इसमें कुछ विशेषता हो । कर्मवादियों का यह मानना भी असंगत है कि कर्म से सर्वथा छट जाने पर सभी जीव मुक्त हो जाते हैं। आक्षेपपरिहार
१. यह जगत अनादि-अनन्तकाल से चला आ रहा है, इसकी कोई नव-निर्मिति नहीं हुई है। उतार-चढ़ाव जरूर आते रहे हैं। परिवर्तन और परिवर्धन भी होते हैं। इन परिवर्तनों में कुछ ऐसे परिवर्तन होते हैं जो किसी पुरुष द्वारा किये जाते हैं और बहुत से परिवर्तन बिना किसी की सहायता से स्वतः जड़ तत्त्वों के सहयोग से हो जाते हैं। मिट्टी-पत्थर आदि एकत्रित हो जाने पर छोटे-मोटे टीले या पहाड़ बन जाते हैं। इधर-उधर से पानी का प्रवाह मिल जाने से नदी बन जाती है। उष्णता से पानी भाप बनकर बादल के रूप में बरसने लगता है, ये सब कार्य स्वत: होते हैं। इसमें ईश्वर को कर्ता मानने की कोई जरूरत नहीं है।
२. जिस प्रकार जीव कर्म करने में स्वतन्त्र है उसी प्रकार उसका फल भोगने में भी स्वतन्त्र है, अर्थात् जिस प्रकार का कर्म करता है उसी प्रकार फल परिभोग भी करना पड़ता है । कर्म का फल भुगताने के लिये कोई ईश्वर नहीं आता। यद्यपि कर्म जड़ है किन्तु चैतन्य, जीव के संयोग से उसमें ऐसी शक्ति प्रादुर्भूत हो जाती है कि जिससे वह अपने शुभाशुभ विपाकों को नियत समय पर जीव पर प्रकट कर देता है । कर्मवाद का यह सिद्धान्त नहीं है कि चैतन्य के सिवाय कर्म स्वयं फल देने में सामर्थ्यवान हो जाता है। उसका तो