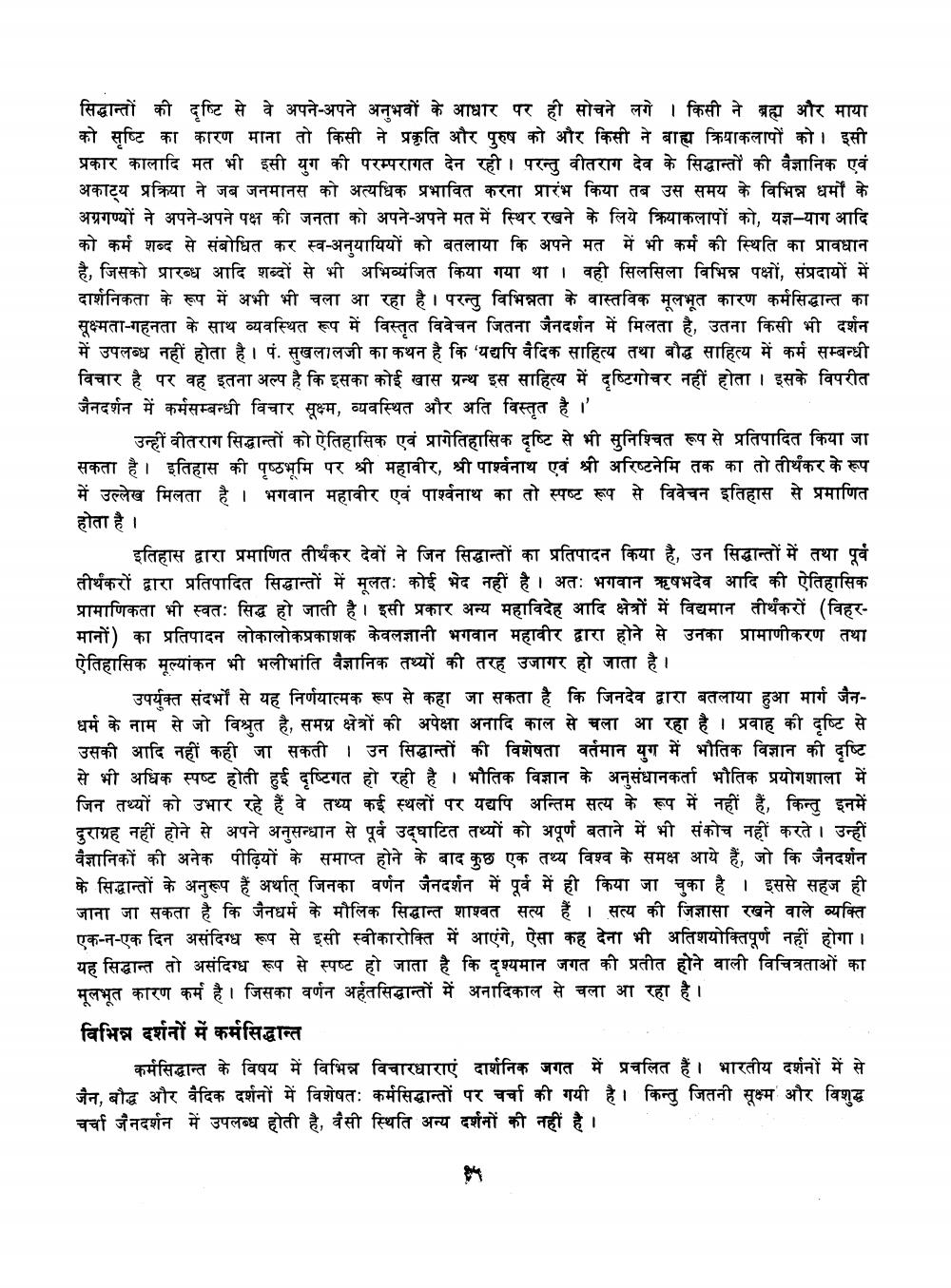________________
सिद्धान्तों की दृष्टि से वे अपने-अपने अनुभवों के आधार पर ही सोचने लगे । किसी ने ब्रह्म और माया को सृष्टि का कारण माना तो किसी ने प्रकृति और पुरुष को और किसी ने बाह्य क्रियाकलापों को। इसी प्रकार कालादि मत भी इसी युग की परम्परागत देन रही। परन्तु वीतराग देव के सिद्धान्तों की वैज्ञानिक एवं अकाट्य प्रक्रिया ने जब जनमानस को अत्यधिक प्रभावित करना प्रारंभ किया तब उस समय के विभिन्न धर्मों के अग्रगण्यों ने अपने-अपने पक्ष की जनता को अपने-अपने मत में स्थिर रखने के लिये क्रियाकलापों को, यज्ञ-याग आदि को कर्म शब्द से संबोधित कर स्व-अनुयायियों को बतलाया कि अपने मत में भी कर्म की स्थिति का प्रावधान है, जिसको प्रारब्ध आदि शब्दों से भी अभिव्यंजित किया गया था । वही सिलसिला विभिन्न पक्षों, संप्रदायों में दार्शनिकता के रूप में अभी भी चला आ रहा है। परन्तु विभिन्नता के वास्तविक मूलभूत कारण कर्मसिद्धान्त का सूक्ष्मता-गहनता के साथ व्यवस्थित रूप में विस्तृत विवेचन जितना जैनदर्शन में मिलता है, उतना किसी भी दर्शन में उपलब्ध नहीं होता है। पं. सुखलालजी का कथन है कि 'यद्यपि वैदिक साहित्य तथा बौद्ध साहित्य में कर्म सम्बन्धी विचार है पर वह इतना अल्प है कि इसका कोई खास ग्रन्थ इस साहित्य में दृष्टिगोचर नहीं होता। इसके विपरीत जैनदर्शन में कर्मसम्बन्धी विचार सूक्ष्म, व्यवस्थित और अति विस्तृत है।'
उन्हीं वीतराग सिद्धान्तों को ऐतिहासिक एवं प्रागेतिहासिक दृष्टि से भी सुनिश्चित रूप से प्रतिपादित किया जा सकता है। इतिहास की पृष्ठभूमि पर श्री महावीर, श्री पार्श्वनाथ एवं श्री अरिष्टनेमि तक का तो तीर्थंकर के रूप में उल्लेख मिलता है। भगवान महावीर एवं पार्श्वनाथ का तो स्पष्ट रूप से विवेचन इतिहास से प्रमाणित होता है।
इतिहास द्वारा प्रमाणित तीर्थंकर देवों ने जिन सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया है, उन सिद्धान्तों में तथा पूर्व तीर्थंकरों द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्तों में मूलतः कोई भेद नहीं है। अतः भगवान ऋषभदेव आदि की ऐतिहासिक प्रामाणिकता भी स्वतः सिद्ध हो जाती है। इसी प्रकार अन्य महाविदेह आदि क्षेत्रों में विद्यमान तीर्थंकरों (विहरमानों) का प्रतिपादन लोकालोकप्रकाशक केवलज्ञानी भगवान महावीर द्वारा होने से उनका प्रामाणीकरण तथा ऐतिहासिक मूल्यांकन भी भलीभांति वैज्ञानिक तथ्यों की तरह उजागर हो जाता है।
उपर्युक्त संदर्भो से यह निर्णयात्मक रूप से कहा जा सकता है कि जिनदेव द्वारा बतलाया हुआ मार्ग जैनधर्म के नाम से जो विश्रुत है, समग्र क्षेत्रों की अपेक्षा अनादि काल से चला आ रहा है । प्रवाह की दृष्टि से उसकी आदि नहीं कही जा सकती । उन सिद्धान्तों की विशेषता वर्तमान युग में भौतिक विज्ञान की दृष्टि से भी अधिक स्पष्ट होती हुई दृष्टिगत हो रही है । भौतिक विज्ञान के अनुसंधानकर्ता भौतिक प्रयोगशाला में जिन तथ्यों को उभार रहे हैं वे तथ्य कई स्थलों पर यद्यपि अन्तिम सत्य के रूप में नहीं हैं, किन्तु इनमें दुराग्रह नहीं होने से अपने अनुसन्धान से पूर्व उद्घाटित तथ्यों को अपूर्ण बताने में भी संकोच नहीं करते। उन्हीं वैज्ञानिकों की अनेक पीढ़ियों के समाप्त होने के बाद कुछ एक तथ्य विश्व के समक्ष आये हैं, जो कि जैनदर्शन के सिद्धान्तों के अनुरूप हैं अर्थात् जिनका वर्णन जैनदर्शन में पूर्व में ही किया जा चुका है । इससे सहज ही जाना जा सकता है कि जैनधर्म के मौलिक सिद्धान्त शाश्वत सत्य हैं । सत्य की जिज्ञासा रखने वाले व्यक्ति एक-न-एक दिन असंदिग्ध रूप से इसी स्वीकारोक्ति में आएंगे, ऐसा कह देना भी अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं होगा। यह सिद्धान्त तो असंदिग्ध रूप से स्पष्ट हो जाता है कि दृश्यमान जगत की प्रतीत होने वाली विचित्रताओं का मलभत कारण कर्म है। जिसका वर्णन अर्हतसिद्धान्तों में अनादिकाल से चला आ रहा है। विभिन्न दर्शनों में कर्मसिद्धान्त
कर्मसिद्धान्त के विषय में विभिन्न विचारधाराएं दार्शनिक जगत में प्रचलित हैं। भारतीय दर्शनों में से जैन, बौद्ध और वैदिक दर्शनों में विशेषतः कर्मसिद्धान्तों पर चर्चा की गयी है। किन्तु जितनी सूक्ष्म और विशुद्ध चर्चा जैनदर्शन में उपलब्ध होती है, वैसी स्थिति अन्य दर्शनों की नहीं है।