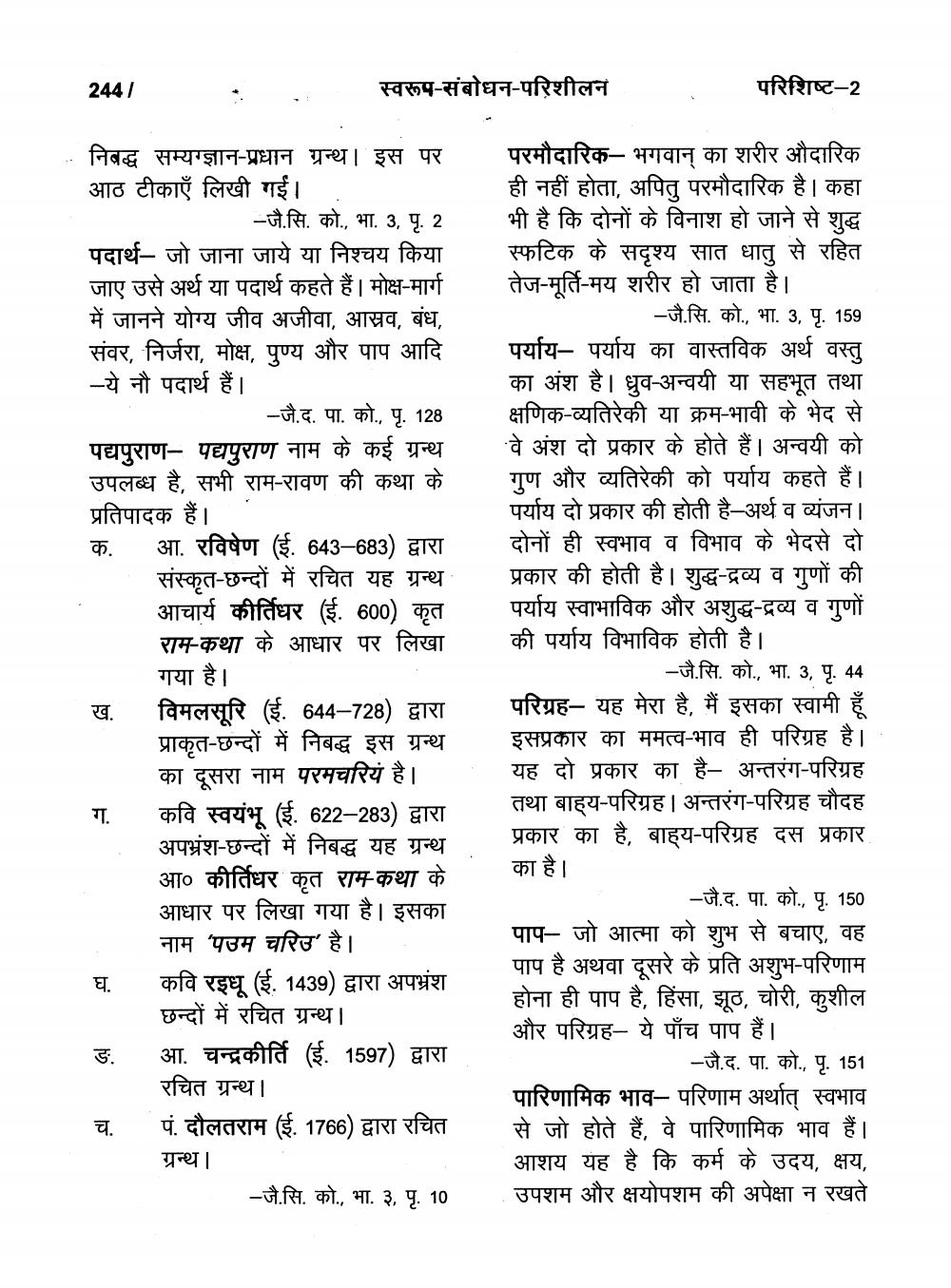________________
244/
निबद्ध सम्यग्ज्ञान- प्रधान ग्रन्थ। इस पर आठ टीकाएँ लिखी गईं।
- जै. सि. को. भा. 3, पृ. 2 पदार्थ- जो जाना जाये या निश्चय किया जाए उसे अर्थ या पदार्थ कहते हैं। मोक्ष-मार्ग में जानने योग्य जीव अजीवा, आस्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष, पुण्य और पाप आदि - ये नौ पदार्थ हैं।
- जै. द. पा. को ., पृ. 128 पद्यपुराण- पद्यपुराण नाम के कई ग्रन्थ उपलब्ध है, सभी राम-रावण की कथा के प्रतिपादक हैं।
क.
ख.
ग.
घ.
स्वरूप-संबोधन - परिशीलन
ङ.
च.
आ. रविषेण (ई. 643 - 683) द्वारा संस्कृत छन्दों में रचित यह ग्रन्थ आचार्य कीर्तिधर (ई. 600) कृत राम कथा के आधार पर लिखा गया है ।
विमलसूरि (ई. 644-728) द्वारा प्राकृत-छन्दों में निबद्ध इस ग्रन्थ का दूसरा नाम परमचरियं है। कवि स्वयंभू (ई. 622-283) द्वारा अपभ्रंश - छन्दों में निबद्ध यह ग्रन्थ आ० कीर्तिधर कृत राम कथा के आधार पर लिखा गया है। इसका नाम 'पउम चरिउ' है ।
कवि इधू (ई. 1439 ) द्वारा अपभ्रंश छन्दों में रचित ग्रन्थ ।
आ. चन्द्रकीर्ति (ई. 1597 ) द्वारा रचित ग्रन्थ ।
पं. दौलतराम (ई. 1766) द्वारा रचित
ग्रन्थ ।
- जै. सि. को. भा. ३, पृ. 10
परिशिष्ट-2
परमौदारिक- भगवान् का शरीर औदारिक ही नहीं होता, अपितु परमौदारिक है। कहा भी है कि दोनों के विनाश हो जाने से शुद्ध स्फटिक के सदृश्य सात धातु से रहित तेज-मूर्ति-मय शरीर हो जाता है ।
- जै. सि. को., भा. 3, पृ. 159 पर्याय- पर्याय का वास्तविक अर्थ वस्तु का अंश है। ध्रुव - अन्वयी या सहभूत तथा क्षणिक - व्यतिरेकी या क्रम-भावी के भेद से वे अंश दो प्रकार के होते हैं । अन्वयी को गुण और व्यतिरेकी को पर्याय कहते हैं । पर्याय दो प्रकार की होती है-अर्थ व व्यंजन | दोनों ही स्वभाव व विभाव के भेदसे दो प्रकार की होती है। शुद्ध-द्रव्य व गुणों की पर्याय स्वाभाविक और अशुद्ध-द्रव्य व गुणों की पर्याय विभाविक होती है।
- जै. सि. को., भा. 3, पृ. 44 परिग्रह- यह मेरा है, मैं इसका स्वामी हूँ इसप्रकार का ममत्व-भाव ही परिग्रह है । यह दो प्रकार का है- अन्तरंग परिग्रह तथा बाह्य परिग्रह | अन्तरंग - परिग्रह चौदह प्रकार का है, बाह्य परिग्रह दस प्रकार का है।
- जै. द. पा. को ., पृ. 150 पाप - जो आत्मा को शुभ से बचाए, वह पाप है अथवा दूसरे के प्रति अशुभ परिणाम होना ही पाप है, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह- ये
पाँच पाप हैं।
- जै. द. पा. को ., पृ. 151 पारिणामिक भाव- परिणाम अर्थात् स्वभाव से जो होते हैं, वे पारिणामिक भाव हैं । आशय यह है कि कर्म के उदय, क्षय, उपशम और क्षयोपशम की अपेक्षा न रखते